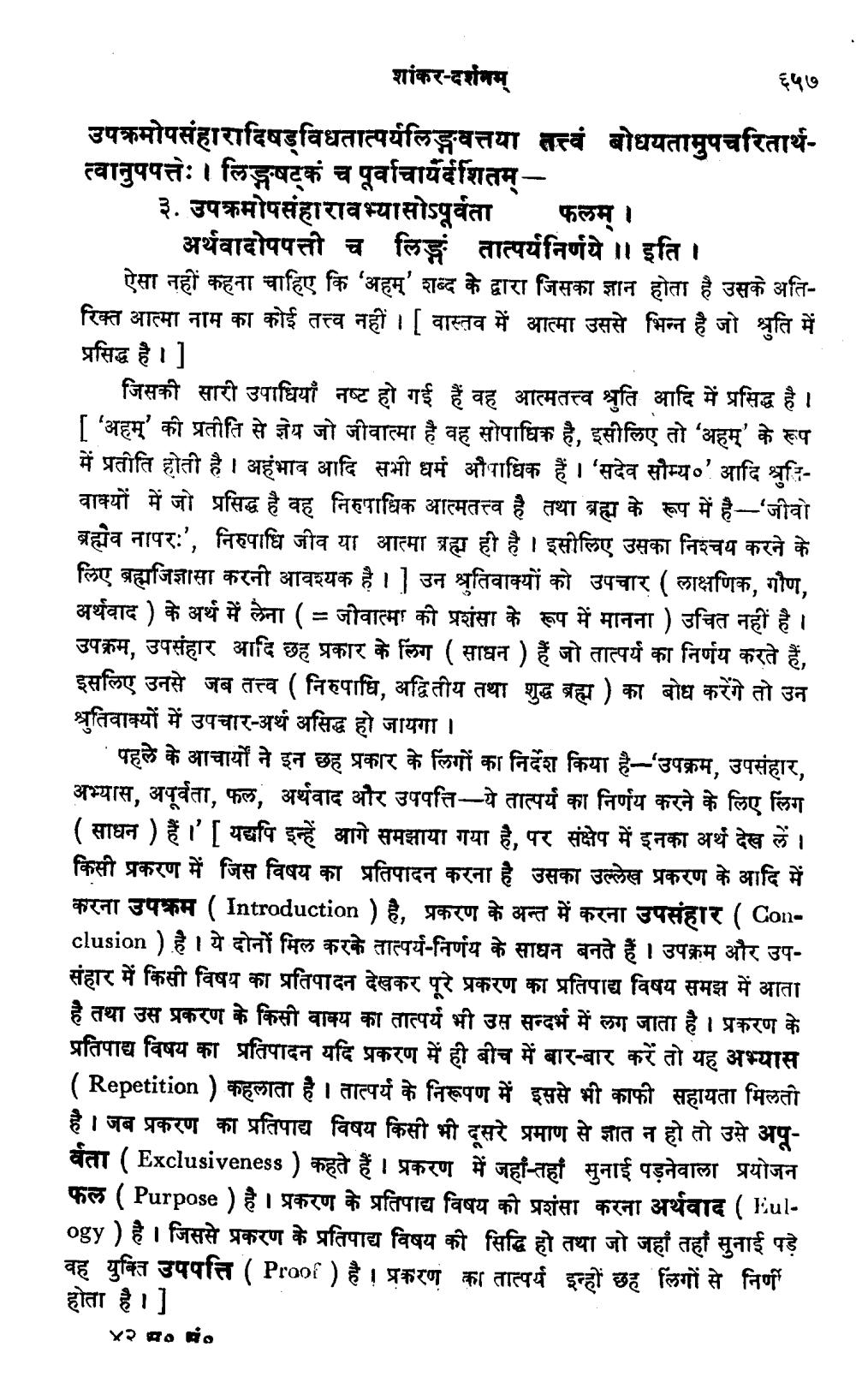________________
शांकर-दर्शनम्
६५७ उपक्रमोपसंहारादिषड्विधतात्पर्यलिङ्गवत्तया तत्त्वं बोधयतामुपचरितार्थत्वानुपपत्तेः । लिङ्गषट्कं च पूर्वाचार्यशितम्
३. उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् ।
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥ इति । ऐसा नहीं कहना चाहिए कि 'अहम्' शब्द के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसके अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई तत्त्व नहीं। [ वास्तव में आत्मा उससे भिन्न है जो श्रुति में प्रसिद्ध है।]
जिसकी सारी उपाधियाँ नष्ट हो गई हैं वह आत्मतत्त्व श्रुति आदि में प्रसिद्ध है । [ 'अहम्' की प्रतीति से ज्ञेय जो जीवात्मा है वह सोपाधिक है, इसीलिए तो 'अहम्' के रूप में प्रतीति होती है । अहंभाव आदि सभी धर्म औपाधिक हैं । 'सदेव सौम्य०' आदि श्रुतिवाक्यों में जो प्रसिद्ध है वह निरुपाधिक आत्मतत्त्व है तथा ब्रह्म के रूप में है-'जीवो ब्रह्मेव नापरः', निरुपाधि जीव या आत्मा ब्रह्म ही है । इसीलिए उसका निश्चय करने के लिए ब्रह्मजिज्ञासा करनी आवश्यक है। ] उन श्रुतिवाक्यों को उपचार ( लाक्षणिक, गौण, अर्थवाद ) के अर्थ में लेना ( = जीवात्मा की प्रशंसा के रूप में मानना ) उचित नहीं है। उपक्रम, उपसंहार आदि छह प्रकार के लिंग ( साधन ) हैं जो तात्पर्य का निर्णय करते हैं, इसलिए उनसे जब तत्त्व (निरुपाधि, अद्वितीय तथा शुद्ध ब्रह्म ) का बोध करेंगे तो उन श्रुतिवाक्यों में उपचार-अर्थ असिद्ध हो जायगा ।
पहले के आचार्यों ने इन छह प्रकार के लिंगों का निर्देश किया है-'उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति-ये तात्पर्य का निर्णय करने के लिए लिंग ( साधन ) हैं।' [ यद्यपि इन्हें आगे समझाया गया है, पर संक्षेप में इनका अर्थ देख लें। किसी प्रकरण में जिस विषय का प्रतिपादन करना है उसका उल्लेख प्रकरण के आदि में करना उपक्रम ( Introduction ) है, प्रकरण के अन्त में करना उपसंहार ( Conclusion ) है । ये दोनों मिल करके तात्पर्य-निर्णय के साधन बनते हैं । उपक्रम और उपसंहार में किसी विषय का प्रतिपादन देखकर पूरे प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय समझ में आता है तथा उस प्रकरण के किसी वाक्य का तात्पर्य भी उस सन्दर्भ में लग जाता है। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन यदि प्रकरण में ही बीच में बार-बार करें तो यह अभ्यास ( Repetition ) कहलाता है । तात्पर्य के निरूपण में इससे भी काफी सहायता मिलती है । जब प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय किसी भी दूसरे प्रमाण से ज्ञात न हो तो उसे अपू. वता ( Exclusiveness ) कहते हैं । प्रकरण में जहां-तहां सुनाई पड़नेवाला प्रयोजन फल ( Purpose ) है । प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय को प्रशंसा करना अर्थवाद ( Eulogy ) है । जिससे प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि हो तथा जो जहाँ तहाँ सुनाई पड़े वह युक्ति उपपत्ति ( Proof ) है । प्रकरण का तात्पर्य इन्हों छह लिंगों से निर्णी होता है।]
४२ ० ०