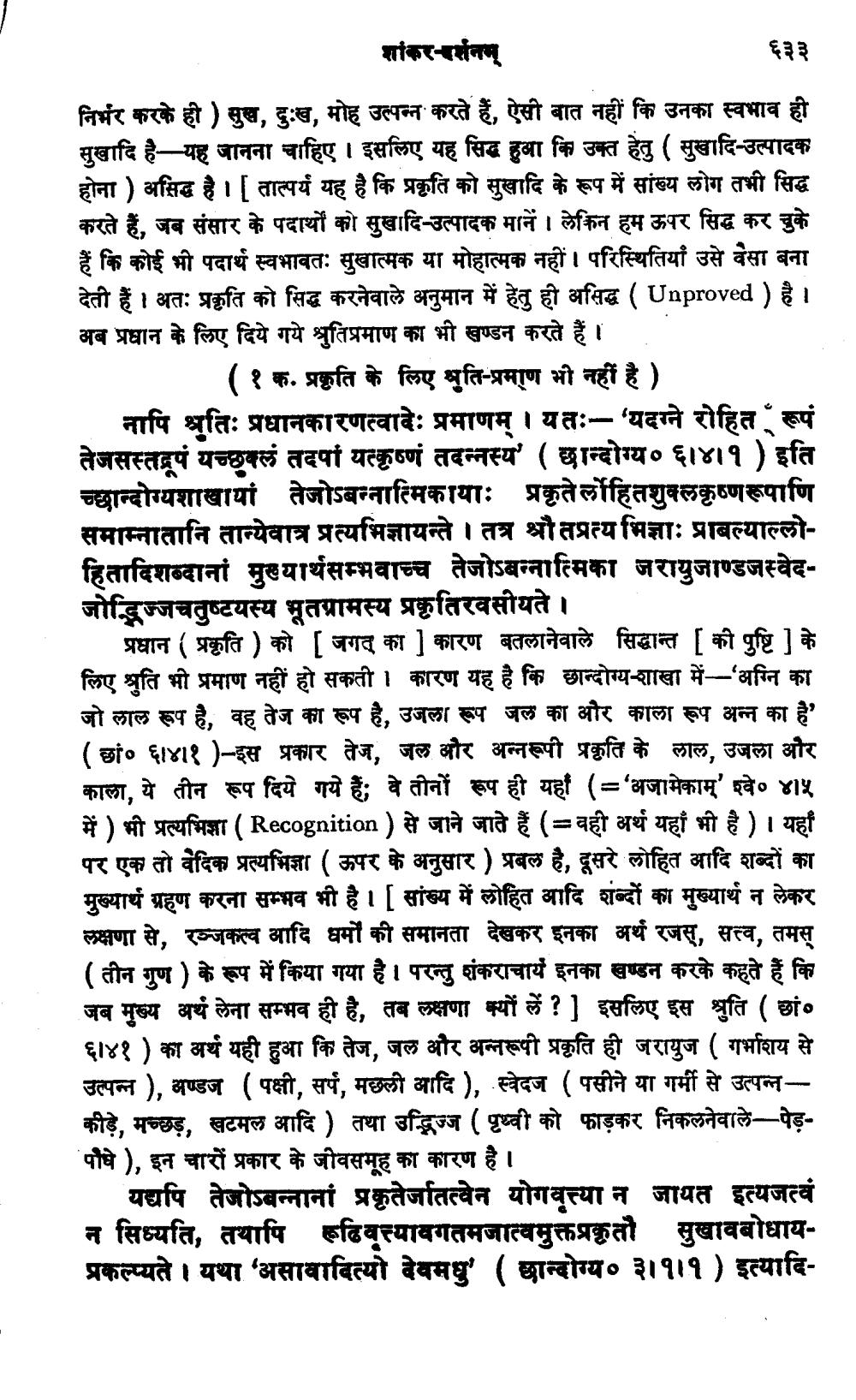________________
शांकर-दर्शनम्
६३३
निर्भर करके ही ) सुख, दुःख, मोह उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनका स्वभाव ही सुखादि है - यह जानना चाहिए । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उक्त हेतु ( सुखादि-उत्पादक होना ) असिद्ध है । [ तात्पर्य यह है कि प्रकृति को सुखादि के रूप में सांख्य लोग तभी सिद्ध करते हैं, जब संसार के पदार्थों को सुखादि उत्पादक मानें। लेकिन हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी पदार्थ स्वभावतः सुखात्मक या मोहात्मक नहीं । परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं । अतः प्रकृति को सिद्ध करनेवाले अनुमान में हेतु ही असिद्ध ( Unproved ) है | अब प्रधान के लिए दिये गये श्रुतिप्रमाण का भी खण्डन करते हैं ।
( १ क. प्रकृति के लिए श्रुति प्रमाण भी नहीं है )
नापि श्रुतिः प्रधानकारणत्वादेः प्रमाणम् । यतः - 'यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदर्पा यत्कृष्णं तदन्नस्य' ( छान्दोग्य० ६ |४| १ ) इति च्छान्दोग्यशाखायां तेजोबन्नात्मिकायाः प्रकृते र्लोहितशुक्लकृष्ण रूपाणि समाम्नातानि तान्येवात्र प्रत्यभिज्ञायन्ते । तत्र श्रौतप्रत्यभिज्ञा: प्राबल्याल्लोहितादिशब्दानां मुख्यार्थसम्भवाच्च तेजोऽबन्नात्मिका जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जचतुष्टयस्य भूतग्रामस्य प्रकृतिरवसीयते ।
प्रधान ( प्रकृति ) को [ जगत् का ] कारण बतलानेवाले सिद्धान्त [ की पुष्टि ] के लिए श्रुति भी प्रमाण नहीं हो सकती । कारण यह है कि छान्दोग्य - शाखा में - ' अग्नि का जो लाल रूप है, वह तेज का रूप है, उजला रूप जल का और काला रूप अन्न का है' ( छा० ६।४।१ ) - इस प्रकार तेज, जल और अन्नरूपी प्रकृति के लाल, उजला और काला, ये तीन रूप दिये गये हैं; वे तीनों रूप ही यहाँ ( = 'अजामेकाम्' श्वे० ४।५ में) भी प्रत्यभिज्ञा ( Recognition ) से जाने जाते हैं (= वही अर्थ यहाँ भी है ) । यहाँ पर एक तो वैदिक प्रत्यभिज्ञा ( ऊपर के अनुसार ) प्रबल है, दूसरे लोहित आदि शब्दों का मुख्यार्थ ग्रहण करना सम्भव भी है । [ सांख्य में लोहित आदि शब्दों का मुख्यार्थ न लेकर लक्षणा से, रञ्जकत्व आदि धर्मों की समानता देखकर इनका अर्थ रजस्, सत्त्व, तमस् ( तीन गुण ) के रूप में किया गया है। परन्तु शंकराचार्य इनका खण्डन करके कहते हैं कि जब मुख्य अर्थ लेना सम्भव ही है, तब लक्षणा क्यों लें ? ] इसलिए इस श्रुति ( छा० ६।४१ ) का अर्थ यही हुआ कि तेज, जल और अन्नरूपी प्रकृति ही जरायुज ( गर्भाशय से उत्पन्न ), अण्डज ( पक्षी, सर्प, मछली आदि ), स्वेदज ( पसीने या गर्मी से उत्पन्नकीड़े, मच्छड़, खटमल आदि ) तथा उद्भिज्ज ( पृथ्वी को फाड़कर निकलनेवाले - पेड़पौधे ), इन चारों प्रकार के जीवसमूह का कारण है ।
यद्यपि तेजोऽबन्नानां प्रकृतेर्जातत्वेन योगवृत्त्या न जायत इत्यजत्वं न सिध्यति, तथापि रुढिवस्यावगतमजात्वमुक्तप्रकृतौ सुखावबोधायप्रकल्प्यते । यथा 'असावादित्यो देवमधु' ( छान्दोग्य० ३।१।१ ) इत्यादि -
--