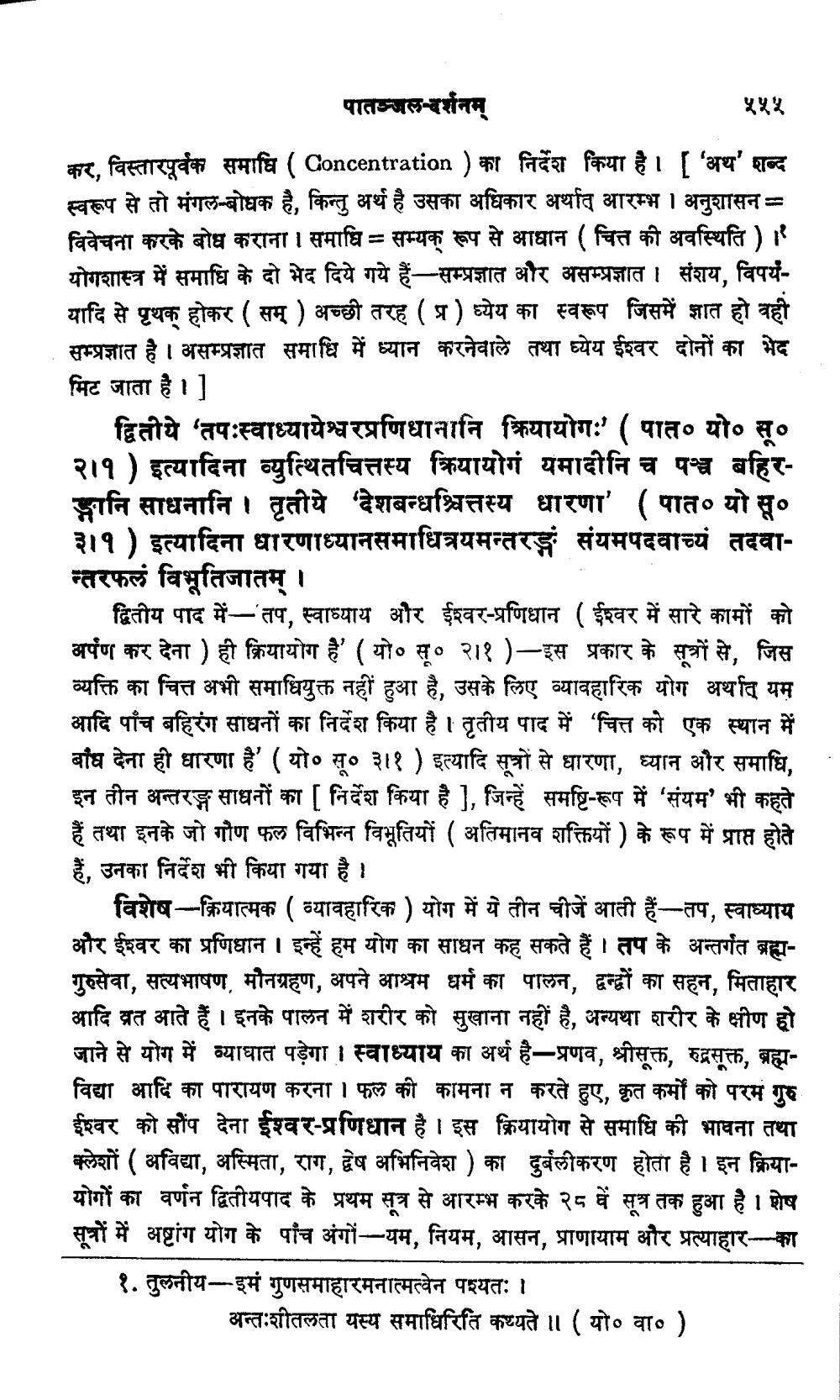________________
पातञ्जल-दर्शनम् कर, विस्तारपूर्वक समाधि ( Concentration ) का निर्देश किया है। [ 'अथ' शब्द स्वरूप से तो मंगल-बोधक है, किन्तु अर्थ है उसका अधिकार अर्थात् आरम्भ । अनुशासन = विवेचना करके बोध कराना । समाधि = सम्यक् रूप से आधान (चित्त की अवस्थिति )। योगशास्त्र में समाधि के दो भेद दिये गये हैं—सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात । संशय, विपर्ययादि से पृथक् होकर ( सम् ) अच्छी तरह (प्र) ध्येय का स्वरूप जिसमें ज्ञात हो वही सम्प्रज्ञात है । असम्प्रज्ञात समाधि में ध्यान करनेवाले तथा ध्येय ईश्वर दोनों का भेद मिट जाता है।]
द्वितीये 'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः' ( पात० यो० स० २११) इत्यादिना व्युत्थितचित्तस्य क्रियायोगं यमादीनि च पञ्च बहिरङ्गानि साधनानि । तृतीये 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' (पात० यो सू० ३११) इत्यादिना धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्ग संयमपदवाच्यं तदवान्तरफलं विभूतिजातम् ।
द्वितीय पाद में-तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ( ईश्वर में सारे कामों को अर्पण कर देना ) ही क्रियायोग है' ( यो० सू० २।१ )-इस प्रकार के सूत्रों से, जिस व्यक्ति का चित्त अभी समाधियुक्त नहीं हुआ है, उसके लिए व्यावहारिक योग अर्थात यम आदि पाँच बहिरंग साधनों का निर्देश किया है। तृतीय पाद में 'चित्त को एक स्थान में बांध देना ही धारणा है' ( यो० सू० ३।१ ) इत्यादि सूत्रों से धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीन अन्तरङ्ग साधनों का [ निर्देश किया है ], जिन्हें समष्टि-रूप में 'संयम' भी कहते हैं तथा इनके जो गौण फल विभिन्न विभूतियों ( अतिमानव शक्तियों ) के रूप में प्राप्त होते हैं, उनका निर्देश भी किया गया है।
विशेष-क्रियात्मक ( व्यावहारिक ) योग में ये तीन चीजें आती हैं-तप, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान । इन्हें हम योग का साधन कह सकते हैं । तप के अन्तर्गत ब्रह्मगुरुसेवा, सत्यभाषण, मौनग्रहण, अपने आश्रम धर्म का पालन, द्वन्द्वों का सहन, मिताहार आदि व्रत आते हैं । इनके पालन में शरीर को सुखाना नहीं है, अन्यथा शरीर के क्षीण हो जाने से योग में व्याघात पड़ेगा । स्वाध्याय का अर्थ है-प्रणव, श्रीसूक्त, रुद्रसूक्त, ब्रह्मविद्या आदि का पारायण करना । फल की कामना न करते हुए, कृत कर्मों को परम गुरु ईश्वर को सौंप देना ईश्वर-प्रणिधान है । इस क्रियायोग से समाधि की भावना तथा क्लेशों ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश ) का दुर्बलीकरण होता है। इन क्रियायोगों का वर्णन द्वितीयपाद के प्रथम सूत्र से आरम्भ करके २८ वें सूत्र तक हुआ है । शेष सूत्रों में अष्टांग योग के पांच अंगों-यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार-का १. तुलनीय-इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः ।
अन्तःशीतलता यस्य समाधिरिति कथ्यते ।। ( यो० वा० )