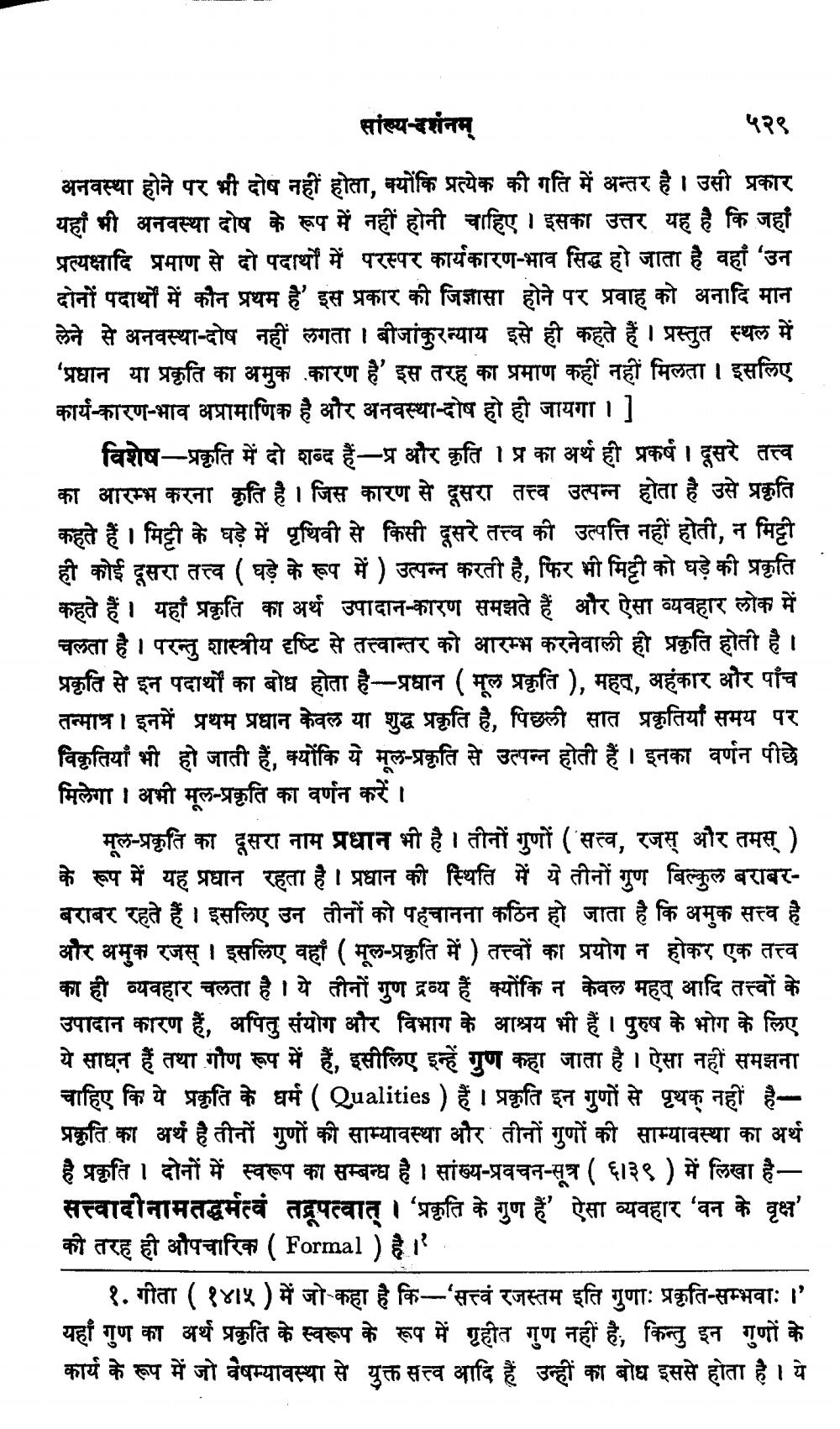________________
सांख्य दर्शनम्
५२९ अनवस्था होने पर भी दोष नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक की गति में अन्तर है । उसी प्रकार यहाँ भी अनवस्था दोष के रूप में नहीं होनी चाहिए । इसका उत्तर यह है कि जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण से दो पदार्थों में परस्पर कार्यकारण-भाव सिद्ध हो जाता है वहाँ 'उन दोनों पदार्थों में कौन प्रथम है' इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष नहीं लगता । बीजांकुरन्याय इसे ही कहते हैं । प्रस्तुत स्थल में 'प्रधान या प्रकृति का अमुक कारण है' इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं मिलता । इसलिए कार्य-कारण-भाव अप्रामाणिक है और अनवस्था-दोष हो हो जायगा । ]
विशेष-प्रकृति में दो शब्द हैं-प्र और कृति । प्र का अर्थ ही प्रकर्ष । दूसरे तत्त्व का आरम्भ करना कृति है । जिस कारण से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है उसे प्रकृति कहते हैं । मिट्टी के घड़े में पृथिवी से किसी दूसरे तत्त्व की उत्पत्ति नहीं होती, न मिट्टी ही कोई दूसरा तत्त्व (घड़े के रूप में ) उत्पन्न करती है, फिर भी मिट्टी को घड़े की प्रकृति कहते हैं। यहाँ प्रकृति का अर्थ उपादान-कारण समझते हैं और ऐसा व्यवहार लोक में चलता है । परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से तत्त्वान्तर को आरम्भ करनेवाली ही प्रकृति होती है । प्रकृति से इन पदार्थों का बोध होता है-प्रधान ( मूल प्रकृति ), महत्', अहंकार और पाँच तन्मात्र। इनमें प्रथम प्रधान केवल या शुद्ध प्रकृति है, पिछली सात प्रकृतियां समय पर विकृतियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि ये मूल-प्रकृति से उत्पन्न होती हैं । इनका वर्णन पीछे मिलेगा। अभी मूल-प्रकृति का वर्णन करें। __मूल-प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान भी है। तीनों गुणों (सत्व, रजस् और तमस् ) के रूप में यह प्रधान रहता है। प्रधान की स्थिति में ये तीनों गुण बिल्कुल बराबरबराबर रहते हैं । इसलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो जाता है कि अमुक सत्त्व है और अमुक रजस् । इसलिए वहाँ ( मूल-प्रकृति में ) तत्त्वों का प्रयोग न होकर एक तत्त्व का ही व्यवहार चलता है। ये तीनों गुण द्रव्य हैं क्योंकि न केवल महत् आदि तत्त्वों के उपादान कारण हैं, अपितु संयोग और विभाग के आश्रय भी हैं । पुरुष के भोग के लिए ये साधन हैं तथा गौण रूप में हैं, इसीलिए इन्हें गुण कहा जाता है । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये प्रकृति के धर्म ( Qualities ) हैं । प्रकृति इन गुणों से पृथक् नहीं हैप्रकृति का अर्थ है तीनों गुणों की साम्यावस्था और तीनों गुणों की साम्यावस्था का अर्थ है प्रकृति । दोनों में स्वरूप का सम्बन्ध है । सांख्य-प्रवचन-सूत्र ( ६।३९ ) में लिखा हैसत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात् । 'प्रकृति के गुण हैं' ऐसा व्यवहार 'वन के वृक्ष' की तरह ही औपचारिक ( Formal ) है। ..
१. गीता ( १४१५ ) में जो कहा है कि-'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति-सम्भवाः ।' यहाँ गुण का अर्थ प्रकृति के स्वरूप के रूप में गृहीत गुण नहीं है, किन्तु इन गुणों के कार्य के रूप में जो वैषम्यावस्था से युक्त सत्त्व आदि हैं उन्हीं का बोध इससे होता है। ये