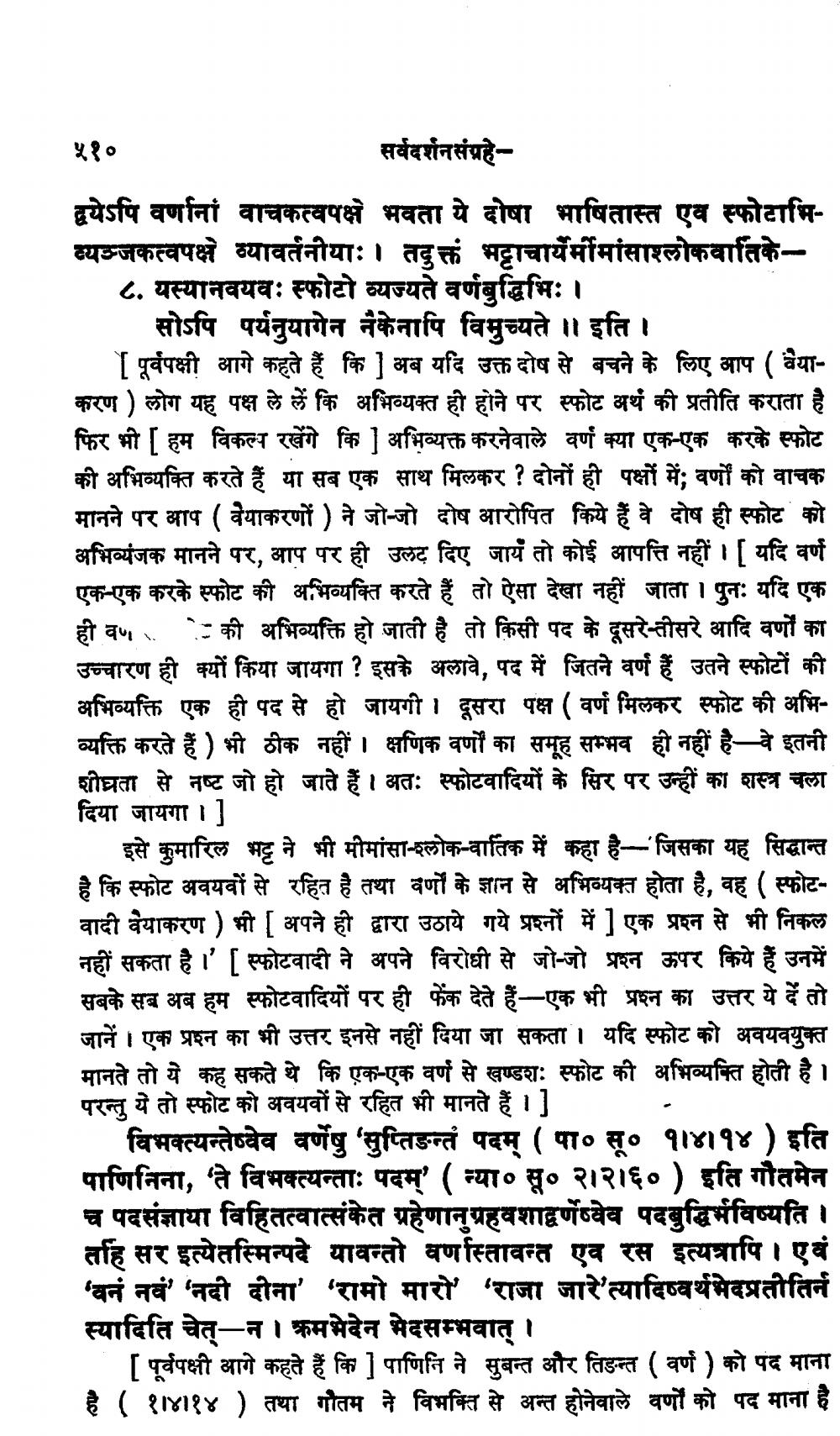________________
५१०
सर्वदर्शनसंग्रहेद्वयेऽपि वर्णानां वाचकत्वपक्षे भवता ये दोषा भाषितास्त एव स्फोटाभिव्यञ्जकत्वपक्षे व्यावर्तनीयाः। तदुक्तं भट्टाचार्यर्मीमांसाश्लोकवातिके८. यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः।
सोऽपि पर्यनुयागेन नैकेनापि विमुच्यते ॥ इति । [ पूर्वपक्षी आगे कहते हैं कि ] अब यदि उक्त दोष से बचने के लिए आप ( वैयाकरण ) लोग यह पक्ष ले लें कि अभिव्यक्त ही होने पर स्फोट अर्थ की प्रतीति कराता है फिर भी [ हम विकल्प रखेंगे कि ] अभिव्यक्त करनेवाले वर्ण क्या एक-एक करके स्फोट की अभिव्यक्ति करते हैं या सब एक साथ मिलकर ? दोनों ही पक्षों में; वर्णों को वाचक मानने पर आप ( वैयाकरणों) ने जो-जो दोष आरोपित किये हैं वे दोष ही स्फोट को अभिव्यंजक मानने पर, आप पर ही उलट दिए जायं तो कोई आपत्ति नहीं। [ यदि वर्ण एक-एक करके स्फोट की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा देखा नहीं जाता । पुनः यदि एक ही व.. की अभिव्यक्ति हो जाती है तो किसी पद के दूसरे-तीसरे आदि वर्णों का उच्चारण ही क्यों किया जायगा ? इसके अलावे, पद में जितने वर्ण हैं उतने स्फोटों की अभिव्यक्ति एक ही पद से हो जायगी। दूसरा पक्ष ( वर्ण मिलकर स्फोट की अभिव्यक्ति करते हैं ) भी ठीक नहीं। क्षणिक वर्णों का समूह सम्भव ही नहीं है वे इतनी शीघ्रता से नष्ट जो हो जाते हैं। अतः स्फोटवादियों के सिर पर उन्हीं का शस्त्र चला दिया जायगा।]
इसे कुमारिल भट्ट ने भी मीमांसा-श्लोक-वार्तिक में कहा है- जिसका यह सिद्धान्त है कि स्फोट अवयवों से रहित है तथा वर्णों के ज्ञान से अभिव्यक्त होता है, वह ( स्फोटवादी वैयाकरण ) भी [ अपने ही द्वारा उठाये गये प्रश्नों में ] एक प्रश्न से भी निकल नहीं सकता है।' [स्फोटवादी ने अपने विरोधी से जो-जो प्रश्न ऊपर किये हैं उनमें सबके सब अब हम स्फोटवादियों पर ही फेंक देते हैं-एक भी प्रश्न का उत्तर ये दें तो जानें । एक प्रश्न का भी उत्तर इनसे नहीं दिया जा सकता। यदि स्फोट को अवयवयुक्त मानते तो ये कह सकते थे कि एक-एक वर्ण से खण्डशः स्फोट की अभिव्यक्ति होती है। परन्तु ये तो स्फोट को अवयवों से रहित भी मानते हैं । ]
विभक्त्यन्तेष्वेव वर्णेषु 'सुप्तिङन्तं पदम् ( पा० सू० १।४।१४) इति पाणिनिना, 'ते विभक्त्यन्ताः पदम्' (न्या० सू० २।२।६०) इति गौतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्संकेत ग्रहेणानुग्रहवशाद्वर्णेष्वेव पदबुद्धिर्भविष्यति । तहि सर इत्येतस्मिन्पदे यावन्तो वस्तावन्त एव रस इत्यत्रापि । एवं 'वनं नवं 'नदी दीना' 'रामो मारों' 'राजा जारे'त्यादिष्वर्थभेवप्रतीतिर्न स्यादिति चेत्-न । क्रमभेदेन भेदसम्भवात् ।
[पूर्वपक्षी आगे कहते हैं कि ] पाणिनि ने सुबन्त और तिङन्त ( वर्ण ) को पद माना है ( १।४।१४ ) तथा गौतम ने विभक्ति से अन्त होनेवाले वर्षों को पद माना है