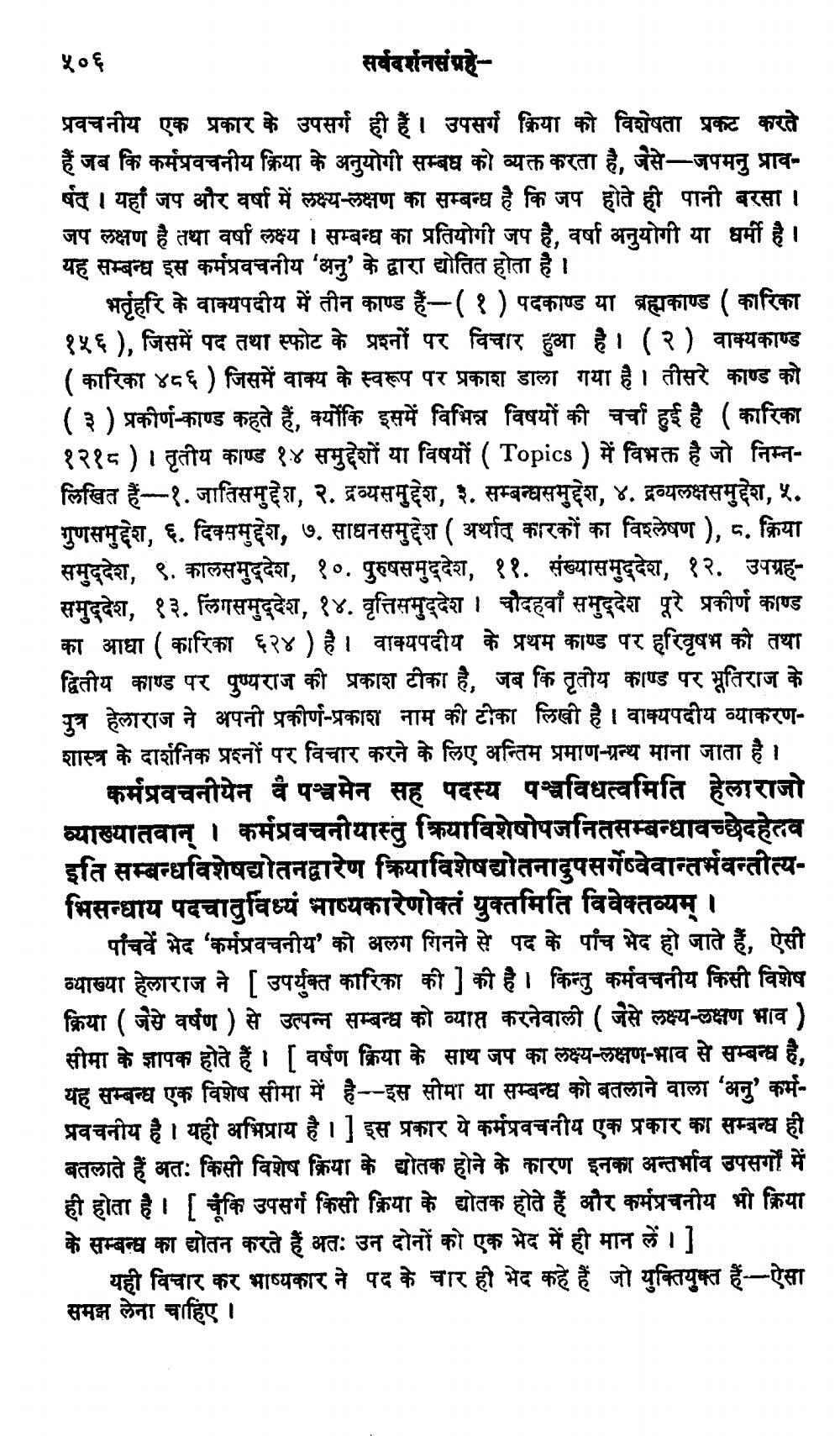________________
५०६
सर्वदर्शनसंग्रहे
प्रवचनीय एक प्रकार के उपसर्ग ही हैं । उपसर्ग क्रिया को विशेषता प्रकट करते हैं जब कि कर्मप्रवचनीय क्रिया के अनुयोगी सम्बध को व्यक्त करता है, जैसे—जपमनु प्रावर्षत । यहाँ जप और वर्षा में लक्ष्य-लक्षण का सम्बन्ध है कि जप होते ही पानी बरसा । जप लक्षण है तथा वर्षा लक्ष्य । सम्बन्ध का प्रतियोगी जप है, वर्षा अनुयोगी या धर्मी है । यह सम्बन्ध इस कर्मप्रवचनीय 'अनु' के द्वारा द्योतित होता है ।
भर्तृहरि के वाक्यपदीय में तीन काण्ड हैं - ( १ ) पदकाण्ड या ब्रह्मकाण्ड ( कारिका १५६ ), जिसमें पद तथा स्फोट के प्रश्नों पर विचार हुआ है । ( २ ) वाक्य काण्ड ( कारिका ४८६ ) जिसमें वाक्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । तीसरे काण्ड को ( ३ ) प्रकीर्ण - काण्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न विषयों की चर्चा हुई है ( कारिका १२१८ ) । तृतीय काण्ड १४ समुद्देशों या विषयों ( Topics ) में विभक्त है जो निम्नलिखित हैं- १. जातिसमुद्देश, २. द्रव्यसमुद्देश, ३. सम्बन्धसमुद्देश, ४. द्रव्यलक्षसमुद्देश, ५. गुणसमुद्देश, ६. दिक्समुद्देश, ७. साधनसमुद्देश ( अर्थात् कारकों का विश्लेषण ), ८. क्रिया समुद्देश, ९. कालसमुद्देश, १०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुद्देश, १२. उपग्रहसमुद्देश, १३. लिंगसमुद्देश, १४. वृत्तिसमुद्देश । चौदहवाँ समुद्देश पूरे प्रकीर्ण काण्ड का आधा ( कारिका ६२४ ) है । वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड पर हरिवृषभ को तथा द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की प्रकाश टीका है, जब कि तृतीय काण्ड पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने अपनी प्रकीर्ण- प्रकाश नाम की टीका लिखी है । वाक्यपदीय व्याकरणशास्त्र के दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए अन्तिम प्रमाण-ग्रन्थ माना जाता है ।
कर्मप्रवचनीयेन वै पश्वमेन सह पदस्य पश्वविधत्वमिति हेलाराजो व्याख्यातवान् । कर्मप्रवचनीयास्तु क्रियाविशेषोपजनितसम्बन्धावच्छेदहेतव इति सम्बन्धविशेषद्योतनद्वारेण क्रियाविशेषद्योतनादुपसर्गेष्वेवान्तर्भवन्तीत्यभिसन्धाय पदचातुविध्यं भाष्यकारेणोक्तं युक्तमिति विवेक्तव्यम् ।
पाँचवें भेद 'कर्मप्रवचनीय' को अलग गिनने से पद के पांच भेद हो जाते हैं, ऐसी व्याख्या हेलाराज ने [ उपर्युक्त कारिका की ] की है । किन्तु कर्मवचनीय किसी विशेष क्रिया ( जैसे वर्षण ) से उत्पन्न सम्बन्ध को व्याप्त करनेवाली ( जैसे लक्ष्य-लक्षण भाव ) सीमा के ज्ञापक होते हैं । [ वर्षण क्रिया के साथ जप का लक्ष्य-लक्षण-भाव से सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध एक विशेष सीमा में है - इस सीमा या सम्बन्ध को बतलाने वाला 'अनु' कर्मप्रवचनीय है । यही अभिप्राय है । ] इस प्रकार ये कर्मप्रवचनीय एक प्रकार का सम्बन्ध ही बतलाते हैं अत: किसी विशेष क्रिया के द्योतक होने के कारण इनका अन्तर्भाव उपसर्गों में ही होता है । [ चूँकि उपसर्ग किसी क्रिया के द्योतक होते हैं और कर्मप्रचनीय भी क्रिया के सम्बन्ध का द्योतन करते हैं अतः उन दोनों को एक भेद में ही मान लें । ]
यही विचार कर भाष्यकार ने पद के चार ही भेद कहे हैं जो युक्तियुक्त हैं - ऐसा समझ लेना चाहिए ।