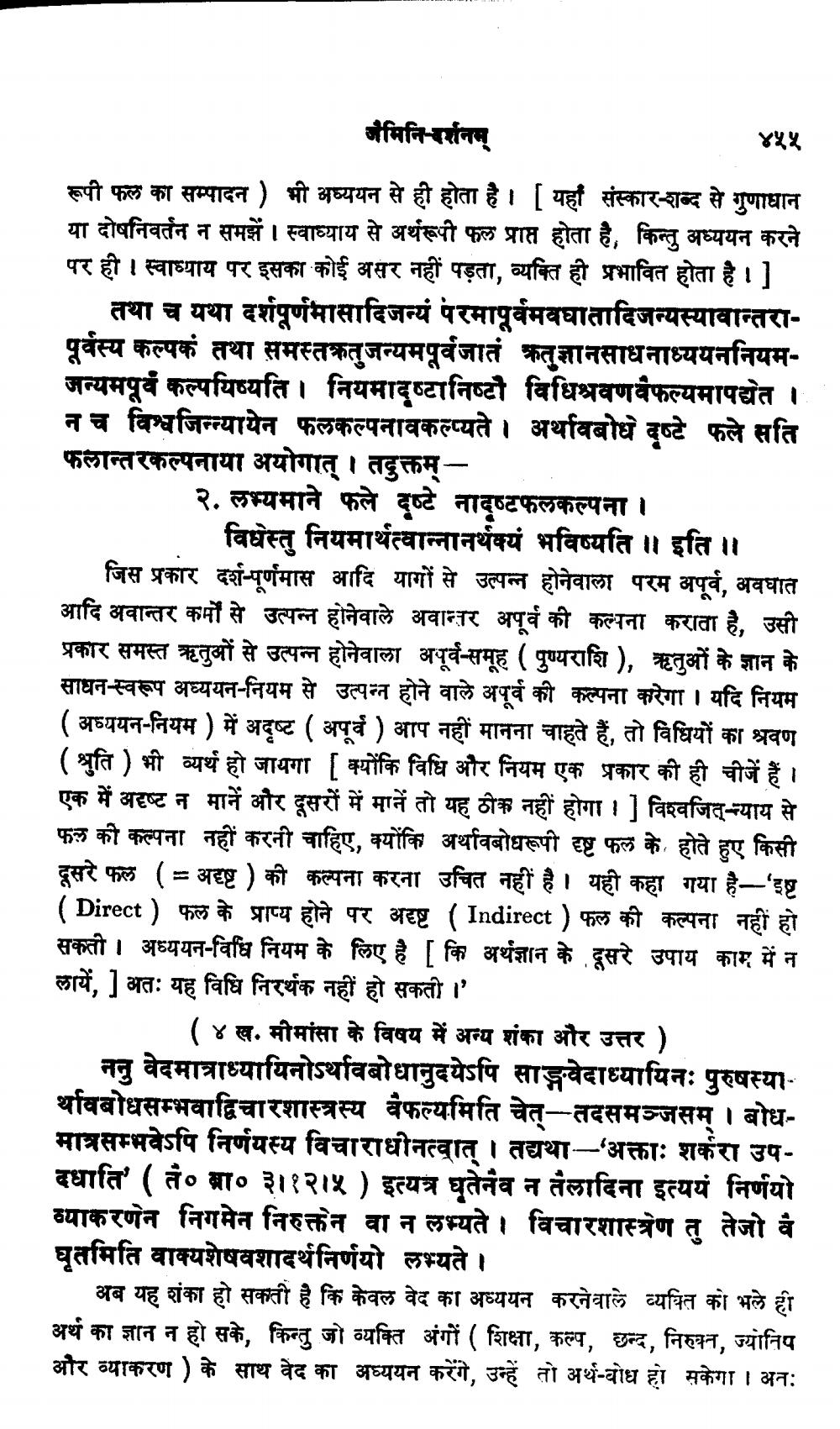________________
जैमिनि-पर्शनम्
४५५
रूपी फल का सम्पादन ) भी अध्ययन से ही होता है। [ यहाँ संस्कार-शब्द से गुणाधान या दोषनिवर्तन न समझें । स्वाध्याय से अर्थरूपी फल प्राप्त होता है, किन्तु अध्ययन करने पर ही । स्वाध्याय पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, व्यक्ति ही प्रभावित होता है।]
तथा च यथा दर्शपूर्णमासादिजन्यं परमापूर्वमवघातादिजन्यस्यावान्तरापूर्वस्य कल्पकं तथा समस्तऋतुजन्यमपूर्वजातं ऋतुज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यमपूर्व कल्पयिष्यति। नियमादृष्टानिष्टौ विधिश्रवणवैफल्यमापद्येत । न च विश्वजिन्न्यायेन फलकल्पनावकल्प्यते। अर्थावबोधे दृष्टे फले सति फलान्तरकल्पनाया अयोगात् । तदुक्तम्
२. लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्टफलकल्पना ।
विधेस्तु नियमार्थत्वान्नानर्थक्यं भविष्यति ॥ इति ॥ जिस प्रकार दर्श-पूर्णमास आदि यागों से उत्पन्न होनेवाला परम अपूर्व, अवघात आदि अवान्तर कर्मों से उत्पन्न होनेवाले अवानर अपूर्व की कल्पना कराता है, उसी प्रकार समस्त ऋतुओं से उत्पन्न होनेवाला अपूर्व-समूह ( पुण्यराशि ), ऋतुओं के ज्ञान के साधन-स्वरूप अध्ययन-नियम से उत्पन्न होने वाले अपूर्व की कल्पना करेगा । यदि नियम ( अध्ययन-नियम ) में अदृष्ट ( अपूर्व ) आप नहीं मानना चाहते हैं, तो विधियों का श्रवण (श्रुति ) भी व्यर्थ हो जायगा [क्योंकि विधि और नियम एक प्रकार की ही चीजें हैं । एक में अदृष्ट न मानें और दूसरों में मानें तो यह ठीक नहीं होगा। ] विश्वजित्-न्याय से फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थावबोधरूपी दृष्ट फल के होते हुए किसी दूसरे फल (= अदृष्ट ) की कल्पना करना उचित नहीं है। यही कहा गया है-'इष्ट ( Direct ) फल के प्राप्य होने पर अदृष्ट ( Indirect ) फल की कल्पना नहीं हो सकती। अध्ययन-विधि नियम के लिए है [ कि अर्थज्ञान के दूसरे उपाय काम में न लायें, ] अतः यह विधि निरर्थक नहीं हो सकती।'
(४ ख. मीमांसा के विषय में अन्य शंका और उत्तर ) ननु वेदमात्राध्यायिनोऽर्थावबोधानुदयेऽपि साङ्गवेदाध्यायिनः पुरुषस्यार्थावबोधसम्भवाद्विचारशास्त्रस्य वैफल्यमिति चेत्-तदसमञ्जसम् । बोधमात्रसम्भवेऽपि निर्णयस्य विचाराधीनत्वात् । तद्यथा-'अक्ताः शर्करा उपदधाति' (ले० प्रा० ३।१२।५ ) इत्यत्र घृतेनैव न तैलादिना इत्ययं निर्णयो व्याकरणेन निगमेन निरुक्तेन वा न लभ्यते। विचारशास्त्रेण तु तेजो वै घृतमिति वाक्यशेषवशादर्थनिर्णयो लभ्यते। ___ अब यह शंका हो सकती है कि केवल वेद का अध्ययन करनेवाले व्यक्ति को भले ही अर्थ का ज्ञान न हो सके, किन्तु जो व्यक्ति अंगों ( शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण ) के साथ वेद का अध्ययन करेंगे, उन्हें तो अर्थ-वोध हो सकेगा । अत: