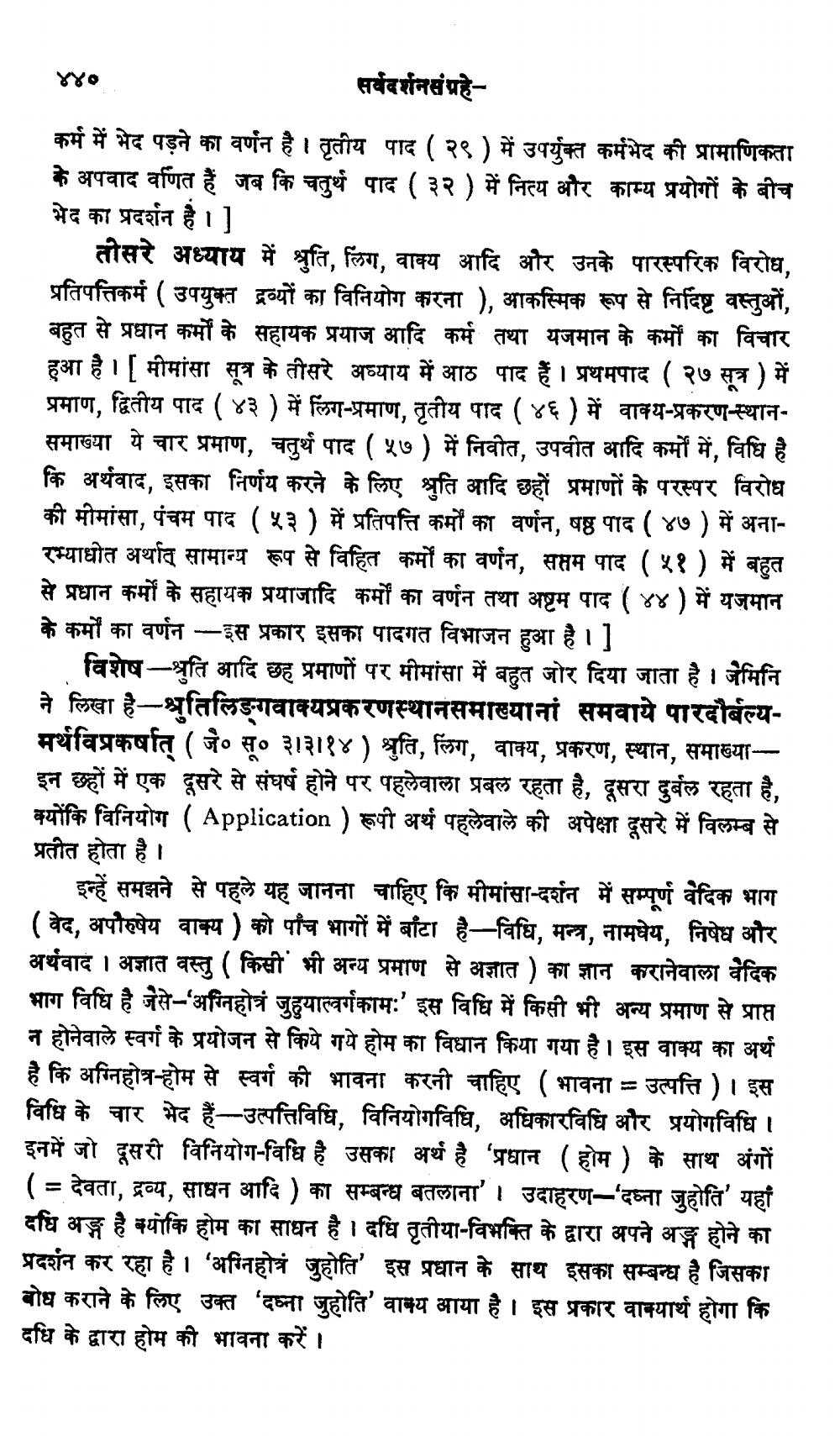________________
४४०
सर्वदर्शनसंग्रहे
कर्म में भेद पड़ने का वर्णन है। तृतीय पाद ( २९ ) में उपर्युक्त कर्मभेद की प्रामाणिकता के अपवाद वर्णित हैं जब कि चतुर्थ पाद ( ३२ ) में नित्य और काम्य प्रयोगों के बीच भेद का प्रदर्शन है।]
तीसरे अध्याय में श्रुति, लिंग, वाक्य आदि और उनके पारस्परिक विरोध, प्रतिपत्तिकर्म ( उपयुक्त द्रव्यों का विनियोग करना ), आकस्मिक रूप से निर्दिष्ट वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मों के सहायक प्रयाज आदि कर्म तथा यजमान के कर्मों का विचार हुआ है। [ मीमांसा सूत्र के तीसरे अध्याय में आठ पाद हैं । प्रथमपाद ( २७ सूत्र ) में प्रमाण, द्वितीय पाद ( ४३ ) में लिंग-प्रमाण, तृतीय पाद ( ४६ ) में वाक्य-प्रकरण-स्थानसमाख्या ये चार प्रमाण, चतुर्थ पाद ( ५७ ) में निवीत, उपवीत आदि कर्मों में, विधि है कि अर्थवाद, इसका निर्णय करने के लिए श्रुति आदि छहों प्रमाणों के परस्पर विरोध की मीमांसा, पंचम पाद ( ५३ ) में प्रतिपत्ति कर्मों का वर्णन, षष्ठ पाद ( ४७ ) में अनारभ्याधीत अर्थात् सामान्य रूप से विहित कर्मों का वर्णन, सप्तम पाद ( ५१ ) में बहुत से प्रधान कर्मों के सहायक प्रयाजादि कर्मों का वर्णन तथा अष्टम पाद ( ४४ ) में यजमान के कर्मों का वर्णन -इस प्रकार इसका पादगत विभाजन हुआ है। ]
विशेष-श्रुति आदि छह प्रमाणों पर मीमांसा में बहुत जोर दिया जाता है । जेमिनि ने लिखा है-श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात् ( जै० सू० ३।३।१४ ) श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्याइन छहों में एक दूसरे से संघर्ष होने पर पहलेवाला प्रबल रहता है, दूसरा दुर्बल रहता है, क्योंकि विनियोग ( Application ) रूपी अर्थ पहलेवाले की अपेक्षा दूसरे में विलम्ब से प्रतीत होता है।
इन्हें समझने से पहले यह जानना चाहिए कि मीमांसा-दर्शन में सम्पूर्ण वैदिक भाग ( वेद, अपौरुषेय वाक्य ) को पांच भागों में बांटा है-विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद । अज्ञात वस्तु ( किसी भी अन्य प्रमाण से अज्ञात ) का ज्ञान करानेवाला वैदिक भाग विधि है जैसे-'अग्निहोत्रं जुहुयात्वर्गकामः' इस विधि में किसी भी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होनेवाले स्वर्ग के प्रयोजन से किये गये होम का विधान किया गया है। इस वाक्य का अर्थ है कि अग्निहोत्र-होम से स्वर्ग की भावना करनी चाहिए ( भावना = उत्पत्ति ) । इस विधि के चार भेद हैं-उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि और प्रयोगविधि । इनमें जो दूसरी विनियोग-विधि है उसका अर्थ है 'प्रधान (होम ) के साथ अंगों ( = देवता, द्रव्य, साधन आदि ) का सम्बन्ध बतलाना' । उदाहरण-'दना जुहोति' यहां दधि अङ्ग है क्योकि होम का साधन है । दधि तृतीया-विभक्ति के द्वारा अपने अङ्ग होने का प्रदर्शन कर रहा है । 'अग्निहोत्रं जुहोति' इस प्रधान के साथ इसका सम्बन्ध है जिसका बोध कराने के लिए उक्त 'दध्ना जुहोति' वाक्य आया है। इस प्रकार वाक्यार्थ होगा कि दधि के द्वारा होम की भावना करें।