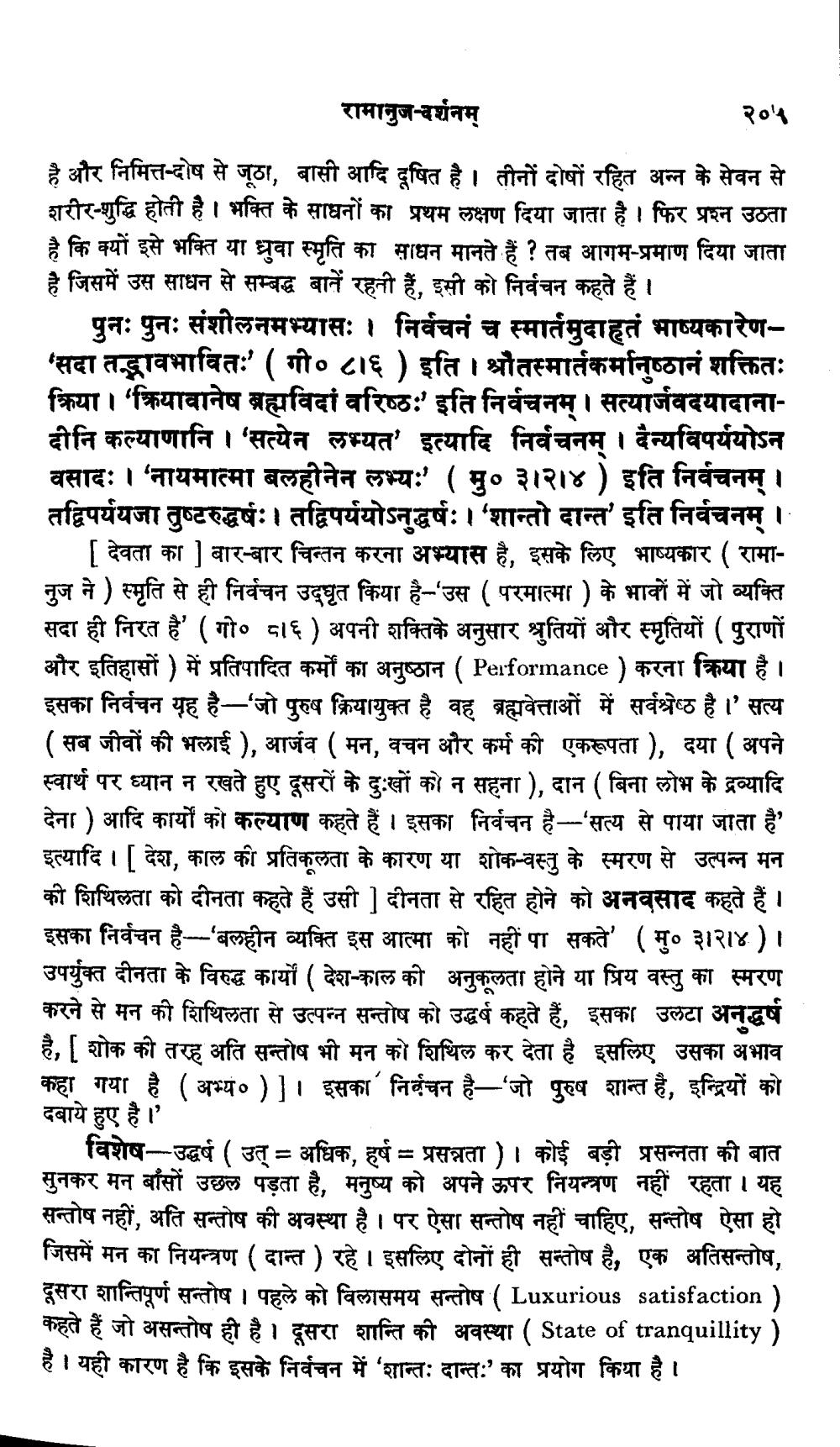________________
रामानुज-चर्शनम्
२०५
है और निमित्त-दोष से जूठा, बासी आदि दूषित है। तीनों दोषों रहित अन्न के सेवन से शरीर-शुद्धि होती है । भक्ति के साधनों का प्रथम लक्षण दिया जाता है । फिर प्रश्न उठता है कि क्यों इसे भक्ति या ध्रुवा स्मृति का साधन मानते हैं ? तब आगम-प्रमाण दिया जाता है जिसमें उस साधन से सम्बद्ध बातें रहती हैं, इसी को निर्वचन कहते हैं।
पुनः पुनः संशोलनमभ्यासः । निर्वचनं च स्मार्तमुदाहृतं भाष्यकारेण'सदा तद्भावभावितः' ( गी० ८।६ ) इति । श्रौतस्मातकर्मानुष्ठानं शक्तितः क्रिया। 'क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः' इति निर्वचनम् । सत्यार्जवदयादानादीनि कल्याणानि । 'सत्येन लभ्यत' इत्यादि निर्वचनम् । दैन्यविपर्ययोऽन वसादः । 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' (मु० ३।२।४) इति निर्वचनम् । तद्विपर्ययजा तुष्टरुद्धर्षः। तद्विपर्ययोऽनुद्धर्षः। 'शान्तो दान्त' इति निर्वचनम् ।
[ देवता का ] बार-बार चिन्तन करना अभ्यास है, इसके लिए भाष्यकार ( रामानुज ने ) स्मृति से ही निर्वचन उद्धृत किया है-'उस (परमात्मा ) के भावों में जो व्यक्ति सदा ही निरत है' ( गो० ८।६ ) अपनी शक्तिके अनुसार श्रुतियों और स्मृतियों ( पुराणों और इतिहासों) में प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान ( Performance ) करना क्रिया है । इसका निर्वचन यह है—'जो पुरुष क्रियायुक्त है वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है ।' सत्य ( सब जीवों की भलाई ), आर्जव ( मन, वचन और कर्म की एकरूपता), दया ( अपने स्वार्थ पर ध्यान न रखते हुए दूसरों के दुःखों को न सहना), दान ( बिना लोभ के द्रव्यादि देना ) आदि कार्यों को कल्याण कहते हैं । इसका निर्वचन है-'सत्य से पाया जाता है। इत्यादि । [ देश, काल की प्रतिकूलता के कारण या शोक-वस्तु के स्मरण से उत्पन्न मन की शिथिलता को दीनता कहते हैं उसी ] दीनता से रहित होने को अनवसाद कहते हैं । इसका निर्वचन है-'बलहीन व्यक्ति इस आत्मा को नहीं पा सकते' (मु० ३।२।४) । उपर्युक्त दीनता के विरुद्ध कार्यों ( देश-काल को अनुकूलता होने या प्रिय वस्तु का स्मरण करने से मन की शिथिलता से उत्पन्न सन्तोष को उद्धर्ष कहते हैं, इसका उलटा अनद्धषं है, [ शोक की तरह अति सन्तोष भी मन को शिथिल कर देता है इसलिए उसका अभाव कहा गया है ( अभ्य० )]। इसका निर्वचन है—'जो पुरुष शान्त है, इन्द्रियों को दबाये हुए है।'
विशेष-उद्धर्ष ( उत् = अधिक, हर्ष = प्रसन्नता )। कोई बड़ी प्रसन्नता की बात सुनकर मन बाँसों उछल पड़ता है, मनुष्य को अपने ऊपर नियन्त्रण नहीं रहता । यह सन्तोष नहीं, अति सन्तोष की अवस्था है । पर ऐसा सन्तोष नहीं चाहिए, सन्तोष ऐसा हो जिसमें मन का नियन्त्रण ( दान्त ) रहे । इसलिए दोनों ही सन्तोष है, एक अतिसन्तोष, दूसरा शान्तिपूर्ण सन्तोष । पहले को विलासमय सन्तोष ( Luxurious satisfaction ) कहते हैं जो असन्तोष ही है। दूसरा शान्ति की अवस्था ( State of tranquillity ) है । यही कारण है कि इसके निर्वचन में 'शान्तः दान्तः' का प्रयोग किया है।