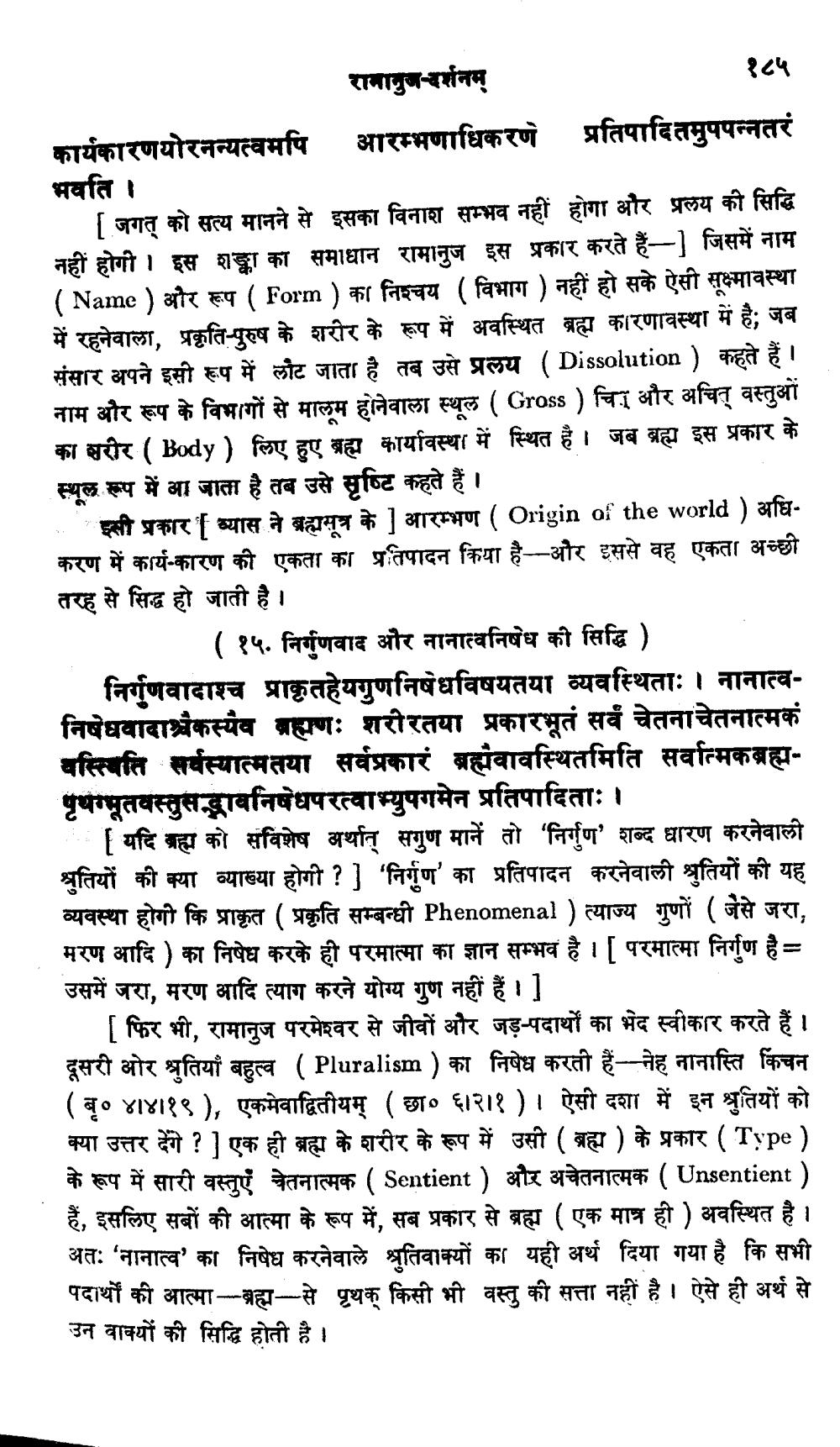________________
रामानुज-दर्शनम्
१८५ कार्यकारणयोरनन्यत्वमपि आरम्भणाधिकरणे प्रतिपादितमुपपन्नतरं भवति ।
[ जगत् को सत्य मानने से इसका विनाश सम्भव नहीं होगा और प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। इस शङ्का का समाधान रामानुज इस प्रकार करते हैं-] जिसमें नाम ( Name ) और रूप ( Form ) का निश्चय (विभाग ) नहीं हो सके ऐसी सूक्ष्मावस्था में रहनेवाला, प्रकृति-पुरुष के शरीर के रूप में अवस्थित ब्रह्म कारणावस्था में है; जब संसार अपने इसी रूप में लौट जाता है तब उसे प्रलय ( Dissolution ) कहते हैं । नाम और रूप के विभागों से मालूम होनेवाला स्थूल ( Gross ) चिा और अचित् वस्तुओं का शरीर ( Body ) लिए हुए ब्रह्म कार्यावस्था में स्थित है। जब ब्रह्म इस प्रकार के स्थूल रूप में आ जाता है तब उसे सृष्टि कहते हैं। .. इसी प्रकार [ व्यास ने ब्रह्मसूत्र के ] आरम्भण ( Origin of the world ) अधिकरण में कार्य-कारण की एकता का प्रतिपादन किया है और इससे वह एकता अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है।
(१५. निर्गणवाद और नानात्वनिषेध की सिद्धि ) निर्गुणवादाश्च प्राकृतहेयगुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः । नानात्वनिषेधवादाश्चैकस्यैव ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सर्व चेतनाचेतनात्मकं वस्थिति सर्वस्यात्मतया सर्वप्रकारं ब्रह्मवावस्थितमिति सर्वात्मकब्रह्मपृथग्भूतवस्तुसद्भावनिषेधपरत्वाभ्युपगमेन प्रतिपादिताः। - [ यदि ब्रह्म को सविशेष अर्थात् सगुण मानें तो 'निर्गुण' शब्द धारण करनेवाली श्रुतियों की क्या व्याख्या होगी ? ] 'निर्गुण' का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों की यह व्यवस्था होगी कि प्राकृत (प्रकृति सम्बन्धी Phenomenal ) त्याज्य गुणों (जैसे जरा, मरण आदि ) का निषेध करके ही परमात्मा का ज्ञान सम्भव है । [ परमात्मा निर्गुण है = उसमें जरा, मरण आदि त्याग करने योग्य गुण नहीं हैं। ]
[फिर भी, रामानुज परमेश्वर से जीवों और जड़-पदार्थों का भेद स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर श्रुतियां बहुत्व ( Pluralism ) का निषेध करती हैं-नेह नानास्ति किंचन ( बृ० ४।४।१९), एकमेवाद्वितीयम् ( छा० ६।२।१)। ऐसी दशा में इन श्रुतियों को क्या उत्तर देंगे ? ] एक ही ब्रह्म के शरीर के रूप में उसी ( ब्रह्म ) के प्रकार ( Type ) के रूप में सारी वस्तुएं चेतनात्मक ( Sentient ) और अचेतनात्मक ( Unsentient ) हैं, इसलिए सबों की आत्मा के रूप में, सब प्रकार से ब्रह्म ( एक मात्र ही ) अवस्थित है। अतः 'नानात्व' का निषेध करनेवाले श्रुतिवाक्यों का यही अर्थ दिया गया है कि सभी पदार्थों की आत्मा-ब्रह्म-से पृथक् किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। ऐसे ही अर्थ से उन वाक्यों की सिद्धि होती है।