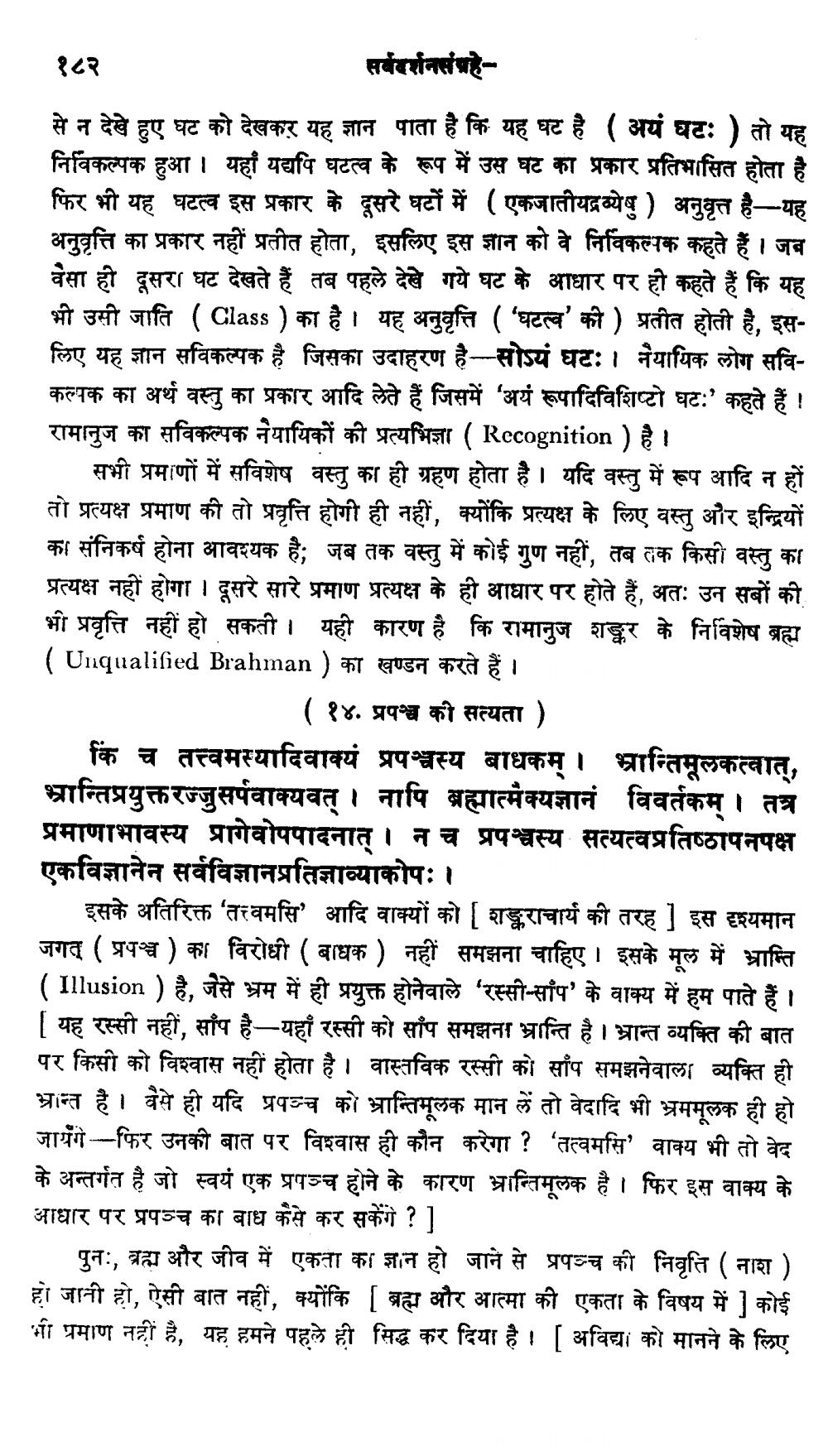________________
१८२
सर्वदर्शनसंग्रहे
से न देखे हुए घट को देखकर यह ज्ञान पाता है कि यह घट है ( अयं घटः ) तो यह निर्विकल्पक हुआ । यहाँ यद्यपि घटत्व के रूप में उस घट का प्रकार प्रतिभासित होता है फिर भी यह घटत्व इस प्रकार के दूसरे घटों में ( एकजातीयद्रव्येषु ) अनुवृत्त है - यह अनुवृत्ति का प्रकार नहीं प्रतीत होता, इसलिए इस ज्ञान को वे निर्विकल्पक कहते हैं । जब वैसा ही दूसरा घट देखते हैं तब पहले देखे गये घट के आधार पर ही कहते हैं कि यह भी उसी जाति ( Class ) का है । यह अनुवृत्ति ( 'घटत्व' की ) प्रतीत होती है, इसलिए यह ज्ञान सविकल्पक है जिसका उदाहरण है-सोऽयं घटः । नेयायिक लोग सविकल्पक का अर्थ वस्तु का प्रकार आदि लेते हैं जिसमें 'अयं रूपादिविशिष्टो घट : ' कहते हैं । रामानुज का सविकल्पक नेयायिकों की प्रत्यभिज्ञा ( Recognition ) है।
में
सभी प्रमाणों में सविशेष वस्तु का ही ग्रहण होता है । यदि वस्तु में रूप आदि न हों तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए वस्तु और इन्द्रियों का संनिकर्ष होना आवश्यक है; जब तक वस्तु कोई गुण नहीं, तब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा । दूसरे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के ही आधार पर होते हैं, अतः उन सबों की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यही कारण है कि रामानुज शङ्कर के निर्विशेष ब्रह्म ( Unqualified Brahman ) का खण्डन करते हैं ।
( १४. प्रपश्व की सत्यता )
किं च तत्त्वमस्यादिवाक्यं प्रपश्वस्य बाधकम् । भ्रान्तिमूलकत्वात्, भ्रान्तिप्रयुक्त रज्जुसर्पवाक्यवत् । नापि ब्रह्मात्मैक्यज्ञानं विवर्तकम् । तत्र प्रमाणाभावस्य प्रागेवोपपादनात् । न च प्रपश्वस्य सत्यत्वप्रतिष्ठापनपक्ष एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाव्याकोपः ।
इसके अतिरिक्त 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों को [ शङ्कराचार्य की तरह ] इस दृश्यमान जगत् ( प्रपञ्च ) का विरोधी ( बाधक ) नहीं समझना चाहिए। इसके मूल में भ्रान्ति ( Illusion ) है, जैसे भ्रम में ही प्रयुक्त होनेवाले 'रस्सी - साँप' के वाक्य में हम पाते हैं । [ यह रस्सी नहीं, साँप है—यहाँ रस्सी को साँप समझना भ्रान्ति है । भ्रान्त व्यक्ति की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता है । वास्तविक रस्सी को साँप समझनेवाला व्यक्ति ही भ्रान्त है | वैसे ही यदि प्रपञ्च को भ्रान्तिमूलक मान लें तो वेदादि भी भ्रममूलक ही हो जायेंगे - फिर उनकी बात पर विश्वास ही कौन करेगा ? 'तत्वमसि' वाक्य भी तो वेद के अन्तर्गत है जो स्वयं एक प्रपञ्च होने के कारण भ्रान्तिमूलक है । फिर इस वाक्य के आधार पर प्रपञ्च का बाध कैसे कर सकेंगे ? ]
पुनः, ब्रह्म और जीव में एकता का ज्ञान हो जाने से प्रपञ्च की निवृत्ति ( नाश ) हो जाती हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि [ ब्रह्म और आत्मा की एकता के विषय में ] कोई भी प्रमाण नहीं है, यह हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है । [ अविद्या को मानने के लिए