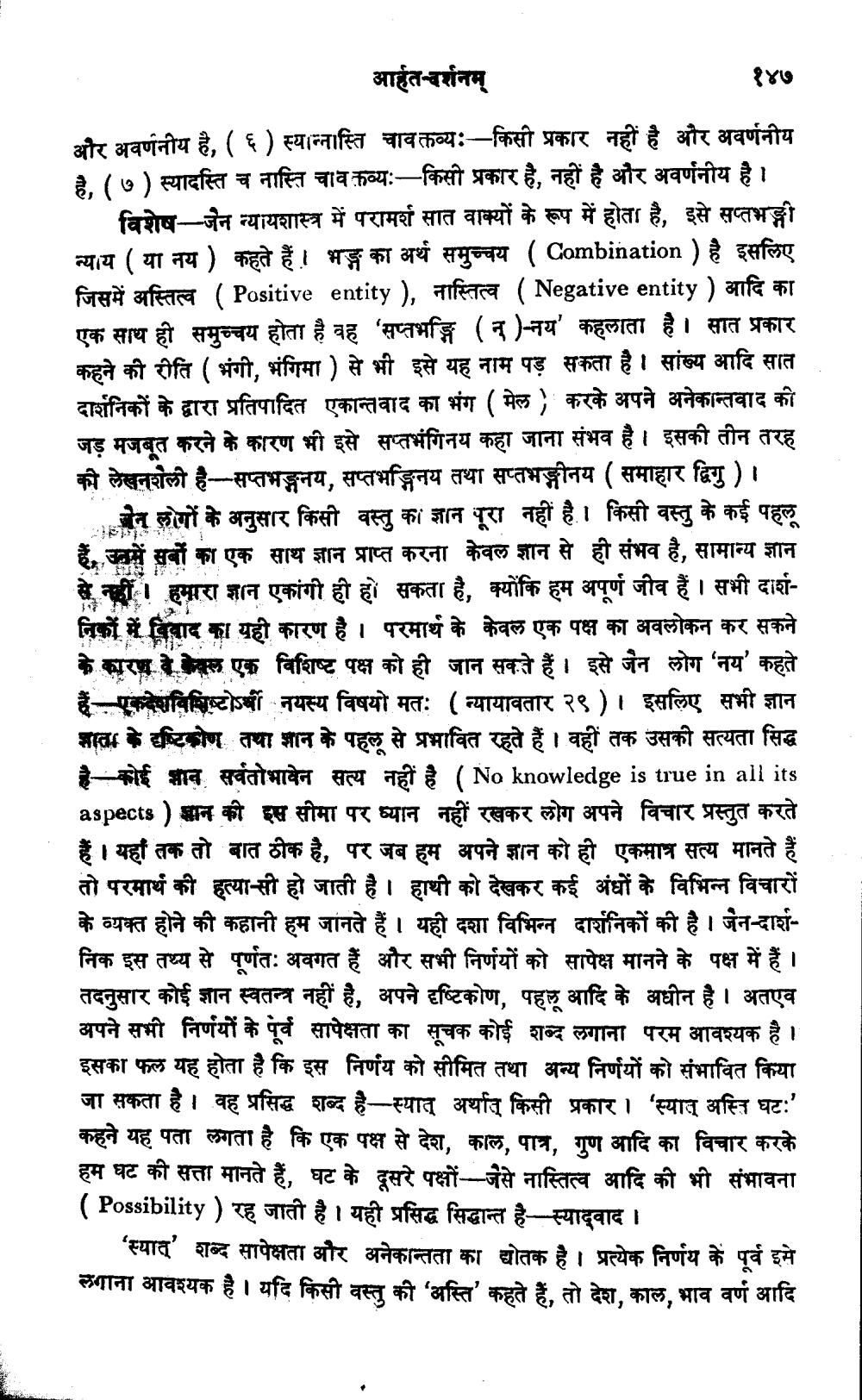________________
क
.
आहेत-चर्शनम्
१४७ और अवर्णनीय है, ( ६ ) स्यान्नास्ति चावक्तव्यः-किसी प्रकार नहीं है और अवर्णनीय है, (७) स्यादस्ति च नास्ति चावतव्यः—किसी प्रकार है, नहीं है और अवर्णनीय है।
विशेष-जैन न्यायशास्त्र में परामर्श सात वाक्यों के रूप में होता है, इसे सप्तभङ्गी न्याय ( या नय) कहते हैं। भङ्ग का अर्थ समुच्चय ( Combination ) है इसलिए जिसमें अस्तित्व ( Positive entity ), नास्तित्व ( Negative entity ) आदि का एक साथ ही समुच्चय होता है वह 'सप्तभङ्गि (न )-नय' कहलाता है। सात प्रकार कहने की रीति ( भंगी, भंगिमा ) से भी इसे यह नाम पड़ सकता है। सांख्य आदि सात दार्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित एकान्तवाद का भंग ( मेल ) करके अपने अनेकान्तवाद की जड़ मजबूत करने के कारण भी इसे सप्तभंगिनय कहा जाना संभव है। इसकी तीन तरह को लेखनशैली है-सप्तभङ्गनय, सप्तभङ्गिनय तथा सप्तभङ्गीनय ( समाहार द्विगु )।
जेन लोगों के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान पूरा नहीं है। किसी वस्तु के कई पहलू हैं, उनमें सबों का एक साथ ज्ञान प्राप्त करना केवल ज्ञान से ही संभव है, सामान्य ज्ञान से नहीं। हमारा ज्ञान एकांगी ही हो सकता है, क्योंकि हम अपूर्ण जीव हैं । सभी दार्शनिकों में विवाद का यही कारण है। परमार्थ के केवल एक पक्ष का अवलोकन कर सकने के कारण वे केवल एक विशिष्ट पक्ष को ही जान सकते हैं। इसे जैन लोग 'नय' कहते हैं- एकदेशविषिष्टोऽर्थी नयस्य विषयो मतः (न्यायावतार २९)। इसलिए सभी ज्ञान माता के दृष्टिकोण तथा शान के पहल से प्रभावित रहते हैं। वहीं तक उसकी सत्यता सिद्ध है-कोई शान सर्वतोभावेन सत्य नहीं है ( No knowledge is true in all its aspects ) शान की इस सीमा पर ध्यान नहीं रखकर लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, पर जब हम अपने ज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानते हैं तो परमार्थ की हत्या-सी हो जाती है। हाथी को देखकर कई अंधों के विभिन्न विचारों के व्यक्त होने की कहानी हम जानते हैं। यही दशा विभिन्न दार्शनिकों की है । जेन-दार्शनिक इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हैं और सभी निर्णयों को सापेक्ष मानने के पक्ष में हैं । तदनुसार कोई ज्ञान स्वतन्त्र नहीं है, अपने दृष्टिकोण, पहल आदि के अधीन है । अतएव अपने सभी निर्णयों के पूर्व सापेक्षता का सूचक कोई शब्द लगाना परम आवश्यक है। इसका फल यह होता है कि इस निर्णय को सीमित तथा अन्य निर्णयों को संभावित किया जा सकता है। वह प्रसिद्ध शब्द है-स्यात् अर्थात् किसी प्रकार । 'स्यात् अस्ति घटः' कहने यह पता लगता है कि एक पक्ष से देश, काल, पात्र, गुण आदि का विचार करके हम घट की सत्ता मानते हैं, घट के दूसरे पक्षों-जैसे नास्तित्व आदि की भी संभावना ( Possibility ) रह जाती है । यही प्रसिद्ध सिद्धान्त है-स्याद्वाद ।
'स्यात्' शब्द सापेक्षता और अनेकान्तता का द्योतक है। प्रत्येक निर्णय के पूर्व इमे लगाना आवश्यक है । यदि किसी वस्तु की 'अस्ति' कहते हैं, तो देश, काल, भाव वर्ण आदि