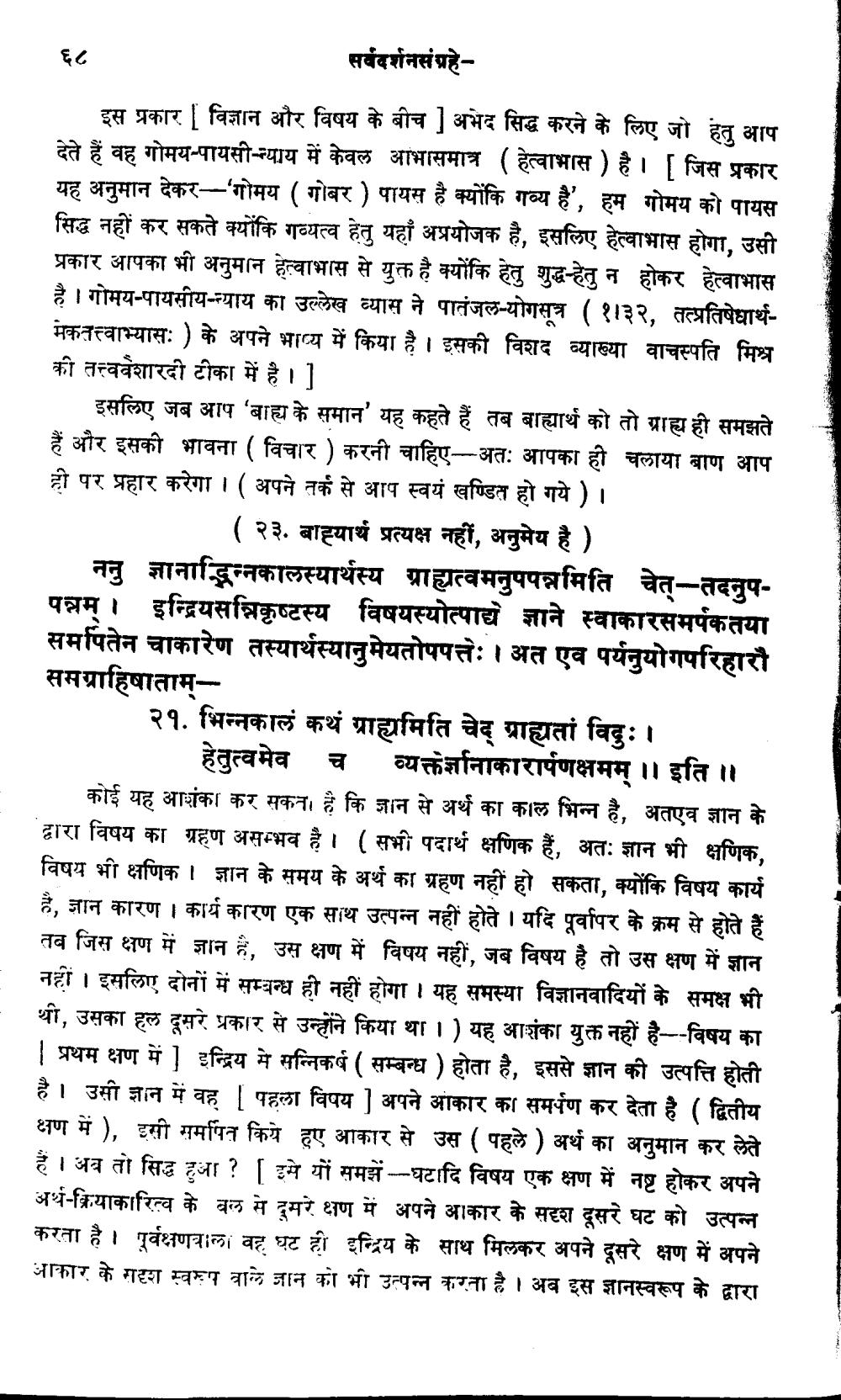________________
६
.
सर्वदर्शनसंग्रहे
इस प्रकार [ विज्ञान और विषय के बीच ] अभेद सिद्ध करने के लिए जो हंतु आप देते हैं वह गोमय-पायसी-न्याय में केवल आभासमात्र ( हेत्वाभास) है। जिस प्रकार यह अनुमान देकर-गोमय (गोबर) पायस है क्योंकि गव्य है', हम गोमय को पायस सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि गव्यत्व हेतु यहाँ अप्रयोजक है, इसलिए हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार आपका भी अनुमान हेत्वाभास से युक्त है क्योंकि हेतु शुद्ध हेतु न होकर हेत्वाभास है । गोमय-पायसीय-न्याय का उल्लेख व्यास ने पातंजल-योगसूत्र ( ११३२, तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ) के अपने भाष्य में किया है । इसकी विशद व्याख्या वाचस्पति मिश्र की तत्त्ववैशारदी टीका में है। ___इसलिए जब आप 'बाह्य के समान' यह कहते हैं तब बाह्यार्थ को तो ग्राह्य ही समझते हैं और इसकी भावना ( विचार ) करनी चाहिए-अतः आपका ही चलाया बाण आप ही पर प्रहार करेगा । ( अपने तर्क से आप स्वयं खण्डित हो गये )।
( २३. बाह्यार्थ प्रत्यक्ष नहीं, अनुमेय है ) ननु ज्ञानाद्भिन्नकालस्यार्थस्य ग्राह्यत्वमनुपपन्नमिति चेत्-तदनुपपन्नम्। इन्द्रियसन्निकृष्टस्य विषयस्योत्पाद्ये ज्ञाने स्वाकारसमर्पकतया समपितेन चाकारेण तस्यार्थस्यानुमेयतोपपत्तेः । अत एव पर्यनुयोगपरिहारौ समग्राहिषाताम्__२१. भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद् ग्राह्यतां विदुः।
हेतुत्वमेव च व्यक्तआनाकारार्पणक्षमम् ॥ इति ॥ कोई यह आशंका कर सकता है कि ज्ञान से अर्थ का काल भिन्न है, अतएव ज्ञान के द्वारा विषय का ग्रहण असम्भव है। ( सभी पदार्थ क्षणिक हैं, अतः ज्ञान भी क्षणिक, विषय भी क्षणिक । ज्ञान के समय के अर्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि विषय कार्य है, ज्ञान कारण । कार्य कारण एक साथ उत्पन्न नहीं होते । यदि पूर्वापर के क्रम से होते हैं तव जिस क्षण में ज्ञान है, उस क्षण में विषय नहीं, जब विषय है तो उस क्षण में ज्ञान नहीं । इसलिए दोनों में सम्बन्ध ही नहीं होगा। यह समस्या विज्ञानवादियों के समक्ष भी थी, उसका हल दूसरे प्रकार से उन्होंने किया था। ) यह आशंका युक्त नहीं है--विषय का | प्रथम क्षण में ] इन्द्रिय मे सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) होता है, इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसी ज्ञान में वह [ पहला विषय ] अपने आकार का समर्पण कर देता है (द्वितीय क्षण में ), इसी मर्पित किये हए आकार से उस ( पहले ) अर्थ का अनुमान कर लेते हैं । अब तो सिद्ध हुआ ? [ इसे यों समझें-घटादि विषय एक क्षण में नष्ट होकर अपने अर्थ-क्रियाकारित्व के बल से दुमरे क्षण में अपने आकार के सदृश दूसरे घट को उत्पन्न करता है। पूर्वक्षणवाला वह घट ही इन्द्रिय के साथ मिलकर अपने दूसरे क्षण में अपने आकार के सदृश स्वरूप वाले ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। अब इस ज्ञानस्वरूप के द्वारा