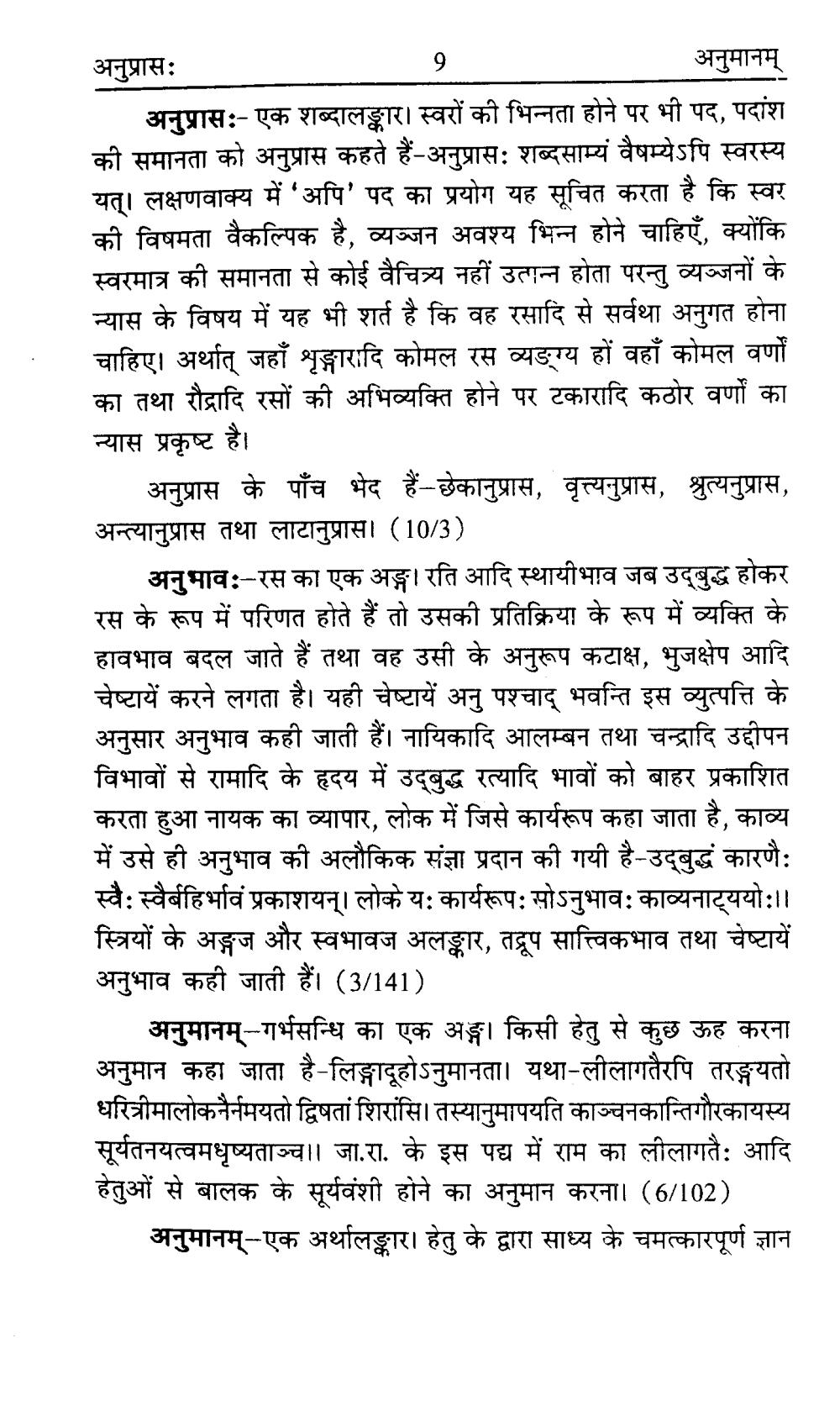________________
अनुप्रासः
अनुमानम् अनुप्रासः- एक शब्दालङ्कार। स्वरों की भिन्नता होने पर भी पद, पदांश की समानता को अनुप्रास कहते हैं-अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। लक्षणवाक्य में 'अपि' पद का प्रयोग यह सूचित करता है कि स्वर की विषमता वैकल्पिक है, व्यञ्जन अवश्य भिन्न होने चाहिए, क्योंकि स्वरमात्र की समानता से कोई वैचित्र्य नहीं उतान्न होता परन्तु व्यञ्जनों के न्यास के विषय में यह भी शर्त है कि वह रसादि से सर्वथा अनुगत होना चाहिए। अर्थात् जहाँ शृङ्गारादि कोमल रस व्यङ्ग्य हों वहाँ कोमल वर्णों का तथा रौद्रादि रसों की अभिव्यक्ति होने पर टकारादि कठोर वर्गों का न्यास प्रकृष्ट है।
अनुप्रास के पाँच भेद हैं-छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास तथा लाटानुप्रास। (10/3)
अनुभावः-रस का एक अङ्ग। रति आदि स्थायीभाव जब उबुद्ध होकर रस के रूप में परिणत होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्ति के हावभाव बदल जाते हैं तथा वह उसी के अनुरूप कटाक्ष, भुजक्षेप आदि चेष्टायें करने लगता है। यही चेष्टायें अनु पश्चाद् भवन्ति इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुभाव कही जाती हैं। नायिकादि आलम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन विभावों से रामादि के हृदय में उबुद्ध रत्यादि भावों को बाहर प्रकाशित करता हुआ नायक का व्यापार, लोक में जिसे कार्यरूप कहा जाता है, काव्य में उसे ही अनुभाव की अलौकिक संज्ञा प्रदान की गयी है-उबुद्ध कारणैः स्वैः स्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन्। लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः।। स्त्रियों के अङ्गज और स्वभावज अलङ्कार, तद्रूप सात्त्विकभाव तथा चेष्टायें अनुभाव कही जाती हैं। (3/141) ___ अनुमानम्-गर्भसन्धि का एक अङ्ग। किसी हेतु से कुछ ऊह करना अनुमान कहा जाता है-लिङ्गादूहोऽनुमानता। यथा-लीलागतैरपि तरङ्गयतो धरित्रीमालोकनैर्नमयतो द्विषतां शिरांसि। तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौरकायस्य सूर्यतनयत्वमधृष्यताञ्च।। जा.रा. के इस पद्य में राम का लीलागतैः आदि हेतुओं से बालक के सूर्यवंशी होने का अनुमान करना। (6/102)
अनुमानम्-एक अर्थालङ्कार। हेतु के द्वारा साध्य के चमत्कारपूर्ण ज्ञान