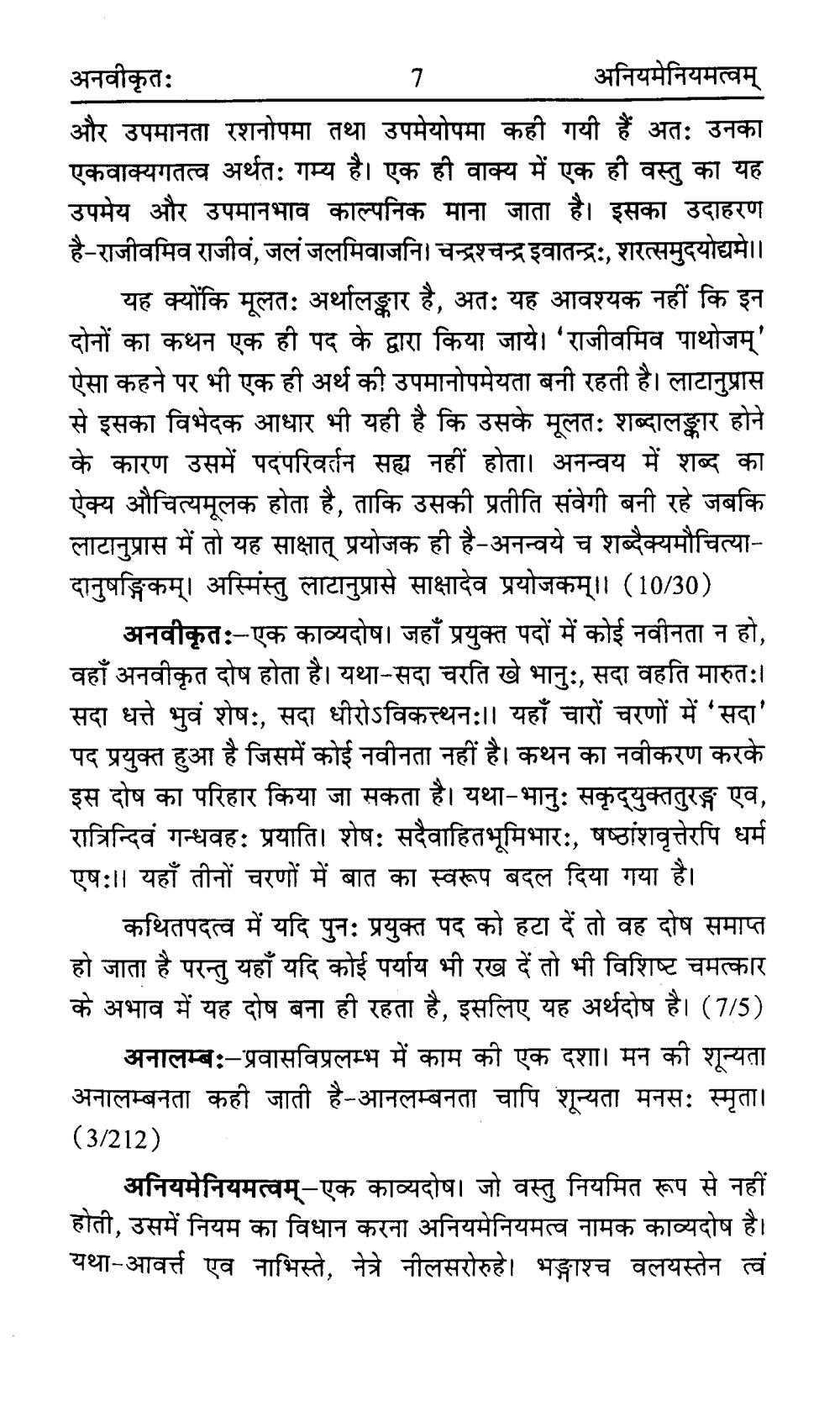________________
अनवीकृत:
7
अनियमेनियमत्वम्
और उपमानता रशनोपमा तथा उपमेयोपमा कही गयी हैं अतः उनका एकवाक्यगतत्व अर्थतः गम्य है। एक ही वाक्य में एक ही वस्तु का यह उपमेय और उपमानभाव काल्पनिक माना जाता है। इसका उदाहरण है-राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि । चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्रः, शरत्समुदयोद्यमे ।।
यह क्योंकि मूलतः अर्थालङ्कार है, अत: यह आवश्यक नहीं कि इन दोनों का कथन एक ही पद के द्वारा किया जाये । 'राजीवमिव पाथोजम्' ऐसा कहने पर भी एक ही अर्थ की उपमानोपमेयता बनी रहती है। लाटानुप्रास से इसका विभेदक आधार भी यही है कि उसके मूलतः शब्दालङ्कार होने के कारण उसमें पदपरिवर्तन सह्य नहीं होता। अनन्वय में शब्द का ऐक्य औचित्यमूलक होता है, ताकि उसकी प्रतीति संवेगी बनी रहे जबकि लाटानुप्रास में तो यह साक्षात् प्रयोजक ही है- अनन्वये च शब्दैक्यमौचित्यादानुषङ्गिकम् । अस्मिंस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम् || ( 10/30 )
अनवीकृत :- एक काव्यदोष । जहाँ प्रयुक्त पदों में कोई नवीनता न हो, वहाँ अनवीकृत दोष होता है । यथा - सदा चरति खे भानुः, सदा वहति मारुतः । सदा धत्ते भुवं शेषः, सदा धीरोऽविकत्थनः । । यहाँ चारों चरणों में 'सदा' पद प्रयुक्त हुआ है जिसमें कोई नवीनता नहीं है । कथन का नवीकरण करके इस दोष का परिहार किया जा सकता है। यथा - भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव, रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । शेषः सदैवाहितभूमिभारः, षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः।। यहाँ तीनों चरणों में बात का स्वरूप बदल दिया गया है।
कथितपदत्व में यदि पुनः प्रयुक्त पद को हटा दें तो वह दोष समाप्त हो जाता है परन्तु यहाँ यदि कोई पर्याय भी रख दें तो भी विशिष्ट चमत्कार के अभाव में यह दोष बना ही रहता है, इसलिए यह अर्थदोष है। (7/5)
अनालम्ब:-प्रवासविप्रलम्भ में काम की एक दशा । मन की शून्यता अनालम्बनता कही जाती है- आनलम्बनता चापि शून्यता मनसः स्मृता । (3/212)
अनियमेनियमत्वम् - एक काव्यदोष। जो वस्तु नियमित रूप से नहीं होती, उसमें नियम का विधान करना अनियमेनियमत्व नामक काव्यदोष है। यथा - आवर्त्त एव नाभिस्ते, नेत्रे नीलसरोरुहे । भङ्गाश्च वलयस्तेन त्वं