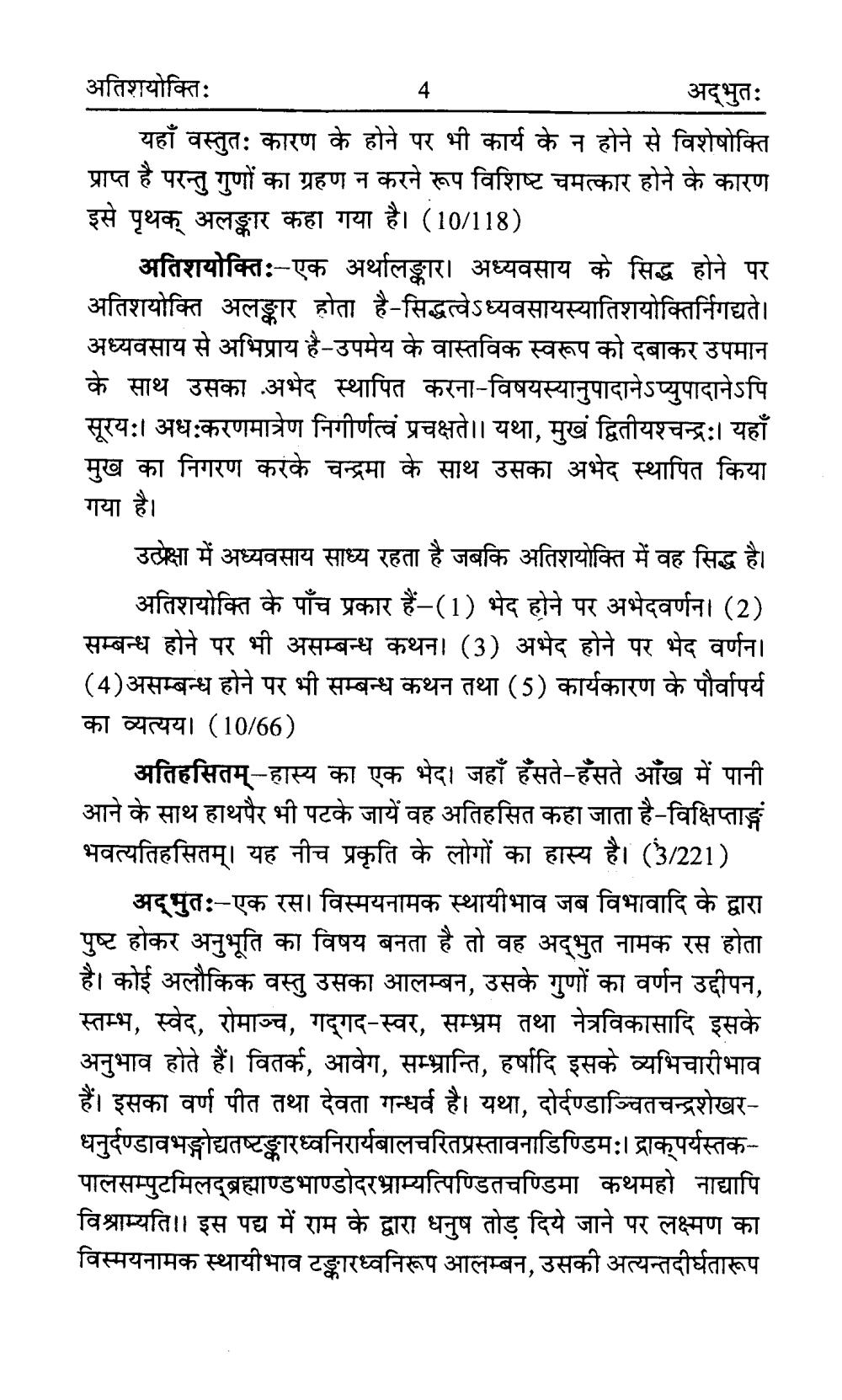________________
अतिशयोक्तिः
4
अद्भुतः
यहाँ वस्तुत: कारण के होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति प्राप्त है परन्तु गुणों का ग्रहण न करने रूप विशिष्ट चमत्कार होने के कारण इसे पृथक् अलङ्कार कहा गया है। ( 10 / 118)
अतिशयोक्तिः - एक अर्थालङ्कार । अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है- सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते। अध्यवसाय से अभिप्राय है-उपमेय के वास्तविक स्वरूप को दबाकर उपमान के साथ उसका अभेद स्थापित करना - विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूरयः । अध:करणमात्रेण निगीर्णत्वं प्रचक्षते । यथा, मुखं द्वितीयश्चन्द्रः । यहाँ मुख का निगरण करके चन्द्रमा के साथ उसका अभेद स्थापित किया गया है।
उत्प्रेक्षा में अध्यवसाय साध्य रहता है जबकि अतिशयोक्ति में वह सिद्ध है। अतिशयोक्ति के पाँच प्रकार हैं- (1) भेद होने पर अभेदवर्णन। (2) सम्बन्ध होने पर भी असम्बन्ध कथन । (3) अभेद होने पर भेद वर्णन । (4) असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध कथन तथा (5) कार्यकारण के पौर्वापर्य का व्यत्यय। (10/66)
अतिहसितम् - हास्य का एक भेद । जहाँ हँसते-हँसते आँख में पानी आने के साथ हाथपैर भी पटके जायें वह अतिहसित कहा जाता है-विक्षिप्ताङ्गं भवत्यतिहसितम् | यह नीच प्रकृति के लोगों का हास्य है। (3/221)
अद्भुत :- एक रस । विस्मयनामक स्थायीभाव जब विभावादि के द्वारा पुष्ट होकर अनुभूति का विषय बनता है तो वह अद्भुत नामक रस होता है। कोई अलौकिक वस्तु उसका आलम्बन, उसके गुणों का वर्णन उद्दीपन, स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गद - स्वर, सम्भ्रम तथा नेत्रविकासादि इसके अनुभाव होते हैं। वितर्क, आवेग, सम्भ्रान्ति, हर्षादि इसके व्यभिचारीभाव हैं। इसका वर्ण पीत तथा देवता गन्धर्व है। यथा, दोर्दण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोद्यतष्टङ्कारध्वनिरार्यबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः। द्राक्पर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्ब्रह्माण्डभाण्डोदरभ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ।। इस पद्य में राम के द्वारा धनुष तोड़ दिये जाने पर लक्ष्मण का विस्मयनामक स्थायीभाव टङ्कारध्वनिरूप आलम्बन, , उसकी अत्यन्तदीर्घतारूप