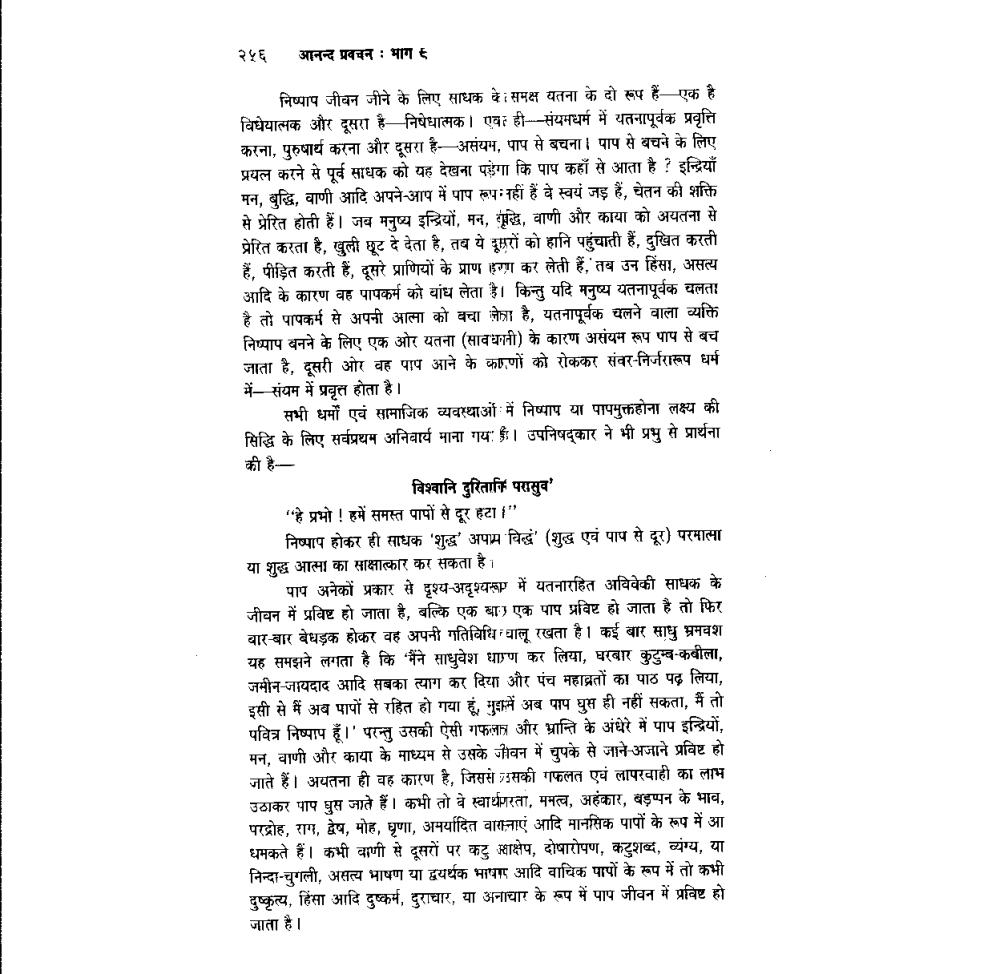________________
२५६
आनन्द प्रवचन : भाग ६
निष्पाप जीवन जीने के लिए साधक के समक्ष यतना के दो रूप हैं— एक है विधेयात्मक और दूसरा है निषेधात्मक। एक ही--संयमधर्म में यतनापूर्वक प्रवृत्ति करना, पुरुषार्थ करना और दूसरा है—असंयम, पाप से बचना । पाप से बचने के लिए प्रयल करने से पूर्व साधक को यह देखना पड़ेगा कि पाप कहाँ से आता है ? इन्द्रियाँ मन, बुद्धि, वाणी आदि अपने-आप में पाप रूप नहीं हैं वे स्वयं जड़ हैं, चेतन की शक्ति से प्रेरित होती हैं। जब मनुष्य इन्द्रियों, मन, शुद्ध, वाणी और काया को अयतना से प्रेरित करता है, खुली छूट दे देता है, तब ये दूसरों को हानि पहुंचाती हैं, दुखित करती हैं, पीड़ित करती हैं, दूसरे प्राणियों के प्राण हरण कर लेती हैं, तब उन हिंसा, असत्य आदि के कारण वह पापकर्म को बांध लेता है। किन्तु यदि मनुष्य यतनापूर्वक चलता है तो पापकर्म से अपनी आत्मा को बचा लेता है, यतनापूर्वक चलने वाला व्यक्ति निष्पाप बनने के लिए एक ओर यतना (सावधानी) के कारण असंयन रूप पाप से बच जाता है, दूसरी ओर वह पाप आने के कारणों को रोककर संवर-निर्जरारूप धर्म में-संयम में प्रवृत्त होता है।
सभी धर्मों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में निष्पाप या पापमुक्तहोना लक्ष्य की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य माना गया। उपनिषद्कार ने भी प्रभु से प्रार्थना
की है
विश्वानि दुरिताकि परासुव' "हे प्रभो ! हमें समस्त पापों से दूर हटा।"
निष्पाप होकर ही साधक 'शुद्ध' अपम विद्धं' (शुद्ध एवं पाप से दूर) परमात्मा या शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है।
पाप अनेकों प्रकार से दृश्य-अदृश्यरूप में यतनारहित अविवेकी साधक के जीवन में प्रविष्ट हो जाता है, बल्कि एक बा) एक पाप प्रविष्ट हो जाता है तो फिर बार बार बेधड़क होकर वह अपनी गतिविधि घालू रखता है। कई बार साधु भ्रमवश यह समझने लगता है कि 'मैंने साधुवेश धारण कर लिया, घरबार कुटुम्ब-कबीला, जमीन जायदाद आदि सबका त्याग कर दिया और पंच महाव्रतों का पाठ पढ़ लिया, इसी से मैं अब पापों से रहित हो गया हूं, मुझमें अब पाप घुस ही नहीं सकता, मैं तो पवित्र निष्पाप हूँ।' परन्तु उसकी ऐसी गफलान और भ्रान्ति के अंधेरे में पाप इन्द्रियों, मन, वाणी और काया के माध्यम से उसके जीवन में चुपके से जाने अजाने प्रविष्ट हो जाते हैं। अयतना ही वह कारण है, जिससे उसकी गफलत एवं लापरवाही का लाभ उठाकर पाप घुस जाते हैं। कभी तो वे स्वार्थपरता, ममत्व, अहंकार, बड़प्पन के भाव, परद्रोह, राग, द्वेष, मोह, घृणा, अमर्यादित वासनाएं आदि मानसिक पापों के रूप में आ धमकते हैं। कभी वाणी से दूसरों पर कटु स्वाक्षेप, दोषारोपण, कटुशब्द, व्यंग्य, या निन्दा-चुगली, असत्य भाषण या द्वयर्थक भाषा आदि वाचिक पापों के रूप में तो कभी दुष्कृत्य, हिंसा आदि दुष्कर्म, दुराचार, या अनाचार के रूप में पाप जीवन में प्रविष्ट हो जाता है।