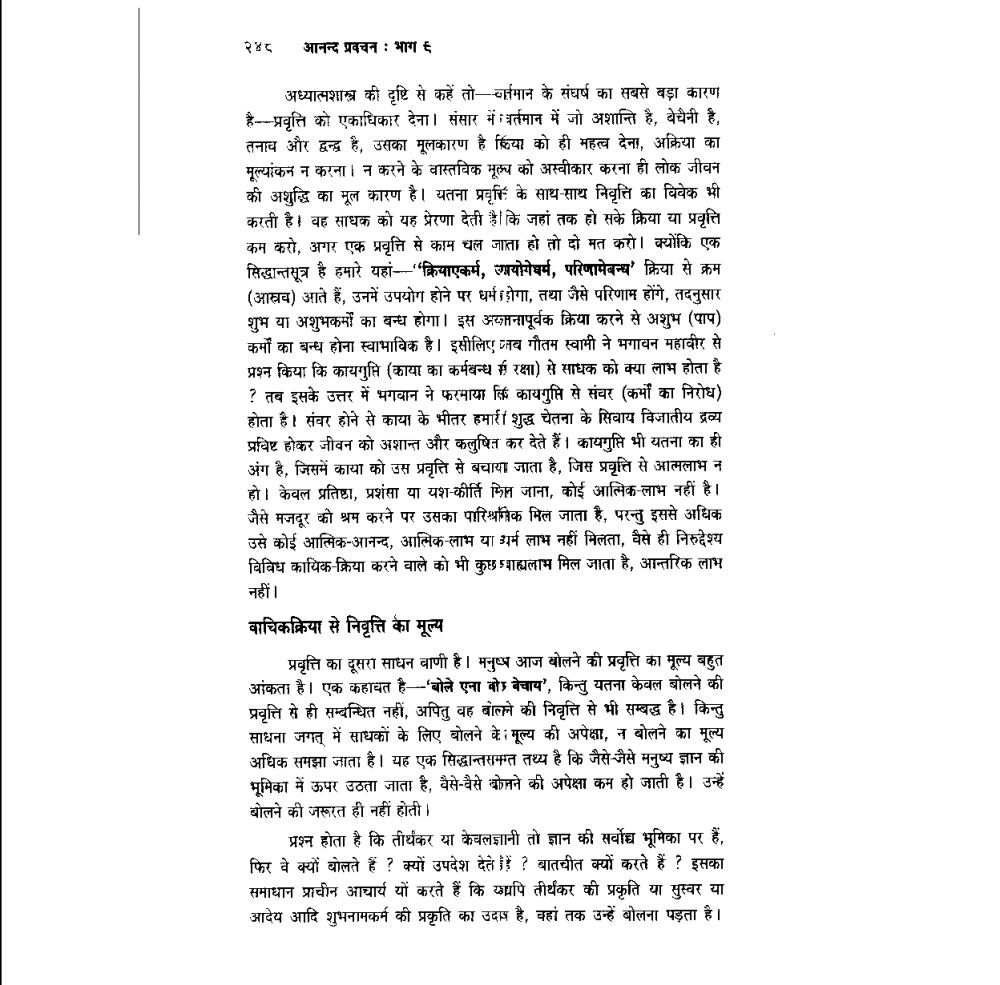________________
२४८
आनन्द प्रवचन: भाग ६
अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से कहें तो वर्तमान के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है--प्रवृत्ति को एकाधिकार देना। संसार में वर्तमान में जो अशान्ति है, बेचैनी है, तनाव और द्वन्द्व है, उसका मूलकारण है किया को ही महत्त्व देना, अक्रिया का मूल्यांकन न करना। न करने के वास्तविक मूल्य को अस्वीकार करना ही लोक जीवन की अशुद्धि का मूल कारण है। यतना प्रवृति के साथ-साथ निवृत्ति का विवेक भी करती है। वह साधक को यह प्रेरणा देती है। कि जहां तक हो सके क्रिया या प्रवृत्ति कम करो, अगर एक प्रवृत्ति से काम चल जाता हो तो दो मत करो। क्योंकि एक सिद्धान्तसूत्र है हमारे यहां-क्रियाएकर्म, उपयोगेधर्म, परिणामेबन्ध' क्रिया से क्रम (आस्रव) आते हैं, उनमें उपयोग होने पर धर्मडोगा, तथा जैसे परिणाम होंगे, तदनुसार शुभ या अशुभकर्मों का बन्ध होगा। इस अयातनापूर्वक क्रिया करने से अशुभ (पाप) कर्मों का बन्ध होना स्वाभाविक है। इसीलिए जब गौतम स्वामी ने भगावन महावीर से प्रश्न किया कि कायगुप्ति (काया का कर्मबन्ध में रक्षा) से साधक को क्या लाभ होता है ? तब इसके उत्तर में भगवान ने फरमाया किं कायगुप्ति से संवर (कर्मों का निरोध) होता है। संबर होने से काया के भीतर हमारी शुद्ध चेतना के सिवाय विजातीय द्रव्य प्रविष्ट होकर जीवन को अशान्त और कलुषित कर देते हैं। कायगुप्ति भी यतना का ही अंग है, जिसमें काया को उस प्रवृत्ति से बचाया जाता है, जिस प्रवृत्ति से आत्मलाभ न हो। केवल प्रतिष्ठा, प्रशंसा या यश-कीर्ति मिल जाना, कोई आत्मिक-लाभ नहीं है। जैसे मजदूर को श्रम करने पर उसका पारिश्रमिक मिल जाता है, परन्तु इससे अधिक उसे कोई आत्मिक-आनन्द, आत्मिक लाभ या धर्म लाभ नहीं मिलता, वैसे ही निरुद्देश्य विविध कायिक क्रिया करने वाले को भी कुछ वाह्यलाभ मिल जाता है, आन्तरिक लाभ नहीं। वाचिकक्रिया से निवृत्ति का मूल्य
प्रवृत्ति का दूसरा साधन वाणी है। मनुष्ष आज बोलने की प्रवृत्ति का मूल्य बहुत आंकता है। एक कहावत है-'बोले एना बो बेचाय', किन्तु यतना केवल बोलने की प्रवृत्ति से ही सम्बन्धित नहीं, अपितु वह बोलने की निवृत्ति से भी सम्बद्ध है। किन्तु साधना जगत् में साधकों के लिए बोलने के मूल्य की अपेक्षा, न बोलने का मूल्य अधिक समझा जाता है। यह एक सिद्धान्तसमत तथ्य है कि जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान की भूमिका में ऊपर उठता जाता है, वैसे-वैसे बनने की अपेक्षा कम हो जाती है। उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं होती।
प्रश्न होता है कि तीर्थकर या केवलज्ञानी तो ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका पर हैं, फिर वे क्यों बोलते हैं ? क्यों उपदेश देते हैं ? बातचीत क्यों करते हैं ? इसका समाधान प्राचीन आचार्य यों करते हैं कि उनपि तीर्थकर की प्रकृति या सुस्वर या आदेय आदि शुभनामकर्म की प्रकृति का उदाप है, वहां तक उन्हें बोलना पड़ता है।