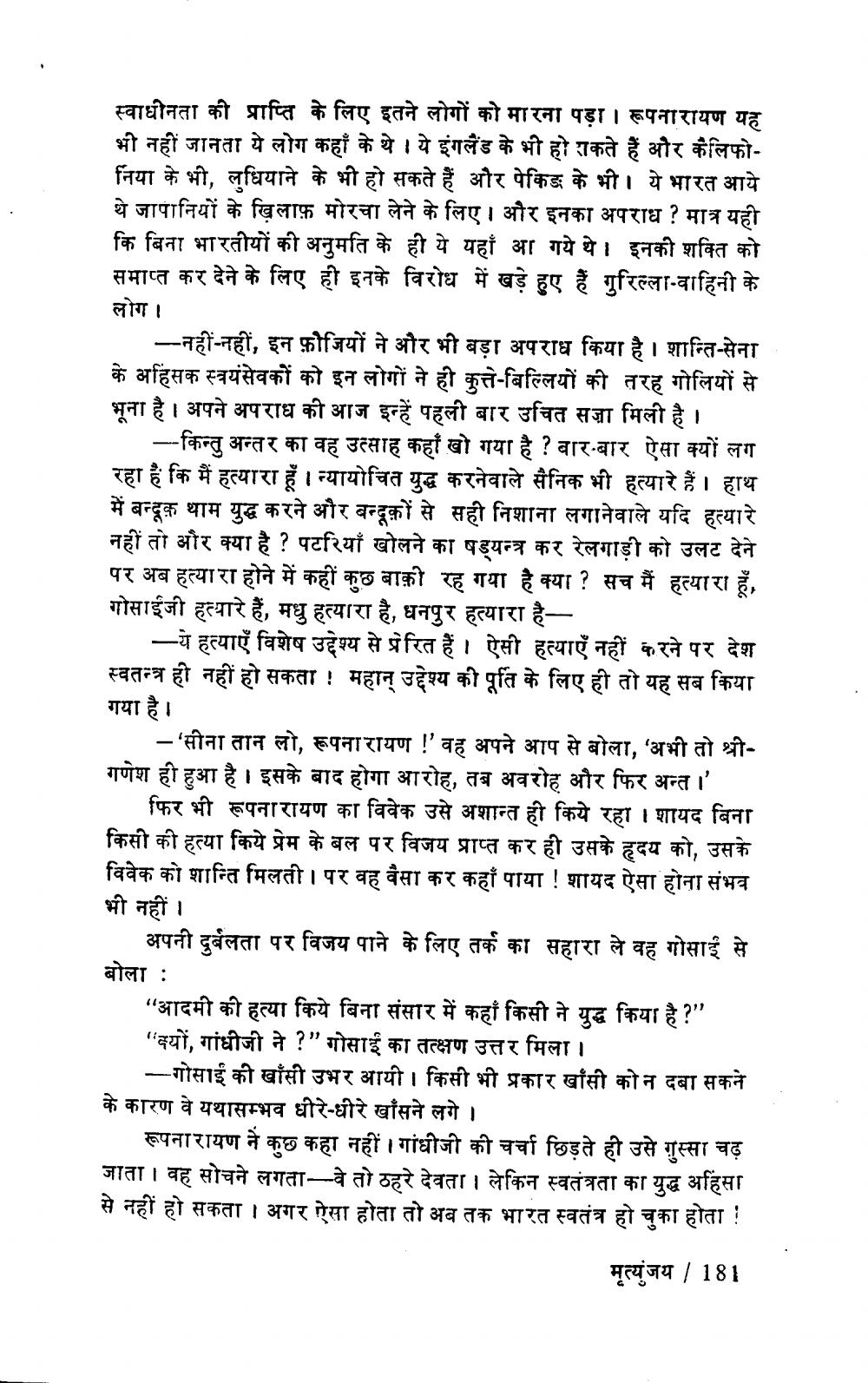________________
स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए इतने लोगों को मारना पड़ा। रूपनारायण यह भी नहीं जानता ये लोग कहाँ के थे । ये इंगलैंड के भी हो सकते हैं और कैलिफोनिया के भी, लुधियाने के भी हो सकते हैं और पेकिङ के भी। ये भारत आये थे जापानियों के ख़िलाफ़ मोरचा लेने के लिए। और इनका अपराध ? मात्र यही कि बिना भारतीयों की अनुमति के ही ये यहाँ आ गये थे। इनकी शक्ति को समाप्त कर देने के लिए ही इनके विरोध में खड़े हुए हैं गुरिल्ला-वाहिनी के लोग।
-नहीं-नहीं, इन फ़ोजियों ने और भी बड़ा अपराध किया है । शान्ति-सेना के अहिंसक स्वयंसेवकों को इन लोगों ने ही कुत्ते-बिल्लियों की तरह गोलियों से भूना है। अपने अपराध की आज इन्हें पहली बार उचित सजा मिली है। ___ --किन्तु अन्तर का वह उत्साह कहाँ खो गया है ? बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हत्यारा हूँ। न्यायोचित युद्ध करनेवाले सैनिक भी हत्यारे हैं। हाथ में बन्दूक थाम युद्ध करने और बन्दूकों से सही निशाना लगानेवाले यदि हत्यारे नहीं तो और क्या है ? पटरियाँ खोलने का षड्यन्त्र कर रेलगाड़ी को उलट देने पर अब हत्यारा होने में कहीं कुछ बाक़ी रह गया है क्या ? सच मैं हत्यारा हूँ, गोसाईंजी हत्यारे हैं, मधु हत्यारा है, धनपुर हत्यारा है
-ये हत्याएँ विशेष उद्देश्य से प्रेरित हैं। ऐसी हत्याएँ नहीं करने पर देश स्वतन्त्र ही नहीं हो सकता ! महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तो यह सब किया गया है।
– 'सीना तान लो, रूपनारायण !' वह अपने आप से बोला, 'अभी तो श्रीगणेश ही हुआ है । इसके बाद होगा आरोह, तब अवरोह और फिर अन्त ।'
फिर भी रूपनारायण का विवेक उसे अशान्त ही किये रहा । शायद बिना किसी की हत्या किये प्रेम के बल पर विजय प्राप्त कर ही उसके हृदय को, उसके विवेक को शान्ति मिलती। पर वह वैसा कर कहाँ पाया ! शायद ऐसा होना संभव भी नहीं। ___अपनी दुर्बलता पर विजय पाने के लिए तर्क का सहारा ले वह गोसाईं से बोला :
"आदमी की हत्या किये बिना संसार में कहाँ किसी ने युद्ध किया है ?" "क्यों, गांधीजी ने ?" गोसाई का तत्क्षण उत्तर मिला।
-गोसाईं की खाँसी उभर आयी। किसी भी प्रकार खाँसी को न दबा सकने के कारण वे यथासम्भव धीरे-धीरे खाँसने लगे।
रूपनारायण ने कुछ कहा नहीं । गांधीजी की चर्चा छिड़ते ही उसे गुस्सा चढ़ जाता। वह सोचने लगता-वे तो ठहरे देवता। लेकिन स्वतंत्रता का युद्ध अहिंसा से नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अब तक भारत स्वतंत्र हो चुका होता !
मृत्युंजय | 181