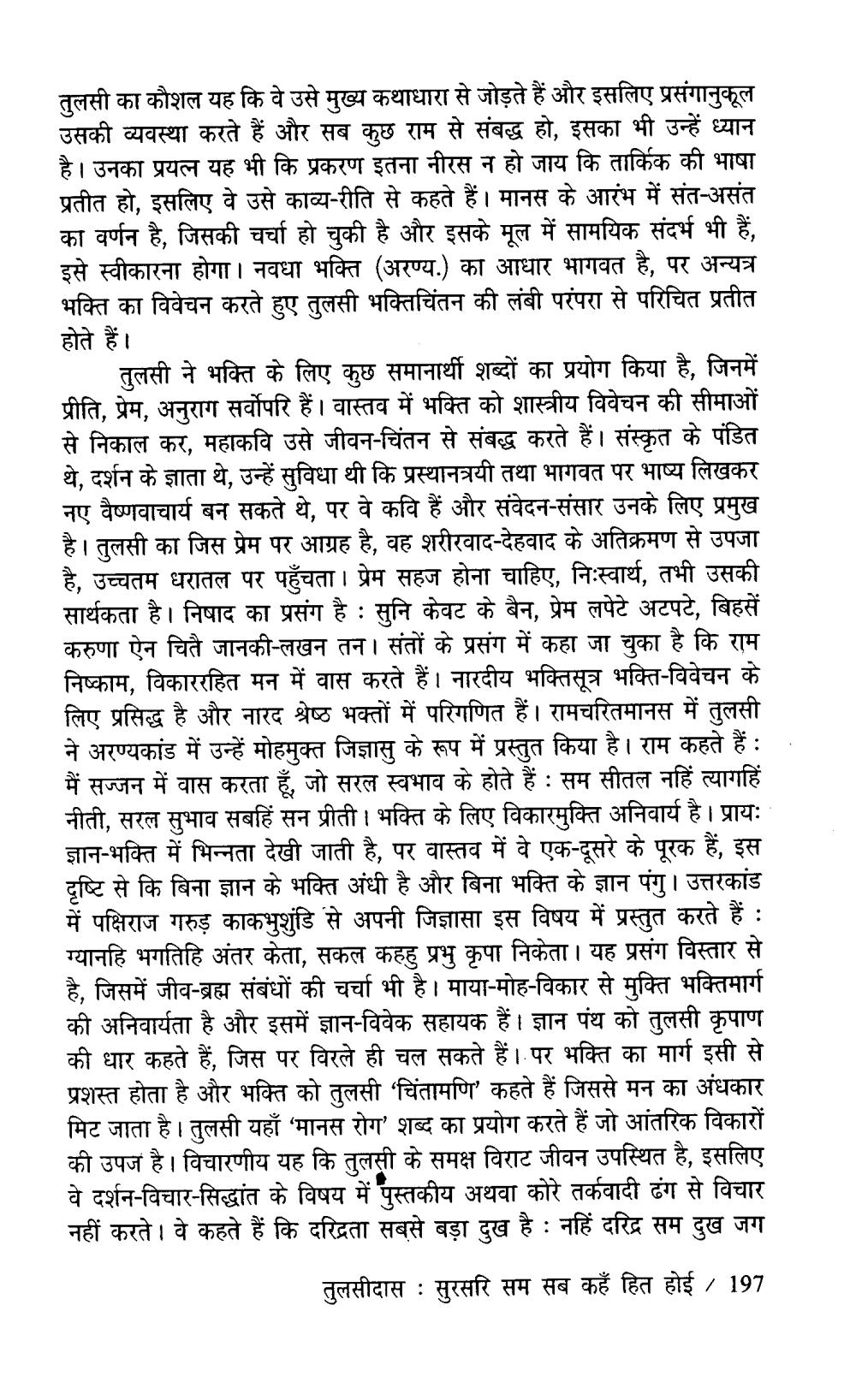________________
तुलसी का कौशल यह कि वे उसे मुख्य कथाधारा से जोड़ते हैं और इसलिए प्रसंगानुकूल उसकी व्यवस्था करते हैं और सब कुछ राम से संबद्ध हो, इसका भी उन्हें ध्यान है। उनका प्रयत्न यह भी कि प्रकरण इतना नीरस न हो जाय कि तार्किक की भाषा प्रतीत हो, इसलिए वे उसे काव्य-रीति से कहते हैं। मानस के आरंभ में संत-असंत का वर्णन है, जिसकी चर्चा हो चुकी है और इसके मूल में सामयिक संदर्भ भी हैं, इसे स्वीकारना होगा। नवधा भक्ति (अरण्य.) का आधार भागवत है, पर अन्यत्र भक्ति का विवेचन करते हुए तुलसी भक्तिचिंतन की लंबी परंपरा से परिचित प्रतीत होते हैं।
तुलसी ने भक्ति के लिए कुछ समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें प्रीति, प्रेम, अनुराग सर्वोपरि हैं। वास्तव में भक्ति को शास्त्रीय विवेचन की सीमाओं से निकाल कर, महाकवि उसे जीवन-चिंतन से संबद्ध करते हैं। संस्कृत के पंडित थे, दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें सुविधा थी कि प्रस्थानत्रयी तथा भागवत पर भाष्य लिखकर नए वैष्णवाचार्य बन सकते थे, पर वे कवि हैं और संवेदन-संसार उनके लिए प्रमुख है। तुलसी का जिस प्रेम पर आग्रह है, वह शरीरवाद-देहवाद के अतिक्रमण से उपजा है, उच्चतम धरातल पर पहुँचता। प्रेम सहज होना चाहिए, निःस्वार्थ, तभी उसकी सार्थकता है। निषाद का प्रसंग है : सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहमें करुणा ऐन चितै जानकी-लखन तन। संतों के प्रसंग में कहा जा चुका है कि राम निष्काम, विकाररहित मन में वास करते हैं। नारदीय भक्तिसूत्र भक्ति-विवेचन के लिए प्रसिद्ध है और नारद श्रेष्ठ भक्तों में परिगणित हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने अरण्यकांड में उन्हें मोहमुक्त जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत किया है। राम कहते हैं : मैं सज्जन में वास करता हूँ, जो सरल स्वभाव के होते हैं : सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती, सरल सुभाव सबहिं सन प्रीती। भक्ति के लिए विकारमुक्ति अनिवार्य है। प्रायः ज्ञान-भक्ति में भिन्नता देखी जाती है, पर वास्तव में वे एक-दूसरे के पूरक हैं, इस दृष्टि से कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु। उत्तरकांड में पक्षिराज गरुड़ काकभुशुंडि से अपनी जिज्ञासा इस विषय में प्रस्तुत करते हैं : ग्यानहि भगतिहि अंतर केता, सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता। यह प्रसंग विस्तार से है, जिसमें जीव-ब्रह्म संबंधों की चर्चा भी है। माया-मोह-विकार से मुक्ति भक्तिमार्ग की अनिवार्यता है और इसमें ज्ञान-विवेक सहायक हैं। ज्ञान पंथ को तुलसी कृपाण की धार कहते हैं, जिस पर विरले ही चल सकते हैं। पर भक्ति का मार्ग इसी से प्रशस्त होता है और भक्ति को तुलसी 'चिंतामणि' कहते हैं जिससे मन का अंधकार मिट जाता है। तुलसी यहाँ 'मानस रोग' शब्द का प्रयोग करते हैं जो आंतरिक विकारों की उपज है। विचारणीय यह कि तुलसी के समक्ष विराट जीवन उपस्थित है, इसलिए वे दर्शन-विचार-सिद्धांत के विषय में पुस्तकीय अथवा कोरे तर्कवादी ढंग से विचार नहीं करते। वे कहते हैं कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है : नहिं दरिद्र सम दुख जग
तुलसीदास : सुरसरि सम सब कहँ हित होई / 197