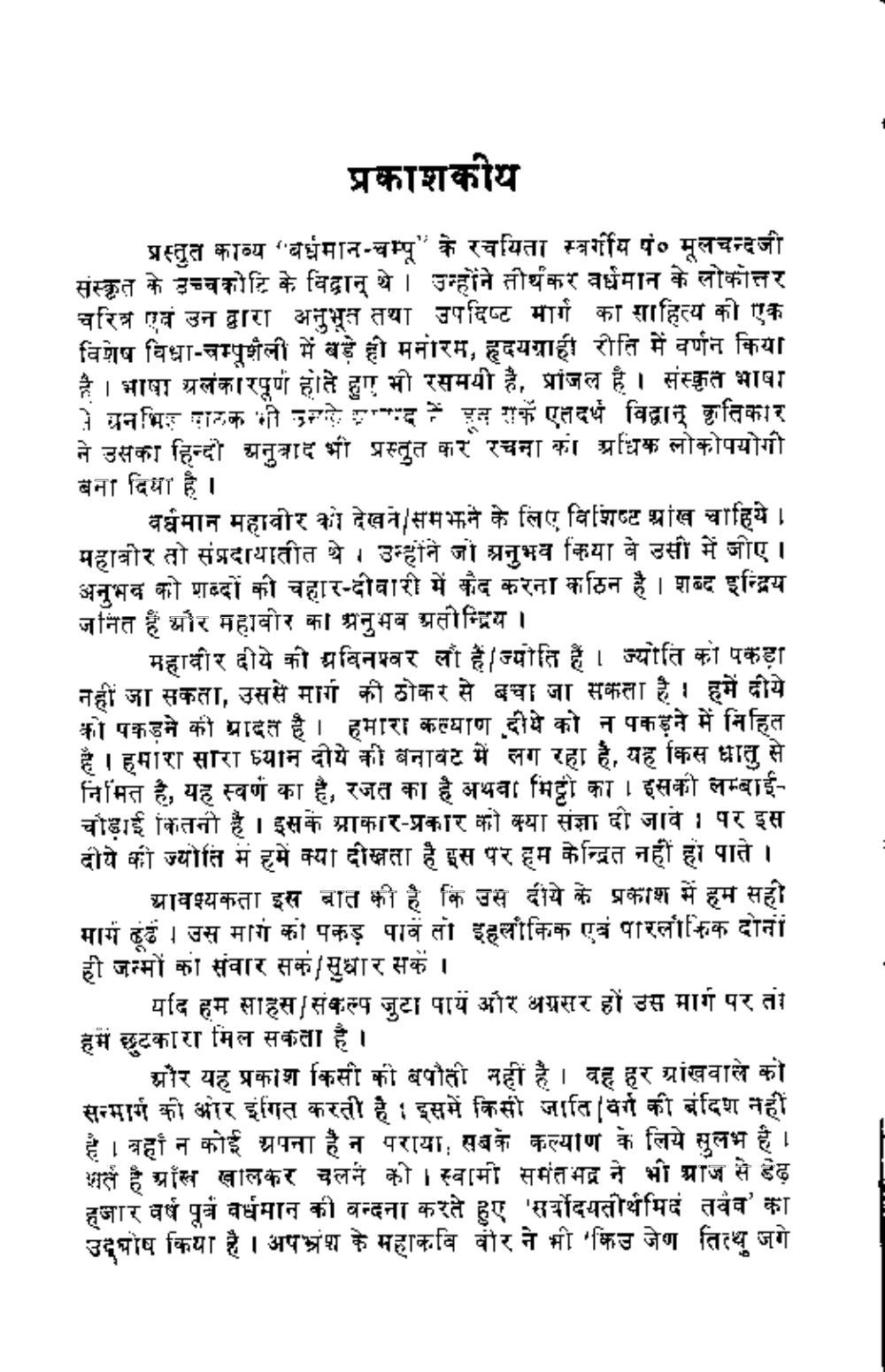________________
प्रकाशकीय
प्रस्तुत काव्य 'बर्धमान-चम्पू" के रचयिता स्वर्गीय पं० मूलचन्दजी संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान् थे | उन्होंने तीर्थंकर वर्धमान के लोकोत्तर चरित्र एवं उन द्वारा अनुभुत तथा उपदिष्ट मार्ग का साहित्य को एक विशेष विधा-चम्पुशैली में बड़े ही मनोरम, हृदयग्राही रीति में वर्णन किया है । भाषा अलंकारपूर्ण होते हुए भी रसमयी है, प्रांजल है। संस्कृत भाषा से अनभिः नाटक भीमद इल सक एतदर्थ विद्वान् कृतिकार ने उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत कर रचना का अधिक लोकोपयोगी बना दिया है।
वर्धमान महावीर को देखने समझने के लिए विशिष्ट प्रांख चाहिये। महाबीर तो संप्रदायातीत थे। उन्होंने जो अनुभव किया वे उसी में जीए । अनुभव को शब्दों की चहारदीवारी में कैद करना कठिन है । शब्द इन्द्रिय जनित हैं और महावीर का अनुभव अतीन्द्रिय ।
महावीर दीये की अविनम्वर लौ हैं। ज्योति हैं । ज्योति को पकड़ा नहीं जा सकता, उससे मार्ग की ठोकर से बचा जा सकता है। हमें दीये को पकड़ने की प्रादत है। हमारा कल्याण दीये को न पकड़ने में निहित है । हमारा सारा ध्यान दीये की बनावट में लग रहा है, यह किस धातु से निमित है, यह स्वर्ण का है, रजत का है अथवा मिट्टी का । इसकी लम्बाईचोड़ाई कितनी है । इसके प्राकार-प्रकार को क्या संज्ञा दी जावे। पर इस दीये की ज्योति में हमें क्या दीनता है इस पर हम केन्द्रित नहीं हो पाते।
आवश्यकता इस बात की है कि उस दीये के प्रकाश में हम सही मार्ग ढूढं । उस मार्ग को पकड़ पाव तो इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही जन्मों का संवार सकं/सुधार सके ।
यदि हम साहस संकल्प जूटा पायं और अग्रसर हों उस मार्ग पर तो हम छुटकारा मिल सकता है।
और यह प्रकाश किसी की बपौती नहीं है। वह हर अांखवाले को सन्मार्ग की ओर इंगित करती है । इसमें किसी जाति वर्ग की बंदिश नहीं है । बहाँ न कोई अपना है न पराया, सबके कल्याण के लिये सुलभ है। शर्त है आँख खालकर चलने की। स्वामी समंतभद्र ने भी पाज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व वर्धमान की बन्दना करते हुए 'सर्योदयतीर्थमिदं तवैव' का उद्घोष किया है । अपभ्रंश के महाकवि वीर ने भी किउ जेण तित्थ जगे