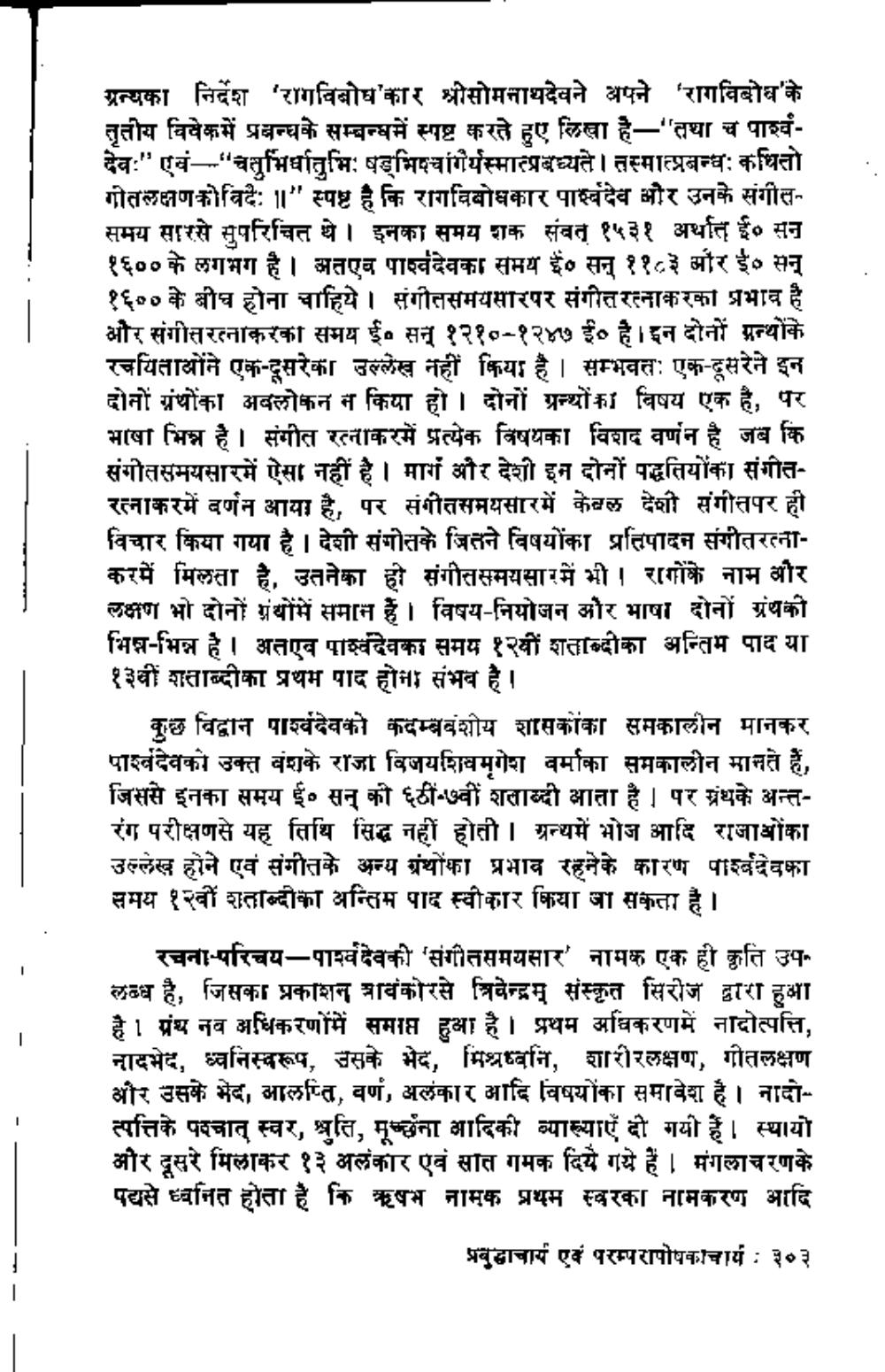________________
ग्रन्यका निर्देश 'रागविबोध'कार श्रीसोमनाथदेवने अपने 'रागविबोध'के तृतीय विवेक में प्रबन्धके सम्बन्धमें स्पष्ट करते हुए लिखा है-"तथा च पाचदेवः" एवं-"चतुभिर्धातुभिः षड्भिश्चांगर्यस्मात्प्रबध्यते। तस्मात्प्रबन्धः कधितो गोतलक्षणकोविदः ॥" स्पष्ट है कि रागविबोधकार पार्श्वदेव और उनके संगीतसमय सारसे सुपरिचित थे। इनका समय शक संवत् १५३१ अर्थात ई. सन १६०० के लगभग है । अतएव पावंदेवका समय ई० सन् ११८३ और ई० सन् १६०० के बीच होना चाहिये। संगीतसमयसारपर संगीतरत्नाकरका प्रभाव है और संगीतरत्नाकरका समय ई. सन् १२१०-१२४७ ई० है। इन दोनों ग्रन्थोंके रचयिताओंने एक-दूसरेका उल्लेख नहीं किया है। सम्भवत: एक-दूसरेने इन दोनों ग्रंथोंका अवलोकन न किया हो। दोनों ग्रन्थों का विषय एक है, पर भाषा भिन्न है। संगीत रत्नाकरमें प्रत्येक विषयका विशद वर्णन है जब कि संगीतसमयसारमें ऐसा नहीं है। मार्ग और देशी इन दोनों पद्धतियोंका संगीतरत्नाकरमें वर्णन आया है, पर संगीतसमयसारमें केवल देशी संगीतपर ही विचार किया गया है । देशी संगोतके जितने विषयोंका प्रतिपादन संगीतरत्नाकरमें मिलता है, उतनेका हो संगीतसमयसारमें भी। रागोंके नाम और लक्षण भी दोनों ग्रंथों में समान है। विषय-नियोजन और भाषा दोनों ग्रंथकी भिन्न-भिन्न है। अतएव पाश्चदेवका समय १२वीं शताब्दीका अन्तिम पाद या १३वीं शताब्दीका प्रथम पाद होना संभव है।
कुछ विद्वान पार्श्वदेवको कदम्बवंशीय शासकोंका समकालीन मानकर पार्श्वदेवको उक्त बंशके राजा विजयशिवमृगेश वर्माका समकालीन मानते हैं, जिससे इनका समय ई० सन् की ६ठी-७वीं शताब्दी आता है। पर ग्रंथके अन्तरंग परीक्षणसे यह तिथि सिद्ध नहीं होती। ग्रन्थमें भोज आदि राजाधोंका उल्लेख होने एवं संगीतके अन्य ग्रंथोंका प्रभाव रहने के कारण पार्श्वदेवका समय १२वीं शताब्दीका अन्तिम पाद स्वीकार किया जा सकता है।
रचना-परिचय-पार्श्वदेवको 'संगीतसमयसार' नामक एक ही कृति उपलब्ध है, जिसका प्रकाशन त्रावंकोरसे त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सिरीज द्वारा हुआ है। ग्रंथ नव अधिकरणोंमें समाप्त हुआ है। प्रथम अधिकरणमें नादोत्पत्ति, नादभेद, ध्वनिस्वरूप, उसके भेद, मिश्रध्वनि, शारीरलक्षण, गीतलक्षण और उसके भेद, आलप्ति, वर्ण, अलंकार आदि विषयोंका समावेश है। नादोत्पत्तिके पश्चात् स्वर, श्रुति, मूछना आदिकी व्याख्याएँ दी गयी है। स्थायो और दूसरे मिलाकर १३ अलंकार एवं सात गमक दिये गये हैं। मंगलाचरणके पद्यसे ध्वनित होता है कि ऋषभ नामक प्रथम स्वरका नामकरण आदि
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३०३