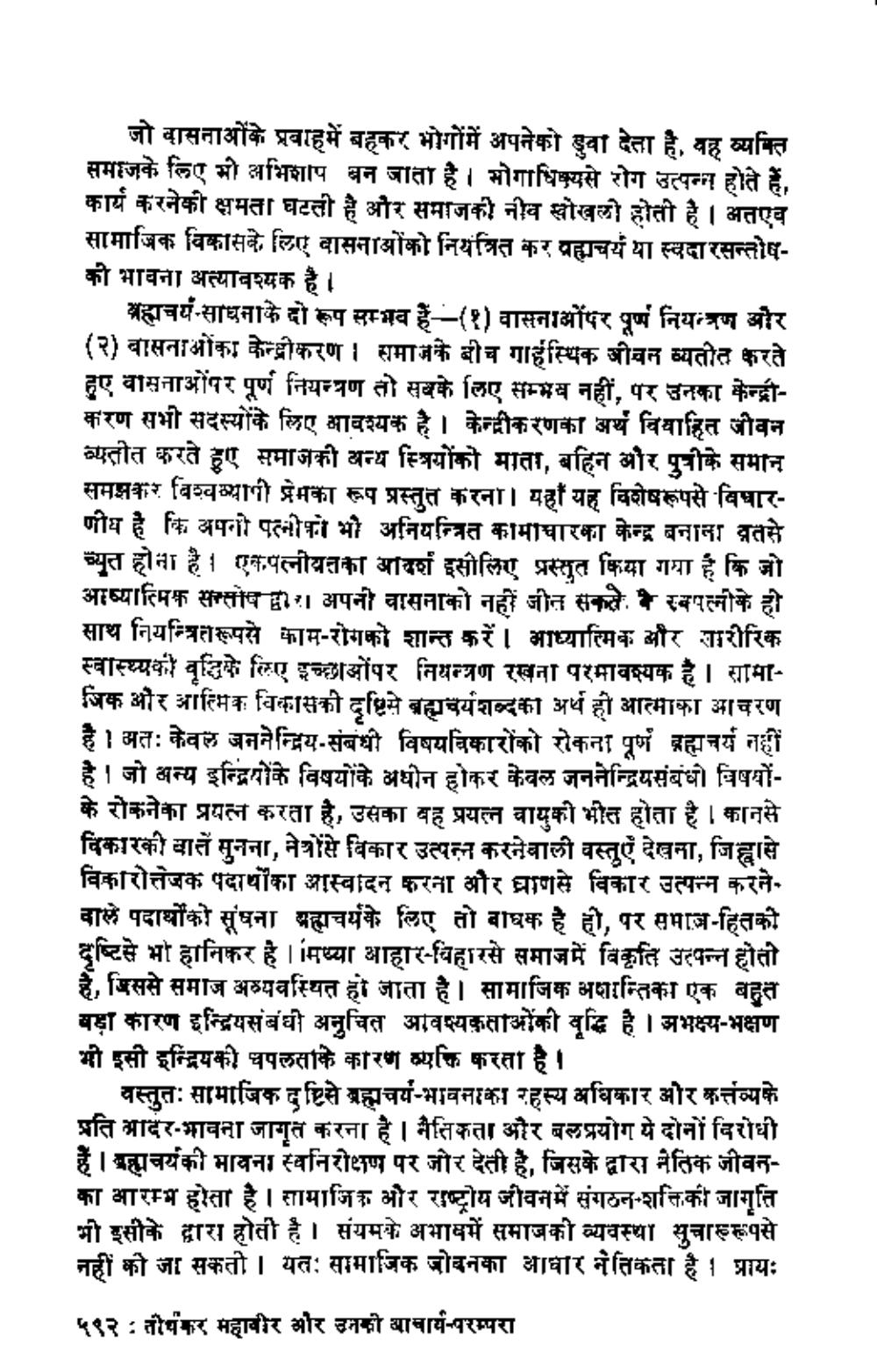________________
जो वासनाओंके प्रवाह में बहकर भोगोंमें अपनेको दुवा देता है, वह व्यक्ति समाज के लिए भी अभिशाप बन जाता है। मोगाधिक्यसे रोग उत्पन्न होते हैं, कार्य करनेकी क्षमता घटती है और समाजकी नीव खोखली होती है । अतएव सामाजिक विकास के लिए वासनाओंको नियंत्रित कर ब्रह्मचर्यं या स्वदा रसन्तोषकी भावना अत्यावश्यक है ।
ब्रह्मचर्यं साधना के दो रूप सम्भव हैं - (१) वासनाओंपर पूर्ण नियन्त्रण और (२) वासनाओंका केन्द्रीकरण । समाजके बीच गार्हस्थिक जीवन व्यतीत करते हुए वासनाओं पर पूर्ण नियन्त्रण तो सबके लिए सम्भव नहीं, पर उनका केन्द्रीकरण सभी सदस्योंके लिए आवश्यक है । केन्द्रीकरणका अर्थ विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए समाजकी अन्य स्त्रियोंको माता, बहिन और पुत्रीके समान समझकर विश्वव्यापी प्रेमका रूप प्रस्तुत करना । यहाँ यह विशेषरूपसे विचारणीव है कि अपनी पत्नीको भी अनियन्त्रित कामाचारका केन्द्र बनाना व्रतसे च्यूत होता है । एकपत्नीयतका आदर्श इसीलिए प्रस्तुत किया गया है कि जो आध्यात्मिक सम्तोष द्वार। अपनी वासनाको नहीं जीत सकते वे स्वपत्नी के ही साथ नियन्त्रितरूपसे काम- रोगको शान्त करें । आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धिके लिए इच्छाओं पर नियन्त्रण रखना परमावश्यक है। सामाजिक और आत्मिक विकासकी दृष्टिसे ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ हो आत्माका आचरण है | अतः केवल जननेन्द्रिय संबंधी विषयविकारोंको रोकना पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है । जो अन्य इन्द्रियोंके विषयोंके अधीन होकर केवल जननेन्द्रियसंबंधी विषयोंके रोकनेका प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न वायुकी भीत होता है । कानसे
कारकी बातें सुनना, नेत्रोंसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तुएँ देखना, जिह्वा से विकारोत्तेजक पदार्थोंका आस्वादन करना और घ्राणसे विकार उत्पन्न करनेवाले पदार्थों को सूंघना ब्रह्मचर्य के लिए तो बाघक है हो, पर समाज हितकी दृष्टिसे भो हानिकर है | मिथ्या आहार-विहारसे समाज में विकृति उत्पन्न होतो है, जिससे समाज अव्यवस्थित हो जाता है । सामाजिक अशान्तिका एक बहुत बड़ा कारण इन्द्रियसंबंधी अनुचित आवश्यकताओंकी वृद्धि है । अभक्ष्य भक्षण भी इसी इन्द्रियकी चपलताकै कारण व्यक्ति करता है ।
वस्तुतः सामाजिक दृष्टिले ब्रह्मचर्य - भावनाका रहस्य अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति आदर भावना जागृत करना है। नैतिकता और बलप्रयोग ये दोनों विरोधी हैं। ब्रह्मचर्य की भावना स्वनिरीक्षण पर जोर देती है, जिसके द्वारा नैतिक जीवनका आरम्भ होता है । सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में संगठन-शक्ति की जागृति भी इसीके द्वारा होती है । संयमके अभाव में समाजकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा सकती । यतः सामाजिक जोबनका आधार नैतिकता है । प्रायः
५९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी बाचार्य - परम्परा