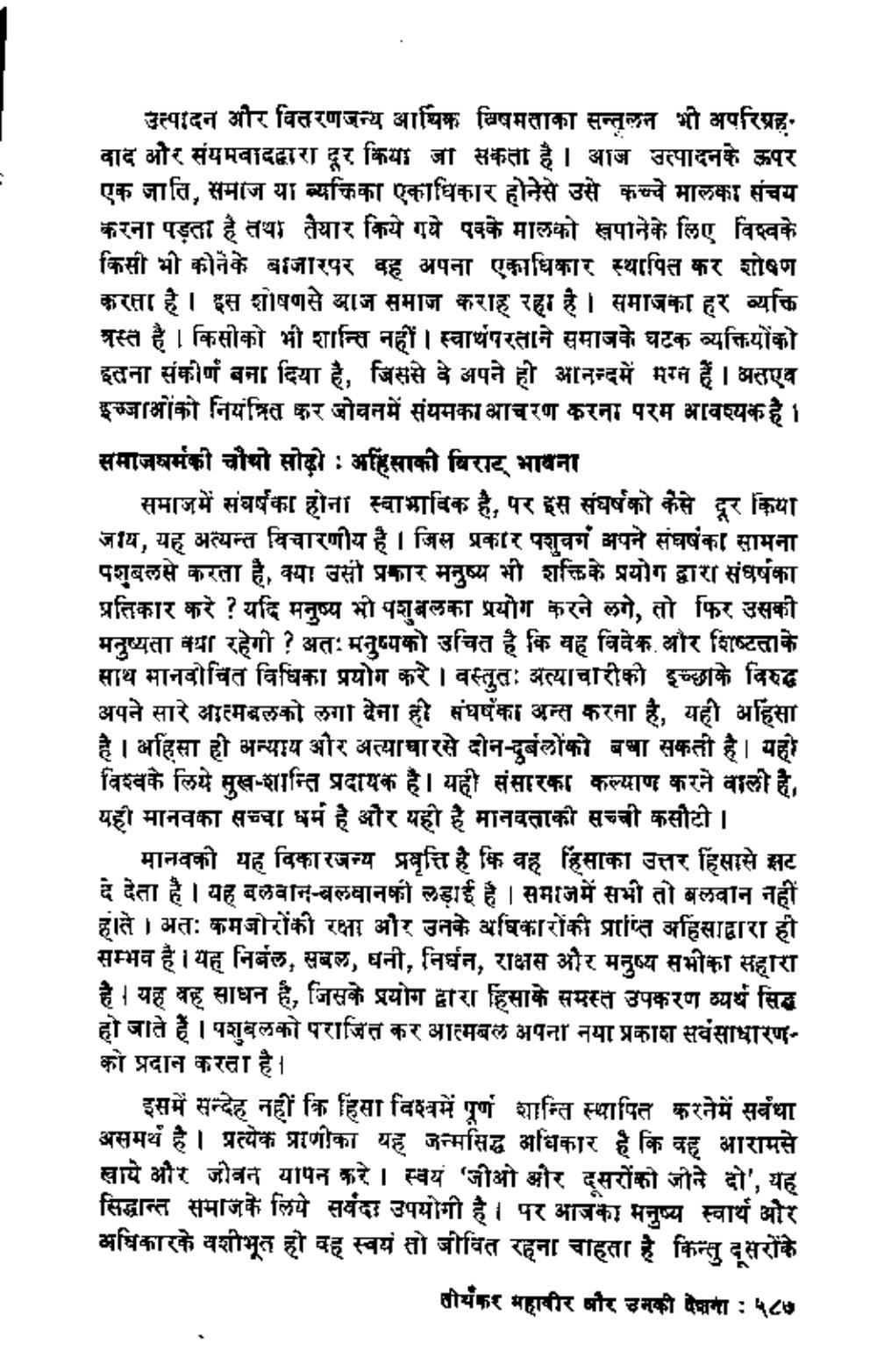________________
उत्पादन और वितरणजन्य आर्थिक विषमताका सन्तुलन भी अपरिग्रहदाद और संयमवादद्वारा दूर किया जा सकता है | आज उत्पादनके ऊपर एक जाति, समाज या व्यक्तिका एकाधिकार होनेसे उसे कच्चे मालका संचय करना पड़ता है तथा तैयार किये गये पक्के मालको खपानेके लिए विश्वके किसी भी कोनेके बाजारपर वह अपना एकाधिकार स्थापित कर शोषण करता है । इस शोषण से आज समाज कराह रहा है । समाजका हर व्यक्ति त्रस्त है | किसीको भी शान्ति नहीं | स्वार्थपरताने समाजके घटक व्यक्तियोंको इतना संकीर्ण बना दिया है, जिससे वे अपने ही आनन्दमें मग्न हैं । अतएव इच्जाओको नियंत्रित कर जोवनमें संयमका आचरण करना परम आवश्यक है । समाजधर्मकी चौथो सोढ़ी: अहिंसाकी विराट् भावना
समाज में संघर्षका होना स्वाभाविक है, पर इस संघर्षको कैसे दूर किया जाय, यह अत्यन्त विचारणीय है । जिस प्रकार पशुवगं अपने संघर्षका सामना पशुबलसे करता है, क्या उसी प्रकार मनुष्य भी शक्तिके प्रयोग द्वारा संघर्षका प्रतिकार करे ? यदि मनुष्य भी पशुबलका प्रयोग करने लगे, तो फिर उसकी मनुष्यता क्या रहेगी ? अतः मनुष्यको उचित है कि यह विवेक और शिष्टता के साथ मानवोचित विधिका प्रयोग करे । वस्तुतः अत्याचारीको इच्छाके विरुद्ध अपने सारे आत्मबलको लगा देना ही संघर्षका अन्त करना है, यही अहिंसा है | अहिसा ही अन्याय और अत्याचारसे दोन दुर्बलोंको बचा सकती है । यहो विश्व के लिये सुख-शान्ति प्रदायक है। यही संसारका कल्याण करने वाली है, यही मानवका सच्चा धर्म है और यही है मानवताकी सच्ची कसौटी |
मानवकी यह विकारजन्य प्रवृत्ति है कि वह हिंसाका उत्तर हिंसासे झट दे देता है । यह बलवान बलवानकी लड़ाई है। समाज में सभी तो बलवान नहीं होते । अतः कमजोरों की रक्षा और उनके अधिकारोंकी प्राप्ति अहिंसाद्वारा ही सम्भव है | यह निर्बल, सबल, धनी, निर्धन, राक्षस और मनुष्य सभीका सहारा है । यह वह साधन है, जिसके प्रयोग द्वारा हिंसाके समस्त उपकरण व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं । पशुबलको पराजित कर आत्मबल अपना नया प्रकाश सर्वसाधारणको प्रदान करता है ।
इसमें सन्देह नहीं कि हिंसा विश्वमें पूर्ण शान्ति स्थापित करनेमें सबंधा असमर्थ है । प्रत्येक प्राणीका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह आरामसे खाये और जीवन यापन करे । स्वयं 'जीओ और दूसरोंको जीने दो', यह सिद्धान्त समाज के लिये सर्वदा उपयोगी है । पर आज का मनुष्य स्वार्थ और अधिकारके वशीभूत हो वह स्वयं तो जीवित रहना चाहता है किन्तु दूसरोंके
तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५८७