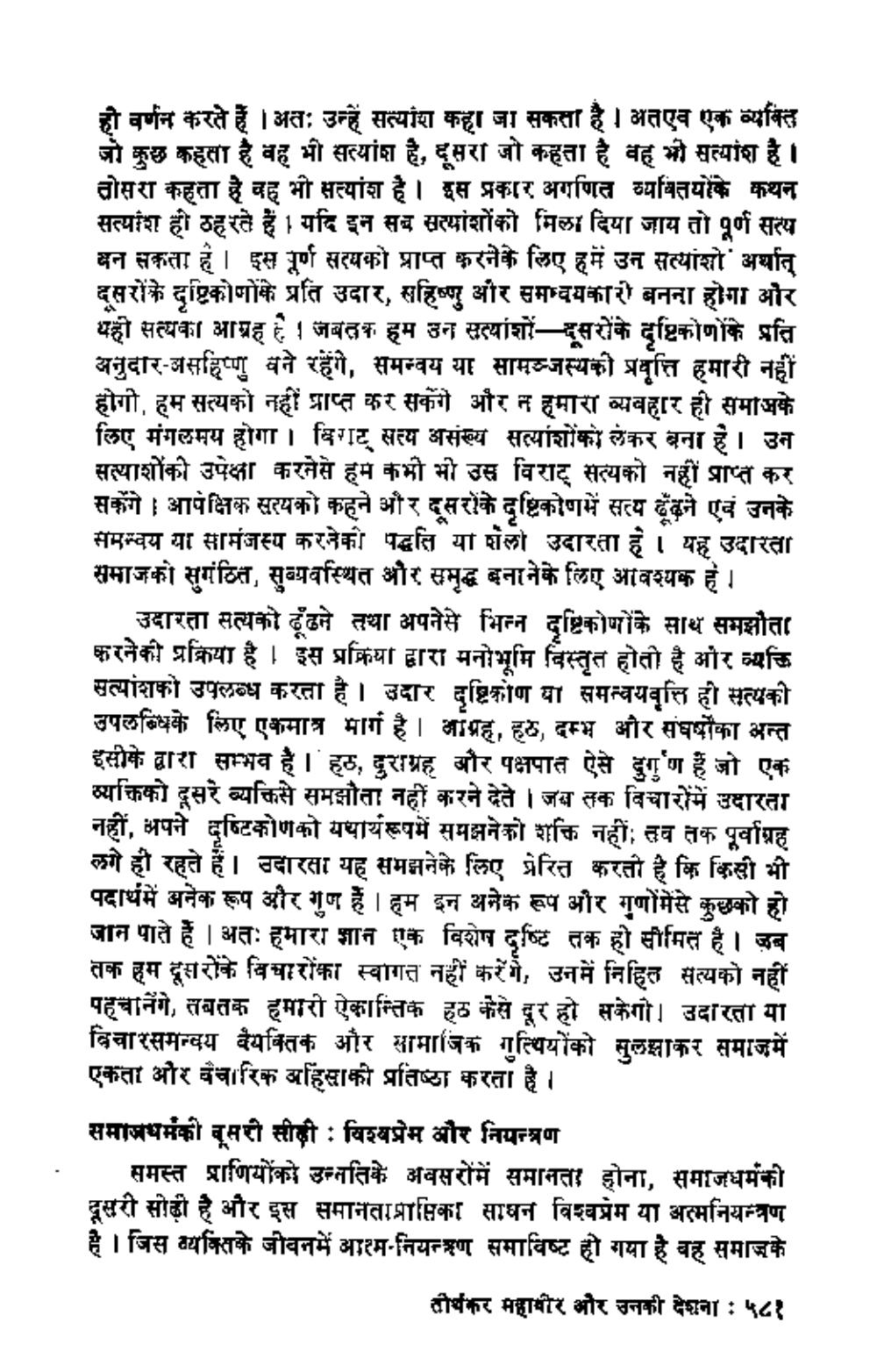________________
हो वर्णन करते हैं । अत: उन्हें सत्यांश कहा जा सकता है । अतएव एक व्यक्ति जो कुछ कहता है वह भी सत्यांश है, दूसरा जो कहता है वह भी सत्यांश है । तीसरा कहता है वह भी सत्यांश है । इस प्रकार अगणित व्यक्तियोंके कथन सत्यांश ही ठहरते हैं। यदि इन सब सत्यांशों को मिला दिया जाय तो पूर्ण सत्य बन सकता है। इस पूर्ण सत्यको प्राप्त करने के लिए हमें उन सत्यांशों अर्थात् दूसरोंके दृष्टिकोणोंके प्रति उदार, सहिष्णु और समन्वयकारी बनना होगा और यही सत्यका आग्रह है । जबतक हम उन सत्यांशों – दूसरोंके दृष्टिकोणोंके प्रति अनुदार असहिष्णु वने रहेंगे, समन्वय या सामञ्जस्यकी प्रवृत्ति हमारी नहीं होगी, हम सत्यको नहीं प्राप्त कर सकेंगे और न हमारा व्यवहार ही समाजके लिए मंगलमय होगा । विराट् सत्य असंख्य सत्यांशोंको लेकर बना है । उन सत्याशोंकी उपेक्षा करनेसे हम कभी भी उस विराट् सत्यको नहीं प्राप्त कर सकेंगे । आपेक्षिक सत्यको कहने और दूसरोंके दृष्टिकोणमें सत्य ढूँढ़ने एवं उनके समन्वय या सामंजस्य करनेकी पद्धति या शैली उदारता है । यह उदारता समाजको सुगठित, सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है ।
उदारता सत्यको ढूँढने तथा अपनेसे भिन्न दृष्टिकोणोंके साथ समझौता करने की प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया द्वारा मनोभूमि विस्तृत होती है और व्यक्ति सत्यांशको उपलब्ध करता है । उदार दृष्टिकोण या समन्वयवृत्ति ही सत्यको उपलब्धि के लिए एकमात्र मार्ग है। आंग्रह, हठ, दम्भ और संघर्षका अन्त इसीके द्वारा सम्भव है । हठ, दुराग्रह और पक्षपात ऐसे दुर्गाण है जो एक व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिसे समझौता नहीं करने देते । जब तक विचारोंमें उदारता नहीं, अपने दृष्टिकोणको यथार्थरूपमें समझनेको शक्ति नहीं, तब तक पूर्वाग्रह लगे ही रहते हैं । उदारता यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि किसी भी पदार्थ में अनेक रूप और गुण है । हम इन अनेक रूप और गुणोंमेंसे कुछको हो जान पाते हैं । अतः हमारा ज्ञान एक विशेष दृष्टि तक ही सीमित है । जब तक हम दूसरोंके विचारोंका स्वागत नहीं करेंगे, उनमें निहित सत्यको नहीं पहचानेंगे, तबतक हमारी ऐकान्तिक हठ कैसे दूर हो सकेगी। उदारता या विचारसमन्वय वैयक्तिक और सामाजिक गुत्थियोंको सुलझाकर समाज में एकता और वैचारिक अहिंसा की प्रतिष्ठा करता है ।
समाजधमकी दूसरी सीही विश्वप्रेम और नियन्त्रण
समस्त प्राणियोंको उन्नति के अवसरोंमें समानता होना, समाजधमंकी दूसरी सीढ़ी है और इस समानताप्राप्तिका साधन विश्वप्रेम या अत्मनियन्त्रण है । जिस व्यक्ति जीवनमें आत्म-नियन्त्रण समाविष्ट हो गया है वह समाज के
तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ५८१