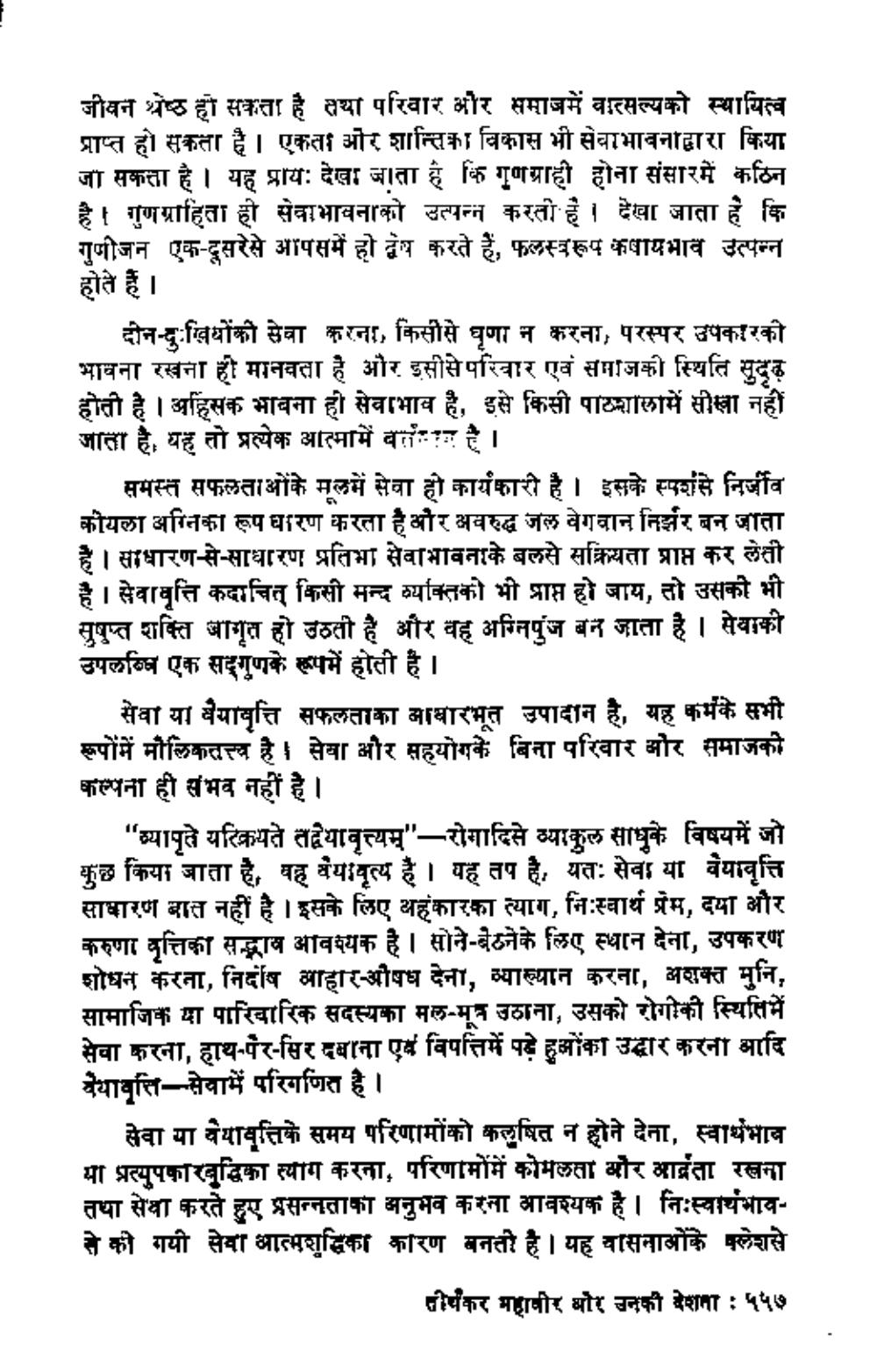________________
जीवन श्रेष्ठ हो सकता है तथा परिवार और समाजमें वात्सल्यको स्थायित्व प्राप्त हो सकता है। एकता और शान्तिका विकास भी सेवाभावनाद्वारा किया जा सकता है । यह प्रायः देखा जाता है कि गुणग्राही होना संसार में कठिन है। गुणग्राहिता ही सेवाभावनाको उत्पन्न करती है। देखा जाता है कि गुणीजन एक-दुसरेसे आपसमें हो द्वेष करते हैं, फलस्वरूप कषायभाव उत्पन्न होते हैं। __ दीन-दुःखियोंकी सेवा करना, किसीसे घृणा न करना, परस्पर उपकारको भावना रखना ही मानवता है और इसीसे परिवार एवं समाजकी स्थिति सुदढ़ होती है । अहिंसक भावना ही सेवाभाव है, इसे किसी पाठशालामें सीखा नहीं जाता है, यह तो प्रत्येक आत्मामें वर्ता है।
समस्त सफलताओंके मूलमें सेवा हो कार्यकारी है। इसके स्पर्शसे निर्जीव कोयला अग्निका रूप धारण करता है और अवरुद्ध जल वेगवान निर्झर बन जाता है । साधारण-से-साधारण प्रतिभा सेवाभावनाके बलसे सक्रियता प्राप्त कर लेती है । सेवावृत्ति कदाचित् किसी मन्द व्यक्तिको भी प्राप्त हो जाय, तो उसको भी सुषुप्त शक्ति जागत हो उठती है और वह अग्निपुंज बन जाता है । सेवाकी उपलब्धि एक सद्गुणके रूप में होती है ।
सेवा या वैयावृत्ति सफलताका आधारभूत उपादान है, यह कर्मके सभी रूपों में मौलिकतत्त्व है। सेवा और सहयोगके बिना परिवार और समाजको कल्पना ही संभव नहीं है।
__ "व्याप्ते यरिक्रयते तद्वयावृत्त्यम्"-रोगादिसे व्याकुल साधुके विषयमें जो कुछ किया जाता है, वह वेयावृत्य है। यह तप है, यतः सेवा या वैयावृत्ति साधारण बात नहीं है । इसके लिए अहंकारका त्याग, निःस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा वृत्तिका सद्भाव आवश्यक है । सोने-बैठने के लिए स्थान देना, उपकरण शोधन करना, निर्दोष आहार-औषध देना, व्याख्यान करना, अशक्त मुनि, सामाजिक या पारिवारिक सदस्यका मल-मूत्र उठाना, उसको रोगीकी स्थितिमें सेवा करना, हाथ-पैर-सिर दबाना एवं विपत्तिमें पड़े हुओंका उद्धार करना आदि यावृत्ति-सेवामें परिगणित है।
सेवा या वैयावृत्तिके समय परिणामोंको कलुषित न होने देना, स्वार्थभाव या प्रत्युपकारवृद्धिका स्याग करना, परिणामोंमें कोमलता और आर्द्रता रखना तथा सेवा करते हुए प्रसन्नताका अनुभव करना आवश्यक है । निःस्वार्थभावसे की गयी सेवा आत्मशुद्धिका कारण बनती है। यह वासनाओंके क्लेशसे
तीर्थकर महावीर और उनकी देशना : ५५५