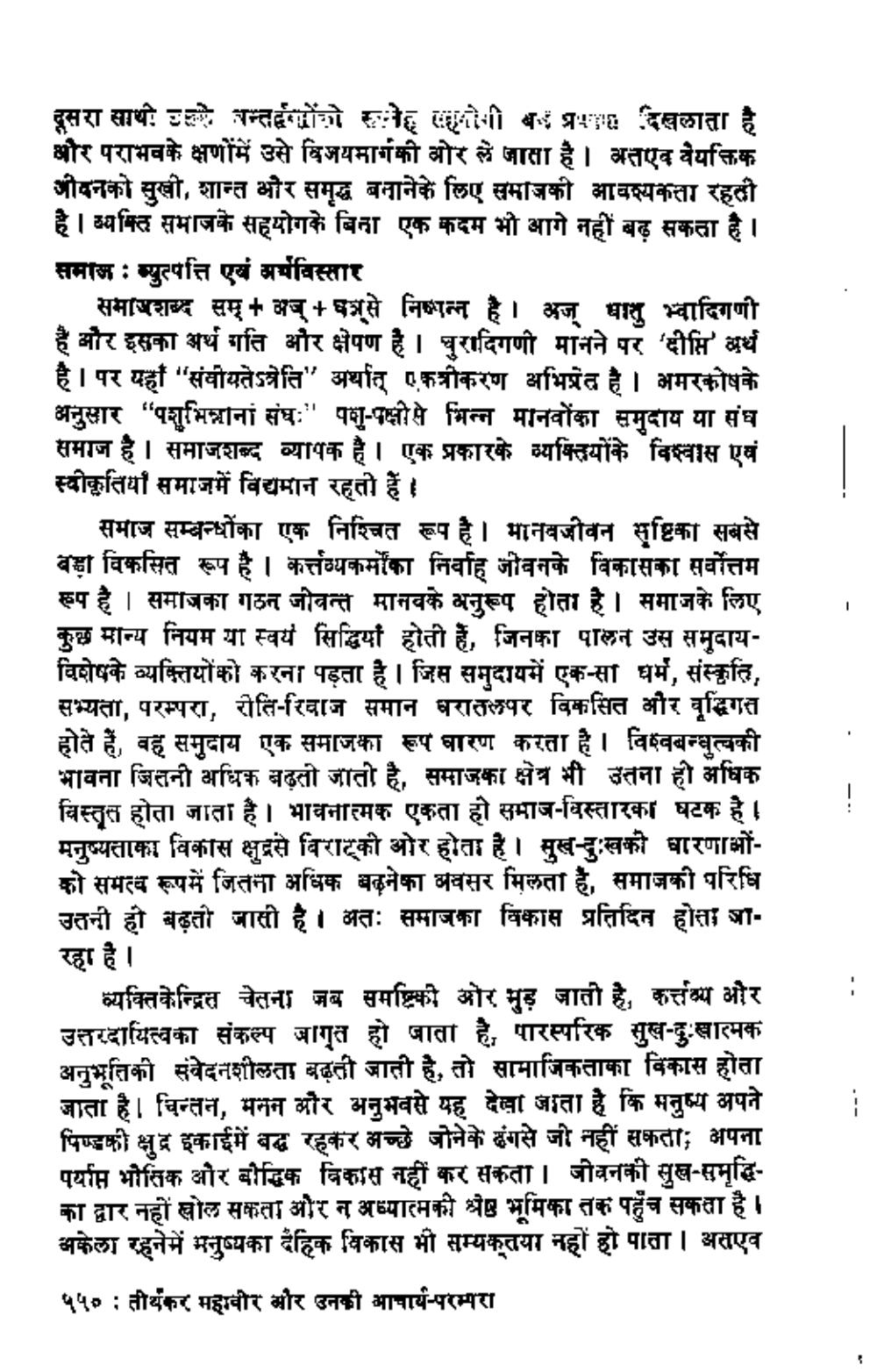________________
दूसरा साथी जो अन्तर्द्वन्नोंको सलेह लगोगी
ब दखलाता है और पराभव के क्षणों में उसे विजयमार्गकी ओर ले जाता है। अतएव वैयक्तिक जीवनको सुखी, शान्त और समृद्ध बनानेके लिए समाजकी आवश्यकता रहती है । व्यक्ति समाजके सहयोगके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है । समाज : म्युत्पत्ति एवं अर्थविस्तार
समाषशब्द सम् + अ + पसे निष्पन्न है। अज् धातु भ्वादिगणी है और इसका अर्थ गति और क्षेपण है | चुरादिगणी मानने पर 'दीप्ति' अर्थ है। पर यहाँ "संवीयतेऽत्रेति" अर्थात् एकत्रीकरण अभिप्रेत है । अमरकोषके अनुसार “पशुभिन्नानां संघः' पशु-पक्षीसे भिन्न मानवोंका समुदाय या संघ समाज है। समाजशब्द व्यापक है। एक प्रकारके व्यक्तियोंके विश्वास एवं स्वीकृतियाँ समाजमें विद्यमान रहती हैं।
समाज सम्बन्धोंका एक निश्चित रूप है। मानवजीवन सृष्टिका सबसे बझा विकसित रूप है। कर्त्तव्यकर्मोका निर्वाह जीवनके विकासका सर्वोत्तम रूप है | समाजका गठन जीवन्त मानवके अनुरूप होता है। समाजके लिए कुछ मान्य नियम या स्वयं सिद्धियां होती हैं, जिनका पालन उस समुदायविशेषके व्यक्तियों को करना पड़ता है । जिस समुदायमें एक-सा धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, रीति-रिवाज समान घरातलपर विकसित और वृद्धिंगत होते हैं, वह समुदाय एक समाजका रूप धारण करता है । विश्वबन्धुत्वकी भावना जितनी अधिक बढ़ती जाती है, समाजका क्षेत्र भी उतना ही अधिक विस्तृत होता जाता है। भावनात्मक एकता हो समाज-विस्तारका घटक है। मनुष्यताका विकास क्षुद्रसे विराट्की ओर होता है। सुख-दुःखको धारणाओंको समत्व रूप में जितना अधिक बढ़नेका अवसर मिलता है, समाजकी परिधि उतनी ही बढ़ती जाती है। अतः समाजका विकास प्रतिदिन होता जा
व्यक्तिकेन्द्रित चेतना जब समष्टिकी ओर मुड़ जाती है, कर्तव्य और उत्तरदायित्वका संकल्प जागृत हो जाता है, पारस्परिक सुख-दुःखात्मक अनुभूतिकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, तो सामाजिकताका विकास होता जाता है। चिन्तन, मनन और अनुभवसे यह देखा जाता है कि मनुष्य अपने पिण्डकी क्षुद्र इकाईमें बद्ध रहकर अच्छे जोनेके दंगसे जी नहीं सकता; अपना पर्याप्त भौसिक और बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। जीवनकी सुख-समृद्धिका द्वार नहीं खोल सकता और न अध्यात्मको श्रेष्ठ भूमिका तक पहुंच सकता है। अकेला रहने में मनुष्यका दैहिक विकास भी सम्यक्तया नहीं हो पाता । अतएव ५५० : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा