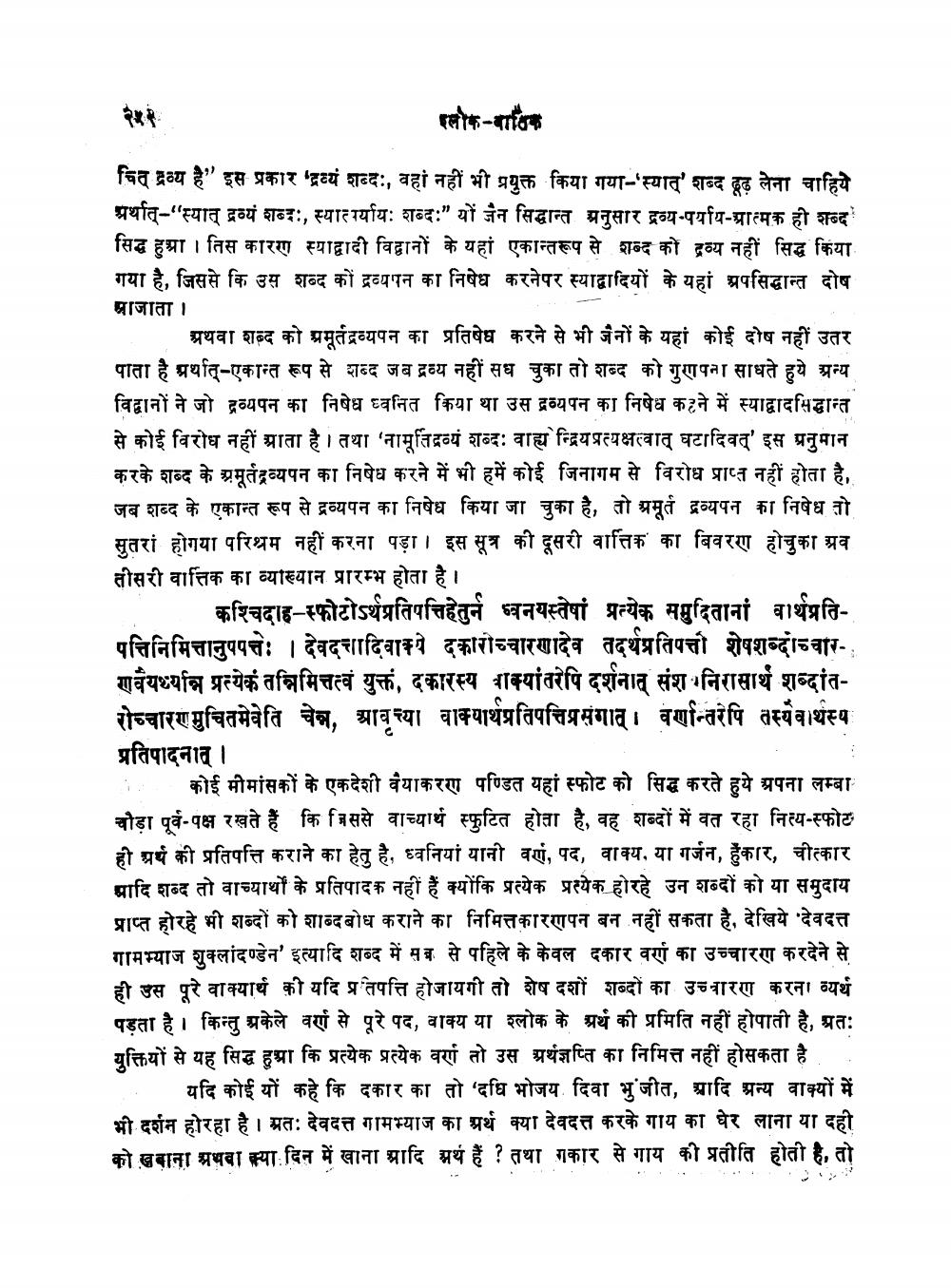________________
२५२
rate-arton
चित् द्रव्य है" इस प्रकार 'द्रव्यं शब्दः, वहां नहीं भी प्रयुक्त किया गया- ' स्यात्' शब्द ढूढ़ लेना चाहिये अर्थात् -" स्यात् द्रव्यं शब्दः स्यात्ययः शब्दः " यों जैन सिद्धान्त अनुसार द्रव्य-पर्याय- प्रात्मक ही शब्द सिद्ध हुआ । तिस कारण स्याद्वादी विद्वानों के यहां एकान्तरूप से शब्द को द्रव्य नहीं सिद्ध किया गया है, जिससे कि उस शब्द कों द्रव्यपन का निषेध करनेपर स्याद्वादियों के यहां अपसिद्धान्त दोष
श्राजाता ।
अथवा शब्द को अमूर्तद्रव्यपन का प्रतिषेध करने से भी जैनों के यहां कोई दोष नहीं उतर पाता है अर्थात् एकान्त रूप से शब्द जब द्रव्य नहीं सघ चुका तो शब्द को गुणपना साधते हुये अन्य विद्वानों ने जो द्रव्यपन का निषेध ध्वनित किया था उस द्रव्यपन का निषेध कहने में स्याद्वाद सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं आता है। तथा 'नामूर्तिद्रव्यं शब्दः वाह्य ेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात् घटादिवत्' इस प्रनुमान करके शब्द के अमूर्तद्रव्यपन का निषेध करने में भी हमें कोई जिनागम से विरोध प्राप्त नहीं होता है, जब शब्द के एकान्त रूप से द्रव्यपन का निषेध किया जा चुका है, तो अमूर्त द्रव्यपन का निषेध तो सुतरां होगया परिश्रम नहीं करना पड़ा। इस सूत्र की दूसरी वार्तिक का विवरण होचुका अव तीसरी वार्तिक का व्याख्यान प्रारम्भ होता है ।
कश्चिदाह-स्फोटोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुर्न ध्वनयस्तेषां प्रत्येक समुदितानां वार्थप्रतिपत्तिनिमित्तानुपपत्तेः । देवदत्तादिवाक्ये दकारोच्चारणादेव तदर्थप्रतिपत्ती शेषशब्दोच्चार-: णर्वैयर्थ्यान्न प्रत्येकं तन्निमित्तत्वं युक्तं, दकारस्य वाक्यांतरेपि दर्शनात् संश निरासार्थं शब्दांत - रोच्चारणमुचितमेवेति चेन्न, आवृत्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रसंगात् । वर्णान्तरेपि तस्यैवार्थस्प प्रतिपादनात् ।
कोई मीमांसकों के एकदेशी वैयाकरण पण्डित यहां स्फोट को सिद्ध करते हुये अपना लम्बा चौड़ा पूर्व - पक्ष रखते हैं कि जिससे वाच्यार्थ स्फुटित होता है, वह शब्दों में वत रहा नित्य-स्फोट ही अर्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु है, ध्वनियां यानी वर्ण, पद, वाक्य, या गर्जन, हुँकार, चीत्कार आदि शब्द तो वाच्यार्थी के प्रतिपादक नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक होरहे उन शब्दों को या समुदाय प्राप्त हो रहे भी शब्दों को शाब्दबोध कराने का निमित्तकारणपन बन नहीं सकता है, देखिये 'देवदत्त गामभ्याज शुक्लांदण्डेन' इत्यादि शब्द में सब से पहिले के केवल दकार वर्ण का उच्चारण करदेने से ही उस पूरे वाक्यार्थ की यदि प्रतिपत्ति होजायगी तो शेष दशों शब्दों का उच्चारण करना व्यर्थ पड़ता है । किन्तु अकेले वर्ण से पूरे पद, वाक्य या श्लोक के अर्थ की प्रमिति नहीं होपाती है, अतः युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ग तो उस अर्थज्ञप्ति का निमित्त नहीं हो सकता है यदि कोई यों कहे कि दकार का तो 'दधि भोजय दिवा भुंजीत, आदि अन्य वाक्यों में भी दर्शन होरहा है । म्रतः देवदत्त गामभ्याज का अर्थ क्या देवदत्त करके गाय का घेर लाना या दही को खबाना अथवा क्या दिन में खाना आदि अर्थ हैं ? तथा गकार से गाय की प्रतीति होती है, तो