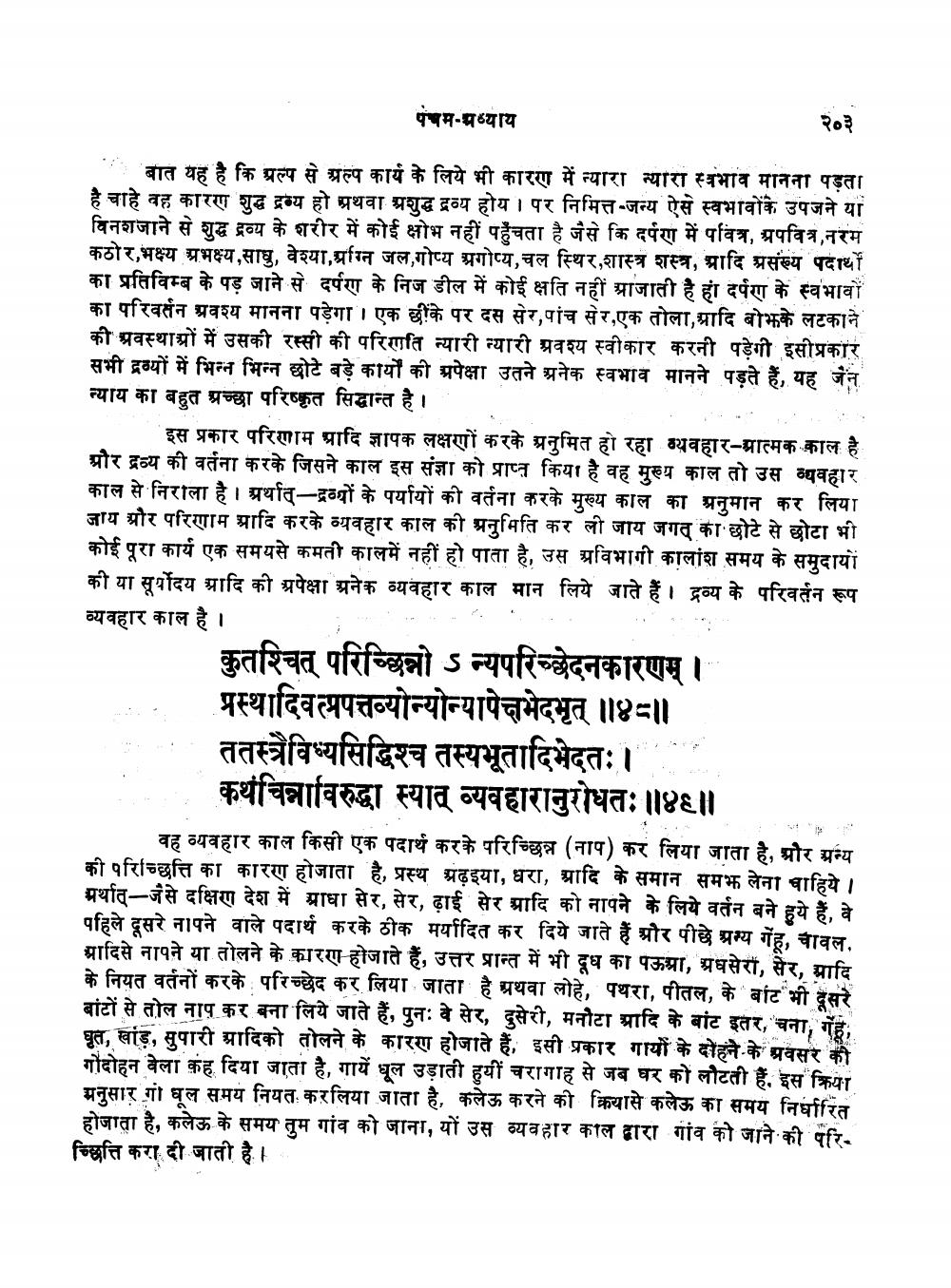________________
पंचम-प्रध्याय
२०३
बात यह है कि अल्प से अल्प कार्य के लिये भी कारण में न्यारा न्यारा स्वभाव मानना पड़ता है चाहे वह कारण शुद्ध द्रग्य हो अथवा अशुद्ध द्रव्य होय । पर निमित्त-जन्य ऐसे स्वभावोंके उपजने या विनशजाने से शुद्ध द्रव्य के शरीर में कोई क्षोभ नहीं पहुँचता है जैसे कि दर्पण में पवित्र, अपवित्र,नरम कठोर,भक्ष्य अभक्ष्य,साधु, वेश्या,अग्नि जल,गोप्य अगोप्य,चल स्थिर,शास्त्र शस्त्र, आदि असंख्य पदार्थों का प्रतिविम्ब के पड़ जाने से दर्पण के निज डील में कोई क्षति नहीं आजाती है हा दर्पण के स्वभावों का परिवर्तन अवश्य मानना पड़ेगा। एक छींके पर दस सेर,पांच सेर,एक तोला,आदि बोझके लटकाने की अवस्थाओं में उसकी रस्सी की परिणति न्यारी न्यारी अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी इसीप्रकार सभी द्रव्यों में भिन्न भिन्न छोटे बड़े कार्यों की अपेक्षा उतने अनेक स्वभाव मानने पड़ते हैं, यह जैन न्याय का बहुत अच्छा परिष्कृत सिद्धान्त है।
इस प्रकार परिणाम प्रादि ज्ञापक लक्षणों करके अनुमित हो रहा व्यवहार-मात्मक काल है और द्रव्य की वर्तना करके जिसने काल इस संज्ञा को प्राप्त किया है वह मुख्य काल तो उस व्यवहार काल से निराला है। अर्थात्-द्रव्यों के पर्यायों की वर्तना करके मुख्य काल का अनुमान कर लिया जाय और परिणाम आदि करके व्यवहार काल की अनुमिति कर ली जाय जगत् का छोटे से छोटा भी कोई पूरा कार्य एक समयसे कमती कालमें नहीं हो पाता है, उस अविभागी कालांश समय के समुदायों की या सूर्योदय आदि की अपेक्षा अनेक व्यवहार काल मान लिये जाते हैं। द्रव्य के परिवर्तन रूप व्यवहार काल है।
कुतश्चित् परिच्छिन्नो ऽ न्यपरिच्छेदनकारणम् । प्रस्थादिवत्प्रपत्तव्योन्योन्यापेक्षभेदभृत् ॥४॥ ततस्त्रैविध्यसिद्धिश्च तस्यभूतादिभेदतः।
कथंचिन्नाविरुद्धा स्यात् व्यवहारानुरोधतः॥४६॥ वह व्यवहार काल किसी एक पदार्थ करके परिच्छिन्न (नाप) कर लिया जाता है, और अन्य कीरिच्छित्ति का कारण होजाता है, प्रस्थ अढडया. धरा. आदि के समान समझ लेता चाहिये। अर्थात्-जैसे दक्षिण देश में प्राधा सेर, सेर, ढ़ाई सेर आदि को नापने के लिये वर्तन बने हये हैं, वे पहिले दूसरे नापने वाले पदार्थ करके ठीक मर्यादित कर दिये जाते हैं और पीछे अन्य गेंह, चावल. आदिसे नापने या तोलने के कारण होजाते हैं, उत्तर प्रान्त में भी दूध का पऊया, अधसेरा, सेर, आदि के नियत वर्तनों करके परिच्छेद कर लिया जाता है अथवा लोहे, पथरा, पीतल, के बांट भी दूसरे बांटों से तोल नाप कर बना लिये जाते हैं, पुनः वे सेर, दुसेरी, मनोटा आदि के बांट इतर, चना, गेंह, घृत, खांड़, सुपारी आदिको तोलने के कारण होजाते हैं, इसी प्रकार गायों के दोहने के अवसर को गोदोहन वेला कह दिया जाता है, गायें धूल उड़ाती हयीं चरागाह से जब घर को लौटती है. इस कि मनुसार गो धूल समय नियतः करलिया जाता है, कलेऊ करने की क्रियासे कलेऊ का समय निर्धारित होजाता है, कलेऊ के समय तुम गांव को जाना, यों उस व्यवहार काल द्वारा गांव को जाने की परिच्छित्ति करा दी जाती है।