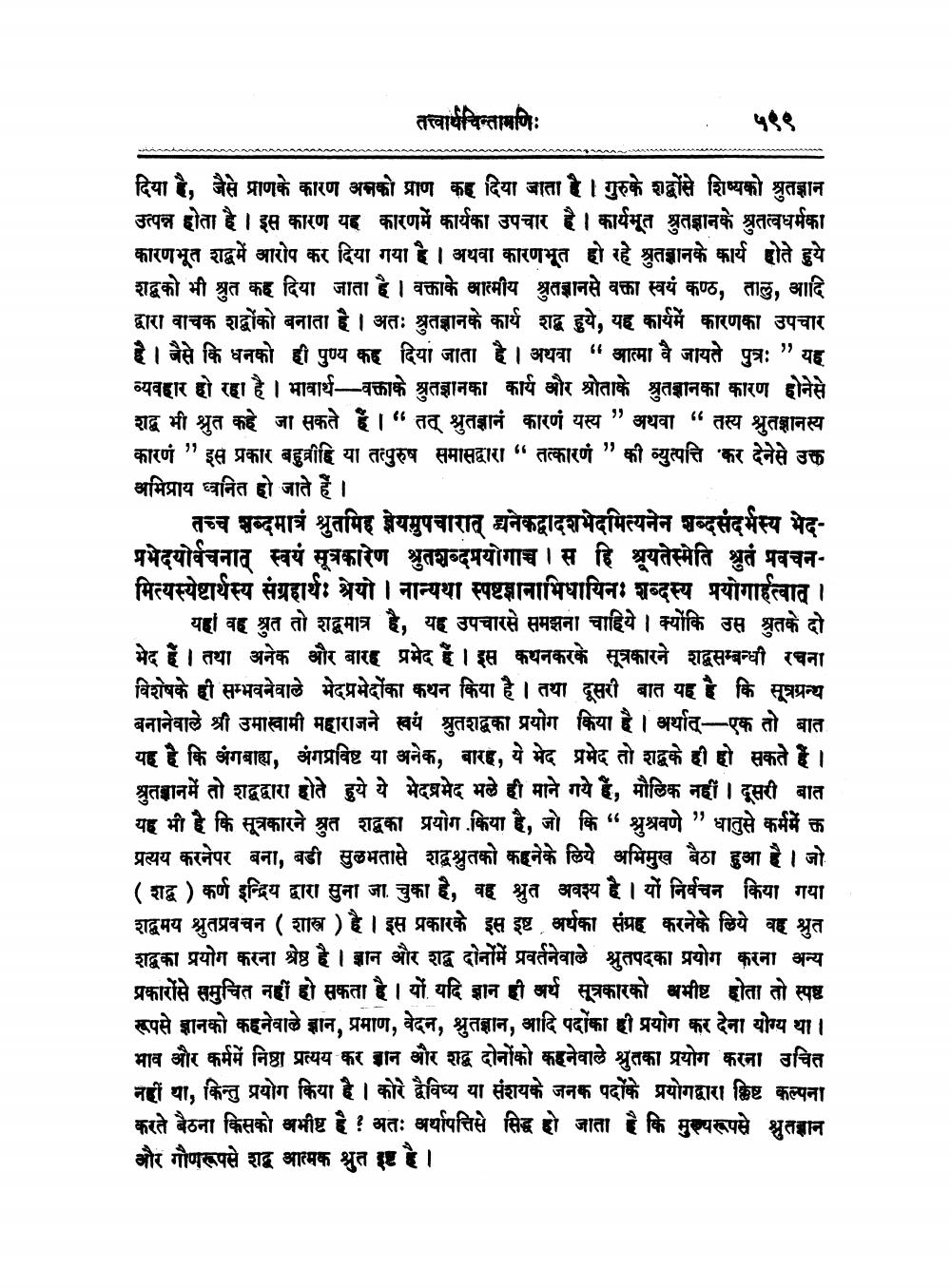________________
तत्त्वार्थचिन्तामणिः
दिया है, जैसे प्राणके कारण अबको प्राण कह दिया जाता है । गुरुके शवोंसे शिष्यको श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । इस कारण यह कारणमें कार्यका उपचार है। कार्यभूत श्रुतज्ञानके श्रुतत्वधर्मका कारणभूत शद्बमें आरोप कर दिया गया है । अथवा कारणभूत हो रहे श्रुतज्ञानके कार्य होते हुये शब्दको भी श्रुत कह दिया जाता है । वक्ताके आत्मीय श्रुतज्ञानसे वक्ता स्वयं कण्ठ, तालु, आदि द्वारा वाचक शद्वोंको बनाता है । अतः श्रुतज्ञानके कार्य शब्द हुये, यह कार्यमें कारणका उपचार है। जैसे कि धनको ही पुण्य कह दिया जाता है । अथवा " आत्मा वै जायते पुत्रः " यह व्यवहार हो रहा है । भावार्थ-वक्ताके श्रुतज्ञानका कार्य और श्रोताके श्रुतज्ञानका कारण होनेसे शब्द भी श्रुत कहे जा सकते हैं । " तत् श्रुतज्ञानं कारणं यस्य " अथवा " तस्य श्रुतज्ञानस्य कारणं " इस प्रकार बहुव्रीहि या तत्पुरुष समासद्वारा " तत्कारणं " की व्युत्पत्ति कर देनेसे उक अभिप्राय ध्वनित हो जाते हैं।
तच्च शब्दमानं श्रुतमिह ज्ञेयमुपचारात् घनेकद्वादशभेदमित्यनेन शब्दसंदर्भस्य भेदप्रभेदयोर्वचनात् स्वयं सूत्रकारेण श्रुतशब्दप्रयोगाच्च । स हि श्रूयतेस्मेति श्रुतं प्रवचनमित्यस्येष्टार्थस्य संग्रहार्थः श्रेयो । नान्यथा स्पष्टज्ञानाभिधायिनः शब्दस्य प्रयोगार्हत्वात् ।
__यहां वह श्रुत तो शब्दमात्र है, यह उपचारसे समझना चाहिये । क्योंकि उस श्रुतके दो भेद हैं। तथा अनेक और बारह प्रभेद हैं । इस कथनकरके सूत्रकारने शद्वसम्बन्धी रचना विशेषके ही सम्भवनेवाले भेदप्रभेदोंका कथन किया है । तथा दूसरी बात यह है कि सूत्रग्रन्थ बनानेवाले श्री उमास्वामी महाराजने स्वयं श्रुतशद्वका प्रयोग किया है । अर्थात्-एक तो बात यह है कि अंगबाह्य, अंगप्रविष्ट या अनेक, बारह, ये मेद प्रभेद तो शब्दके ही हो सकते हैं। श्रुतबानमें तो शद्वद्वारा होते हुये ये भेदभेद भले ही माने गये हैं, मौलिक नहीं । दूसरी बात यह भी है कि सूत्रकारने श्रुत शद्बका प्रयोग किया है, जो कि " श्रुश्रवणे " धातुसे कर्ममें क प्रत्यय करनेपर बना, बडी सुलभतासे शदश्रुतको कहनेके लिये अभिमुख बैठा हुआ है। जो ( शब्द ) कर्ण इन्द्रिय द्वारा सुना जा चुका है, वह श्रुत अवश्य है । यो निर्वचन किया गया शद्वमय श्रुतप्रवचन ( शास्त्र ) है । इस प्रकारके इस इष्ट अर्थका संग्रह करनेके लिये वह श्रुत शद्वका प्रयोग करना श्रेष्ठ है । ज्ञान और शद्ध दोनोंमें प्रवर्तनेवाले श्रुतपदका प्रयोग करना अन्य प्रकारोंसे समुचित नहीं हो सकता है । यों यदि ज्ञान ही अर्थ सूत्रकारको बमीष्ट होता तो स्पष्ट रूपसे ज्ञानको कहनेवाले ज्ञान, प्रमाण, वेदन, श्रुतज्ञान, आदि पदोंका ही प्रयोग कर देना योग्य था। भाव और कर्ममें निष्ठा प्रत्यय कर बान और शब्द दोनोंको कहनेवाले श्रुतका प्रयोग करना उचित नहीं था, किन्तु प्रयोग किया है। कोरे द्वैविध्य या संशयके जनक पदोंके प्रयोगद्वारा क्लिष्ट कल्पना करते बैठना किसको अभीष्ट है ! अतः अर्थापत्तिसे सिद्ध हो जाता है कि मुख्यरूपसे श्रुतज्ञान और गौणरूपसे शब्द आत्मक श्रुत इष्ट है।