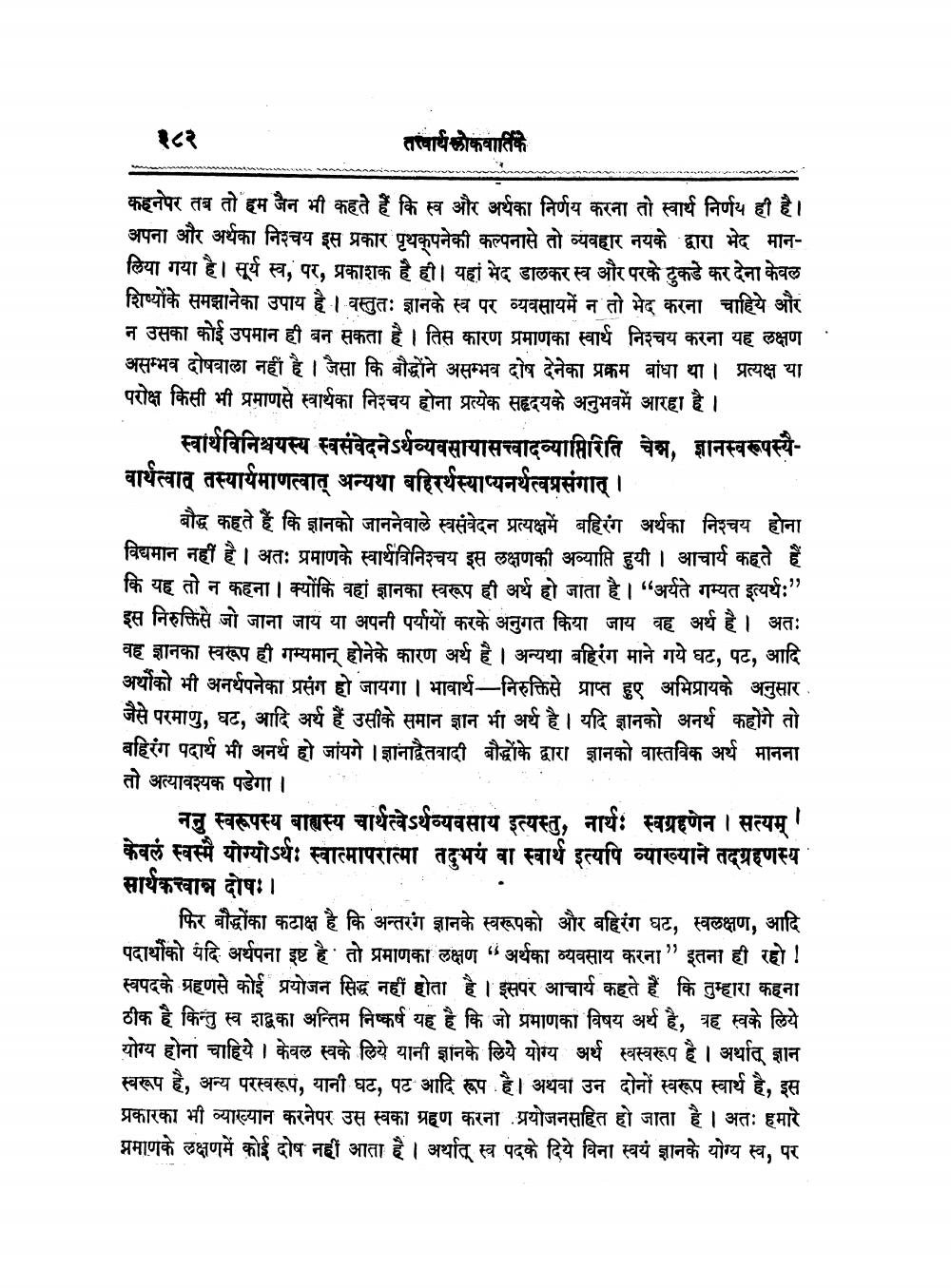________________
तत्वार्थ लोकवार्तिके
कपर तब तो हम जैन भी कहते हैं कि स्व और अर्थका निर्णय करना तो स्वार्थ निर्णय ही है। अपना और अर्थका निश्चय इस प्रकार पृथक्पनेकी कल्पनासे तो व्यवहार नयके द्वारा भेद मानलिया गया है। सूर्य स्व, पर, प्रकाशक है ही। यहां भेद डालकर स्व और परके टुकडे कर देना केवल शिष्यों के समझानेका उपाय है । वस्तुतः ज्ञानके स्व पर व्यवसायमें न तो भेद करना चाहिये और न उसका कोई उपमान ही बन सकता है । तिस कारण प्रमाणका स्वार्थ निश्चय करना यह लक्षण असम्भव दोषवाला नहीं है । जैसा कि बौद्धोंने असम्भव दोष देनेका प्रक्रम बांधा था । प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रमाणसे स्वार्थका निश्चय होना प्रत्येक सहृदय के अनुभवमें आरहा है ।
१८२
स्वार्थविनिश्चयस्य स्वसंवेदनेऽर्थव्यवसायासच्त्वादव्याप्तिरिति चेन्न, ज्ञानस्वरूपस्यैवार्थत्वात् तस्यार्यमाणत्वात् अन्यथा बहिरर्थस्याप्यनर्थत्वप्रसंगात् ।
बौद्ध कहते हैं कि ज्ञानको जाननेवाले स्वसंवेदन प्रत्यक्षमें बहिरंग अर्थका निश्चय होना विद्यमान नहीं है । अतः प्रमाणके स्वार्थविनिश्चय इस लक्षणकी अव्याप्ति हुयी । आचार्य कहते हैं। कि यह तो न कहना। क्योंकि वहां ज्ञानका स्वरूप ही अर्थ हो जाता है । “अर्यते गम्यत इत्यर्थः " इस निरुक्तिसे जो जाना जाय या अपनी पर्यायों करके अनुगत किया जाय वह अर्थ है । अतः वह ज्ञानका स्वरूप ही गम्यमान् होनेके कारण अर्थ है । अन्यथा बहिरंग माने गये घट, पट, आदि अर्थीको भी अनर्थपनेका प्रसंग हो जायगा । भावार्थ — निरुक्तिसे प्राप्त हुए अभिप्रायके अनुसार . जैसे परमाणु, घट, आदि अर्थ हैं उसीके समान ज्ञान भी अर्थ है । यदि ज्ञानको अनर्थ कहोंगे तो बहिरंग पदार्थ भी अनर्थ हो जायगे । ज्ञानाद्वैतवादी बौद्धोंके द्वारा ज्ञानको वास्तविक अर्थ मानना तो अत्यावश्यक पडेगा ।
ननु स्वरूपस्य बाह्यस्य चार्थत्वेऽर्थव्यवसाय इत्यस्तु, नार्यः स्वग्रहणेन । सत्यम् 1 केवलं स्वस्मै योग्योऽर्थः स्वात्मापरात्मा तदुभयं वा स्वार्थ इत्यपि व्याख्याने तद्ग्रहणस्य सार्थकत्त्वान्न दोषः ।
फिर बौद्धोंका कटाक्ष है कि अन्तरंग ज्ञानके स्वरूपको और बहिरंग घट, स्वलक्षण, आदि पदार्थोंको यदि अर्थपना इष्ट है तो प्रमाणका लक्षण " अर्थका व्यवसाय करना" इतना ही रहो ! स्वपद ग्रहणसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । इसपर आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु स्व शका अन्तिम निष्कर्ष यह है कि जो प्रमाणका विषय अर्थ है, वह स्वके लिये योग्य होना चाहिये । केवल स्वके लिये यानी ज्ञानके लिये योग्य अर्थ स्वस्वरूप है । अर्थात् ज्ञान स्वरूप है, अन्य परस्वरूपं, यानी घट, पट आदि रूप है । अथवा उन दोनों स्वरूप स्वार्थ है, इस प्रकारका भी व्याख्यान करनेपर उस स्वका ग्रहण करना प्रयोजनसहित हो जाता है । अतः हमारे प्रमाणके लक्षण में कोई दोष नहीं आता है । अर्थात् स्व पदके दिये विना स्वयं ज्ञानके योग्य स्व, पर