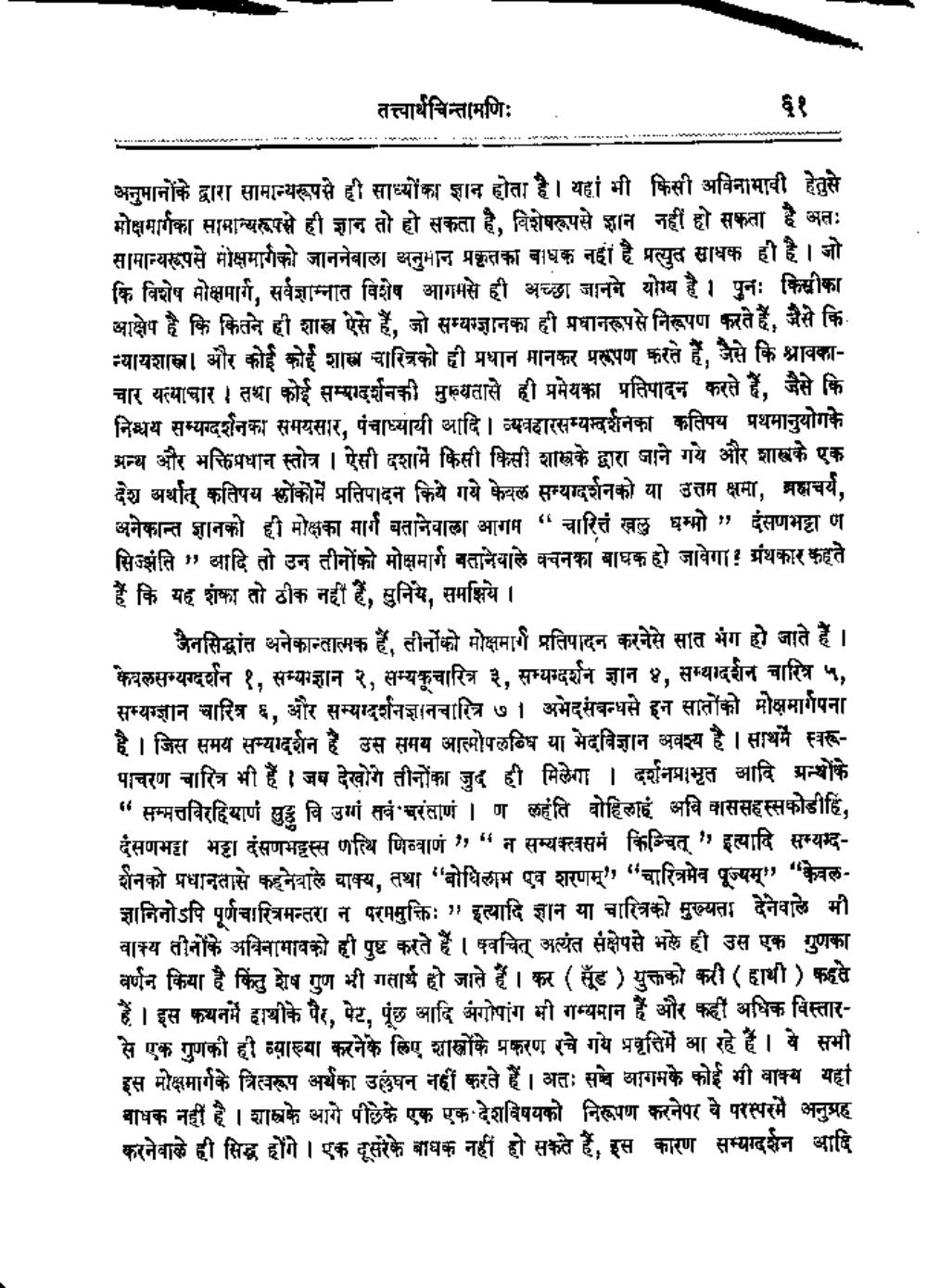________________
तत्त्वार्थचिन्तामणिः
६१
I
अनुमानोंके द्वारा सामान्यरूपसे ही साध्यों का ज्ञान होता है। यहां भी किसी अविनाभावी हेतुसे मोक्षमार्गका सामान्यरूपसे ही ज्ञान तो हो सकता है, विशेषरूप से ज्ञान नहीं हो सकता है अतः सामान्यरूपसे मोक्षमार्गको जाननेवाला अनुमान प्रकृतका बाधक नहीं है प्रत्युत साधक ही है । जो कि विशेष मोक्षमार्ग, सर्वज्ञाम्नात विशेष आगमसे ही अच्छा जानने योग्य है । पुनः किखीका आक्षेप है कि कितने ही शास्त्र ऐसे हैं, जो सम्यग्ज्ञानका ही प्रधानरूप से निरूपण करते हैं, जैसे कि. न्यायशास्त्र | और कोई कोई शास्त्र चारित्रको ही प्रधान मानकर प्ररूपण करते हैं, जैसे कि श्रावकाचार यत्याचार | तथा कोई सम्यग्दर्शनकी मुख्यतासे ही प्रमेयका प्रतिपादन करते हैं, जैसे कि निश्चय सम्यग्दर्शन का समयसार, पंचाध्यायी आदि । व्यवहारसम्यग्दर्शनका कतिपय प्रथमानुयोगके अन्य और भक्तिप्रधान स्तोत्र । ऐसी दशा में किसी किसी शास्त्रके द्वारा जाने गये और शास्त्र के एक देश अर्थात् कतिपय लोक में प्रतिपादन किये गये केवल सम्यग्दर्शन को या उत्तम क्षमा, ब्रह्मचर्य, अनेकान्त ज्ञानको ही मोक्षका मार्ग बतानेवाला आगम " चारितं खलु धम्मो " दंसणभट्टा ण सिज्यंति " बादि तो उन तीनोंको मोक्षमार्ग बतानेवाले वचनका बाधक हो जावेगा ! ग्रंथकार कहते हैं कि यह शंका तो ठीक नहीं हैं, सुनिये, समझिये ।
I
जैन सिद्धांत अनेकान्तात्मक हैं, तीनोंको मोक्षमार्ग प्रतिपादन करनेसे सात भंग हो जाते हैं । केवल सम्यग्दर्शन १, सम्यग्ज्ञान २, सम्यकूचारित्र ३, सम्यग्दर्शन ज्ञान ४, सम्यग्दर्शन चरित्र ५, सम्यग्ज्ञान चारित्र ६, और सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ७ । अभेद संबन्धसे इन सातोंको मोक्षमार्गपना है । जिस समय सम्यग्दर्शन है उस समय आत्मोपलब्धि या भेदविज्ञान अवश्य है । साथमै स्वरूपाचरण चारित्र भी हैं । जब देखोगे तीनोंका जुद ही मिलेगा । दर्शनप्राभृत आदि ग्रन्थोंके " सम्मत्तविरहियाणं हु वि उग्गं सर्व चरंताणं । ण लहंति वोहिलाई अचि वाससह स्सकोडीहिं, दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं " " न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् " इत्यादि सम्यग्दर्शनको प्रधानता कहनेवाले वाक्य, तथा "बोधिलाम एव शरणम्" "चारित्रमेव पूज्यम्” “केवलज्ञानिनोऽपि पूर्णचारित्रमन्तरा न परममुक्तिः " इत्यादि ज्ञान या चारित्रको मुख्यता देनेवाले मी वाक्य तीनों अविनाभावको ही पुष्ट करते हैं । ध्वचित् अत्यंत संक्षेप से भले ही उस एक गुणका वर्णन किया है किंतु शेष गुण भी गतार्थ हो जाते हैं। कर ( सूँड) युक्तको करी ( हाथी ) कहते हैं । इस कथनमें हाथी के पैर, पेट, पूंछ आदि अंगोपांग भी गम्यमान हैं और कहीं अधिक विस्तारसे एक गुणकी ही व्याख्या करनेके लिए शास्त्रोंके प्रकरण रचे गये प्रवृत्ति में आ रहे हैं। ये सभी इस मोक्षमार्ग के त्रिवरूप अर्थका उल्लंघन नहीं करते हैं । अतः स आगमके कोई भी वाक्य यहां बाधक नहीं है । शास्त्र आगे पीछेके एक एक देशविषयको निरूपण करनेपर वे परस्पर में अनुग्रह करनेवाले ही सिद्ध होंगे। एक दूसरेके बाधक नहीं हो सकते हैं, इस कारण सम्यग्दर्शन आदि