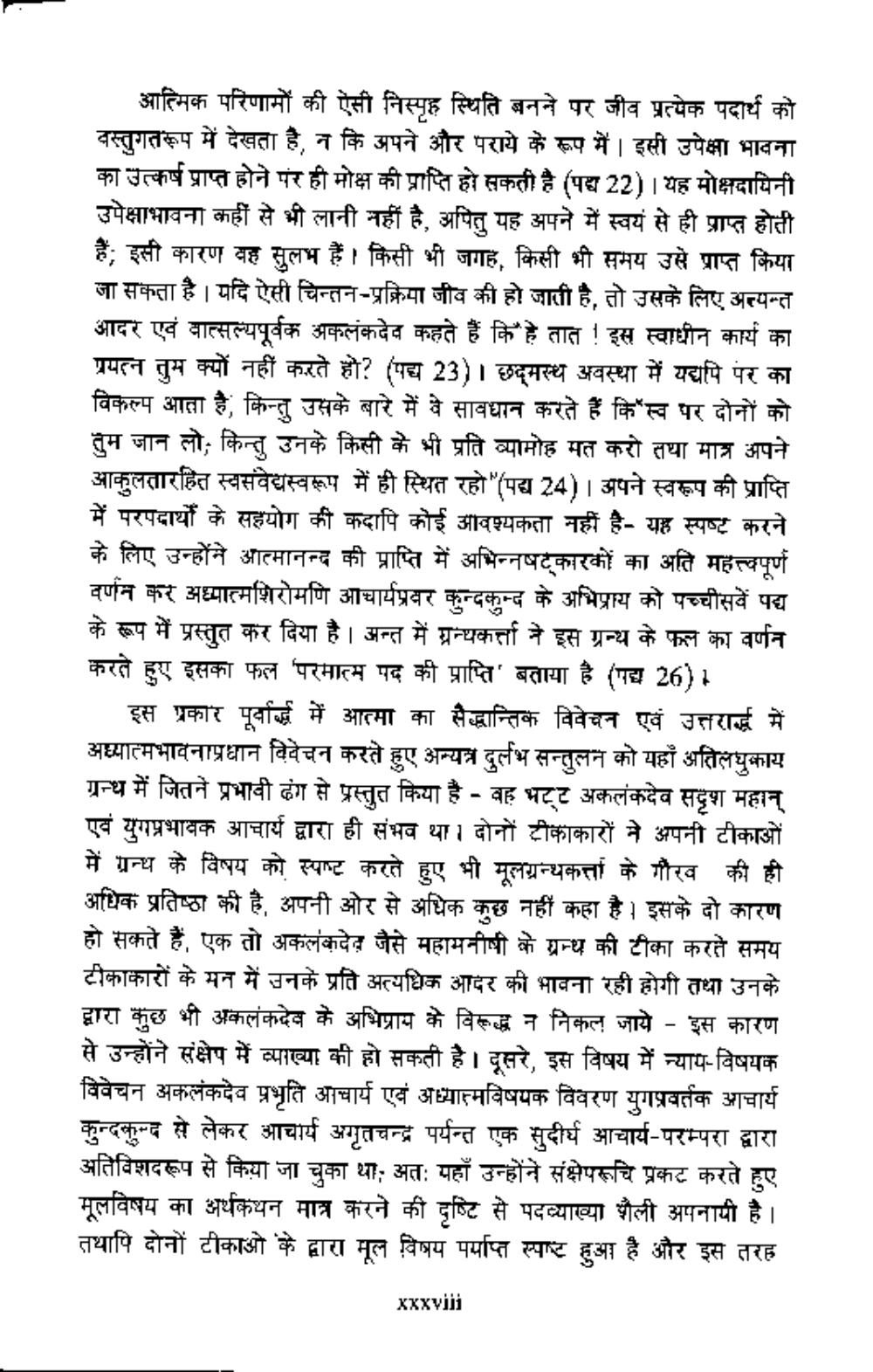________________
आत्मिक परिणामों की ऐसी निस्पृह स्थिति बनने पर जीव प्रत्येक पदार्थ को वस्तुगतरूप में देखता है, न कि अपने और पराये के रूप में । इसी उपेक्षा भावना का उत्कर्ष प्राप्त होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है (पद्य 22)। यह मोक्षदायिनी उपेक्षाभावना कहीं से भी लानी नहीं है, अपितु यह अपने में स्वयं से ही प्राप्त होती हैं; इसी कारण वह सुलभ हैं। किसी भी जगह, किसी भी समय उसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया जीव की हो जाती है, तो उसके लिए अत्यन्त आदर एवं वात्सल्यपूर्वक अकलंकदेव कहते हैं कि हे तात ! इस स्वाधीन कार्य का प्रयत्न तुम क्यों नहीं करते हो? (पद्य 23)। छद्मस्थ अवस्था में यद्यपि पर का विकल्प आता है, किन्तु उसके बारे में वे सावधान करते हैं कि स्व पर दोनों को तुम जान लो; किन्तु उनके किसी के भी प्रति व्यामोह मत करो तथा मात्र अपने आकुलतारहित स्वसंवेद्यस्वरूप में ही स्थित रहो"(पद्य 24)। अपने स्वरूप की प्राप्ति में परपदार्थों के सहयोग की कदापि कोई आवश्यकता नहीं है- यह स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आत्मानन्द की प्राप्ति में अभिन्नषट्कारकों का अति महत्त्वपूर्ण वर्णन कर अध्यात्मशिरोमणि आचार्यप्रवर कुन्दकुन्द के अभिप्राय को पच्चीसवें पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अन्त में ग्रन्थकर्ता ने इस ग्रन्थ के फल का वर्णन करते हुए इसका फल ‘परमात्म पद की प्राप्ति' बताया है (पद्य 26)1
इस प्रकार पूर्वार्द्ध में आत्मा का सैद्धान्तिक विवेचन एवं उत्तरार्द्ध में अध्यात्मभावनाप्रधान विवेचन करते हुए अन्यत्र दुर्लभ सन्तुलन को यहाँ अतिलघुकाय ग्रन्थ में जितने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है - वह भट्ट अकलंकदेव सदृश महान् एवं युगप्रभावक आचार्य द्वारा ही संभव था। दोनों टीकाकारों ने अपनी टीकाओं में ग्रन्ध के विषय को स्पष्ट करते हुए भी मूलग्रन्धकता के गौरव की ही अधिक प्रतिष्ठा की है, अपनी ओर से अधिक कुछ नहीं कहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो अकलंकदेव जैसे महामनीषी के ग्रन्ध की टीका करते समय टीकाकारों के मन में उनके प्रति अत्यधिक आदर की भावना रही होगी तथा उनके द्वारा कुछ भी अकलंकदेव के अभिप्राय के विरूद्ध न निकल जाये - 'इस कारण से उन्होंने संक्षेप में व्याख्या की हो सकती है। दूसरे, इस विषय में न्याय-विषयक विवेचन अकलंकदेव प्रभृति आचार्य एवं अध्यात्मविषयक विवरण युगप्रवर्तक आचार्य कुन्दकुन्द से लेकर आचार्य अमृतचन्द्र पर्यन्त एक सुदीर्घ आचार्य-परम्परा द्वारा अतिविशदरूप से किया जा चुका था, अत: यहाँ उन्होंने संक्षेपरूचि प्रकट करते हुए मूलविषय का अर्थकथन मात्र करने की दृष्टि से पदव्याख्या शैली अपनायी है। तथापि दोनों टीकाओ के द्वारा मूल विषय पर्याप्त स्पाट हुआ है और इस तरह
xxxviii