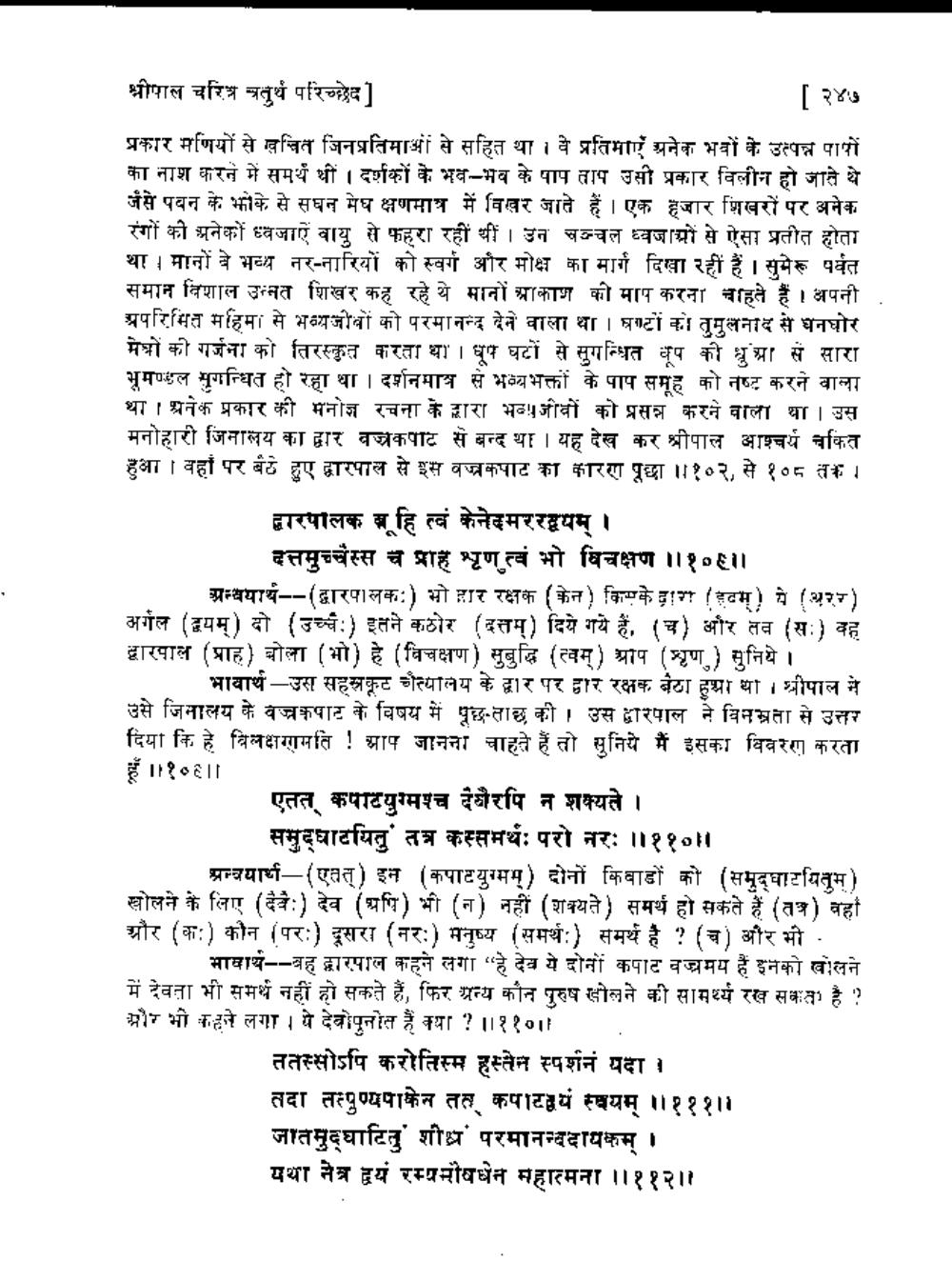________________
श्रीपाल चरित्र चतुर्थ परिच्छेद ]
[ २४७
प्रकार मणियों से खन्वित जिनप्रतिमाओं से सहित था । वे प्रतिमाएँ अनेक भवों के उत्पन्न पापों का नाश करने में समर्थ थीं। दर्शकों के भव-भव के पाप ताप उसी प्रकार विलीन हो जाते थे जैसे पवन के झोंके से सघन मेघ क्षणमात्र में विखर जाते हैं। एक हजार शिखरों पर अनेक रंगों की अनेकों ध्वजाऐं वायु से फहरा रहीं थीं । उन चञ्चल ध्वजाओं से ऐसा प्रतीत होता था। मानों वे भव्य नर-नारियों को स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखा रहीं हैं । सुमेरू पर्वत समान विशाल उन्नत शिखर कह रहे थे मानों आकाश की माप करना चाहते हैं | अपनी अपरिमित महिमा से भव्यजीवों को परमानन्द देने वाला था। घण्टों को तुमुलनाद से घनघोर मैत्रों की गर्जना को तिरस्कृत करता था । धूप घटों से सुगन्धित खूप की धुंआ से सारा भूमण्डल सुगन्धित हो रहा था । दर्शनमात्र से भव्यभक्तों के पाप समूह को नष्ट करने वाला था । श्रनेक प्रकार की मनोज्ञ रचना के द्वारा भव्यजीवों को प्रसन्न करने वाला था । उस मनोहारी जिनालय का द्वार वज्रकपाट से बन्द था । यह देख कर श्रीपाल आश्चर्य चकित हुआ। वहाँ पर बैठे हुए द्वारपाल से इस वज्रकपाट का कारण पूछा ।। १०२ से १०८ तक /
द्वारपालक ब्रूहि त्वं केनेदमररद्वयम् ।
दत्तमुच्चैस्स च प्राह शृणुत्वं भो विचक्षण ।। १०६ ॥
अन्वयार्थ - - ( द्वारपालक: ) भो हार रक्षक (क्रेन) किसके द्वारा ( हदम्) ये ( अरर) अर्गल ( द्वयम् ) दो (उच्च) इतने कठोर ( दत्तम् ) दिये गये हैं, (च) और तब ( स ) वह द्वारपाल ( प्राह ) बोला ( भो ) हे ( विचक्षण) सुबुद्धि ( त्वम् ) श्राप ( श्रृण) सुनिये ।
भावार्थ – उस सहस्रकूट चैत्यालय के द्वार पर द्वार रक्षक बैठा हुआ था । श्रीपाल ने उसे जिनालय के वज्रकपाट के विषय में पूछ-ताछ की। उस द्वारपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे विलक्षमति ! आप जानना चाहते हैं तो सुनिये मैं इसका विवरण करता हूँ ।। १०६ ।।
एतत् कपाटयुग्मश्च देवैरपि न शक्यते ।
समुद्घाटयितु तत्र कस्समर्थः परो नरः ॥ ११०॥
श्रन्वयार्थ - ( एतत् ) इन ( कपाटयुग्मम् ) दोनों किवाडों को ( समुद्घाटयितुम् ) खोलने के लिए (देवैः ) देव (अपि) भी (न) नहीं ( शक्यते ) समर्थ हो सकते हैं (तत्र ) वहाँ और (क: ) कौन ( पर: ) दूसरा ( नरः ) मनुष्य ( समर्थ : ) समर्थ है ? (च) और भी भावार्थ - - वह द्वारपाल कहने लगा "हे देव ये दोनों कपाट वज्रमय हैं इनको खोलने में देवता भी समर्थ नहीं हो सकते हैं, फिर ग्रन्य कौन पुरुष खोलने की सामर्थ्य रख सकता है ? और भी कहने लगा। ये देवोपुनोत हैं क्या ? ॥ ११०॥
ततस्सोऽपि करोतिस्म हस्तेन स्पर्शनं यदा ।
तदा तत्पुण्यपान तत् कपाद्वयं स्वयम् ॥ १११ ॥ जातमुद्घाटितुं शीघ्र परमानन्ददायकम् । यथा नेत्र द्वयं रम्यनौषधेन महात्मना ।। ११२॥