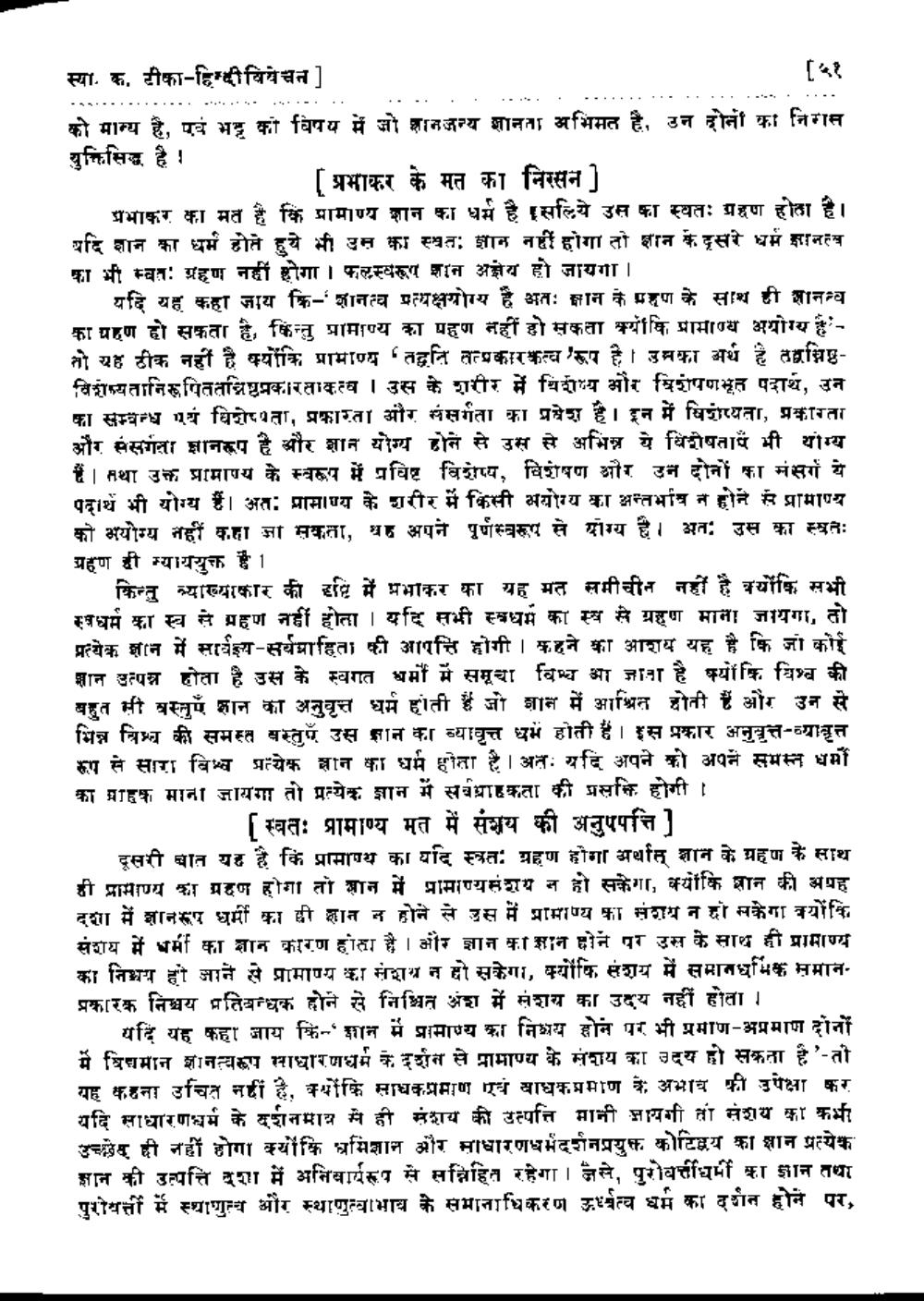________________
स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचन ]
[ ५१
को मान्य है, एवं भट्ट की विषय में जो शानजन्य ज्ञानता अभिमत है, उन दोनों का निगस युक्तिसिद्ध है ।
[ प्रभाकर के मत का निरसन ]
प्रभाकर का मत है कि प्रामाण्य ज्ञान का धर्म है इसलिये उस का स्वतः ग्रहण होता है । यदि ज्ञान का धर्म होते हुये भी उस का स्वतः ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान के दूसरे धर्म ज्ञानव का भी स्वतः ग्रहण नहीं होगा । फलस्वरूप ज्ञान अज्ञेय हो जायगा ।
यदि यह कहा जाय कि ज्ञानत्व प्रत्यक्षयोग्य है अतः ज्ञान के प्रण के साथ ही ज्ञानन्व का ग्रहण हो सकता है, किन्तु प्रामाण्य का पहण नहीं हो सकता क्योंकि प्रामाण्य अयोग्य हैं:तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रामाण्य 'तद्वति तत्प्रकारकत्व रूप है। उसका अर्थ है निष्ठ विशेष्यतानिरूपिततन्निष्टप्रकारताकत्व । उस के शरीर में विशेष्य और विशेषणभूत पदार्थ, उन का सम्बन्ध एवं विशेष्यता, प्रकारता और संसर्गता का प्रवेश है। इन में विशेष्यता, प्रकारता और संसगंता ज्ञानरूप है और ज्ञान योग्य होने से उस से अभिन्न ये विशेषताएँ भी योग्य हैं | तथा उक्त प्रामाण्य के स्वरूप में प्रविष्ट विशेष्य, विशेषण और उन दोनों का संसर्ग ये पदार्थ भी योग्य हैं। अतः प्रामाण्य के शरीर में किसी अयोग्य का अन्तर्भाव न होने से प्रामाण्य को अयोग्य नहीं कहा जा सकता, वह अपने पूर्णस्वरूप से योग्य है । अत: उस का स्वतः ग्रहण ही न्याययुक्त है 1
किन्तु व्याख्याकार की दृष्टि में प्रभाकर का यह मत समीचीन नहीं क्योंकि सभी स्वधर्म का स्व से ग्रहण नहीं होता । यदि सभी स्वधर्म का स्त्र से ग्रहण माना जायगा, तो प्रत्येक ज्ञान में साक्ष्य सर्वप्राहिता की आपत्ति होगी। कहने का आशय यह है कि जो कोई ज्ञान उत्पन्न होता है उस के स्वगत धर्मों में समूचा विश्व आ जाता है क्योंकि विश्व की बहुत भी वस्तुएँ ज्ञान का अनुवृत्त धर्म होती है जो ज्ञान में आश्रित होती हैं और उन से भिन्न विश्व की समस्त वस्तुएँ उस ज्ञान का व्यावृत्त धर्म होती हैं। इस प्रकार अनुवृत्त-व्यावृत्त रूप से सारा विश्व प्रत्येक ज्ञान का धर्म होता है। अतः यदि अपने को अपने समस्त धर्मों का ग्राहक माना जायगा तो प्रत्येक ज्ञान में सर्वग्राहकता की प्रति होगी ।
[ स्वतः प्रामाण्य मत में संशय की अनुपपत्ति ]
के साथ
दूसरी बात यह है किं प्रामाण्य का यदि स्वतः ग्रहण होगा अर्थात् ज्ञान के ग्रहण ही प्रामाण्य का ग्रहण होगा तो ज्ञान में प्रामाण्यसंशय न हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान की अग्रह दशा में ज्ञानरूप धर्मी का ही ज्ञान न होने से उस में प्रामाण्य का संशय न हो सकेगा क्योंकि संशय में धर्म का ज्ञान कारण होता है और ज्ञान का ज्ञान होने पर उस के साथ ही प्रामाण्य का निश्रय हो जाने से प्रामाण्य का संशय न हो सकेगा, क्योंकि संशय में समानधर्मिक समानप्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक होने से निश्चित अंश में संशय का उदय नहीं होता ।
यदि यह कहा जाय कि-' ज्ञान में प्रामाण्य का निश्रय होने पर भी प्रमाण अप्रमाण दोनों में विद्यमान ज्ञानत्वरूप साधारणधर्म के दर्शन से प्रामाण्य के संशय का उदय हो सकता है' - ती यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि साधकप्रमाण एवं बाधकप्रमाण के अभाव की उपेक्षा कर यदि साधारणधर्म के दर्शनमात्र से ही संशय की उत्पत्ति मानी जायगी ती संशय का कभी उच्छेष ही नहीं होगा क्योंकि प्रमिशान और साधारणधर्मदर्शनप्रयुक्त कोटिइय का ज्ञान प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्ति दशा में अनिवार्यरूप से सन्निहित रहेगा। जैसे, पुरोवर्त्तिधर्मी का ज्ञान तथा पुरोयर्ती में स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव के समानाधिकरण ऊर्ध्वत्व धर्म का दर्शन होने पर,