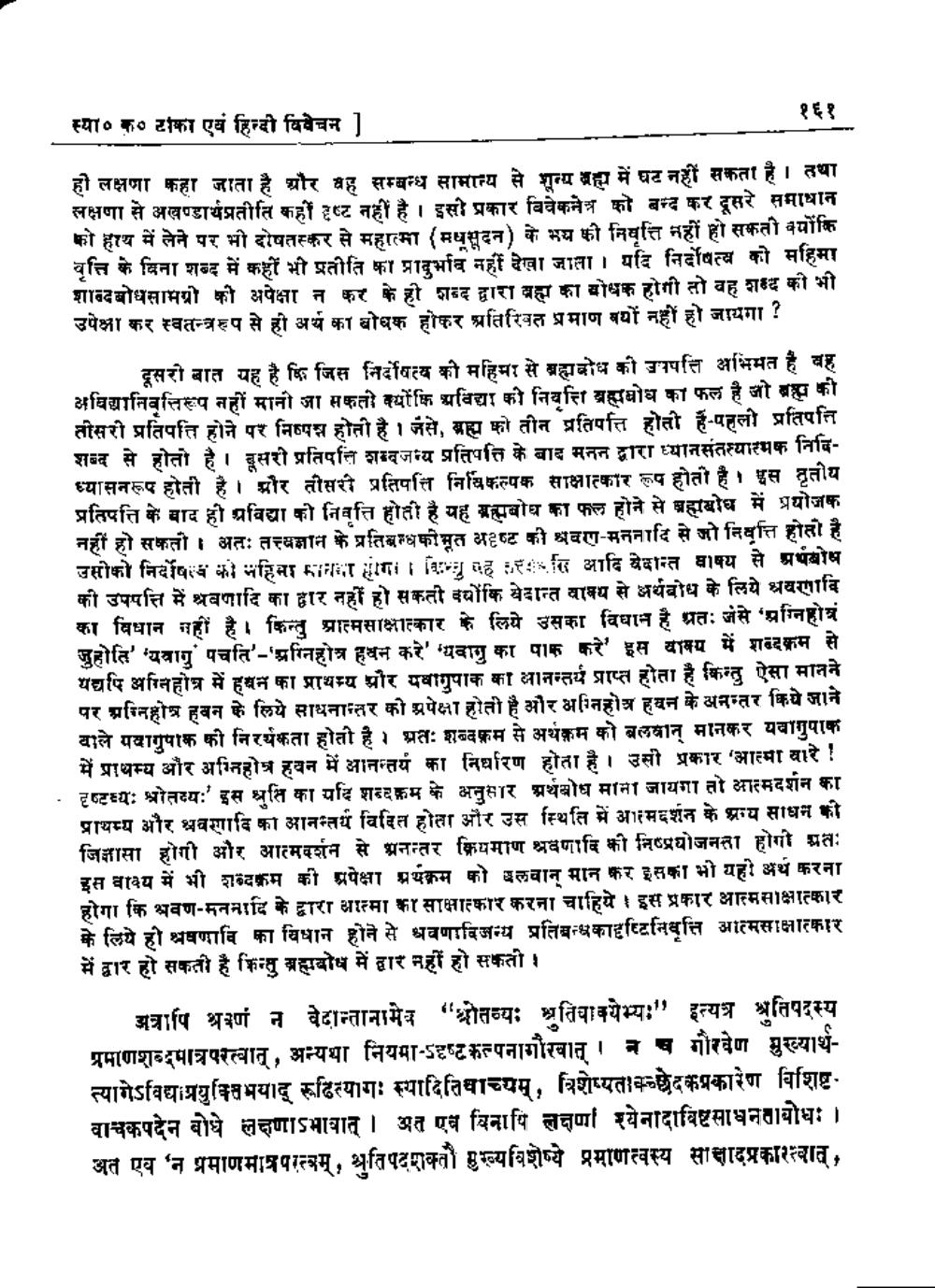________________
स्याक० टका एवं हिन्दी विवेचन ]
हो लक्षणा कहा जाता है और वह सम्बन्ध सामान्य से शून्य ब्रह्म में घट नहीं सकता है । तथा लक्षणा से अखण्डार्थप्रतीति कहीं इष्ट नहीं है। इसी प्रकार विवेकनेत्र को बन्द कर दूसरे समाधान को हाथ में लेने पर भी दोषतस्कर से महात्मा (मधुसूदन) के भय की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वृत्ति के विना शब्द में कहीं भी प्रतीति का प्रादुर्भाव नहीं देखा जाता। यदि निर्दोषत्व को महिमा शाब्दबोधसामग्री की अपेक्षा न कर के ही शब्द द्वारा ब्रह्म का बोधक होगी तो वह शब्द की भी उपेक्षा कर स्वतन्त्ररूप से ही अर्थ का बोधक होकर अतिरिक्त प्रमाण क्यों नहीं हो जायगा ?
दूसरी बात यह है कि जिस निर्दोषत्व को महिमा से ब्रह्मबोध की उत्पत्ति अभिमत है वह अविद्यानिवृत्तिरूप नहीं मानी जा सकती क्योंकि अविद्या को नियत्ति ब्रह्मबोध का फल है जो ब्रह्म की तीसरी प्रतिपत्ति होने पर निष्पन्न होती है । जैसे, ब्रह्म को तीन प्रतिपत्ति होती है-पहली प्रतिपत्ति शब्द से होती है। दूसरी प्रतिपत्ति शम्दजन्य प्रतिपत्ति के बाद मनन द्वारा ध्यानसंतत्यारमक निविध्यासनरूप होती है। और तीसरी प्रतिपत्ति निर्विकल्पक साक्षात्कार रूप होती है। इस तृतीय प्रतिपत्ति के बाद ही विद्या को निवृत्ति होती है यह ब्रह्मबोध का फल होने से बहाबोध में प्रयोजक नहीं हो सकती। अतः तत्त्वज्ञान के प्रतिबन्धको भूत अष्ट की श्रवण-मननादि से जो निवृत्ति होती है उसोको निर्दोषाव को महिमा मापागा। विमुपह
इस आदि वेदान्त पाषय से अर्थबोष की उपपत्ति में श्रवणादि का द्वार नहीं हो सकती क्योंकि वेदान्त वाक्य से अर्थबोध के लिये श्रवणादि का विधान नहीं है। किन्तु प्रात्मसाक्षात्कार के लिये उसका विधान है अतः जैसे 'अग्निहोत्रं जुहोति' 'यवाणु पचति'-'अग्निहोत्र हवन करे' यवागु का पाफ करे' इस वाक्य में शब्दक्रम से यद्यपि अग्निहोत्र में हवन का प्राथम्य और यवागुपाक का आनन्तर्य प्राप्त होता है किन्तु ऐसा मानने पर अग्निहोत्र हवन के लिये साधनान्तर को अपेक्षा होती है और अग्निहोत्र हवन के अनन्तर किये जाने वाले यवागुपाक की निरर्थकता होती है। अतः शब्दक्रम से अर्थक्रम को बलवान् मानकर यवागुपाक में प्राथम्य और अग्निहोत्र हवन में आनन्तयं का निर्धारण होता है। उसी प्रकार 'आत्मा वारे ! दृष्टव्यः श्रोतव्यः' इस श्रुति का यदि शब्दकम के अनुसार अर्थबोध माना जायगा तो आत्मदर्शन का प्राथम्य और श्रवणादि का आनन्तर्य विदित होता और उस स्थिति में आत्मदर्शन के अन्य साधन की जिज्ञासा होगी और आत्मदर्शन से अनन्तर क्रियमाण श्रवणादि की निष्प्रयोजनता होगी प्रतः इस वाक्य में भी शब्दक्रम की अपेक्षा प्रयक्रम को बलवान मान कर इसका भी यही अर्थ करना होगा कि श्रवण-मनमादि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिये। इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार के लिये हो श्रषणादि का विधान होने से श्रवणादिजन्य प्रतिबन्धकादृष्टिनिवृत्ति आत्मसाक्षात्कार में द्वार हो सकती है किन्तु ब्रह्मबोध में द्वार नहीं हो सकती।
अत्रापि श्रवणं न वेदान्तानामेव "श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः" इत्यत्र श्रुतिपदस्य प्रमाणशब्दपात्रपरत्वात् , अन्यथा नियमा-ऽदृष्ट कल्पनागौरवात् । न ष गौरवेण मुख्यार्थत्यागेऽविद्याप्रयुक्तिभयाद् रूढित्यागः स्यादितिधाच्यम् , विशेष्यतावच्छेदकप्रकारेण विशिष्ट. वाचकपदेन बोधे लक्षणाऽभावात् । अत एवं विनायि लक्षणां श्येनादाविष्टसाधनतायोधः । अत एव 'न प्रमाणमात्रपरत्वम् , श्रुतिपदशक्तो मुख्य विशेष्ये प्रमाणत्वस्य साक्षादप्रकारस्वात,