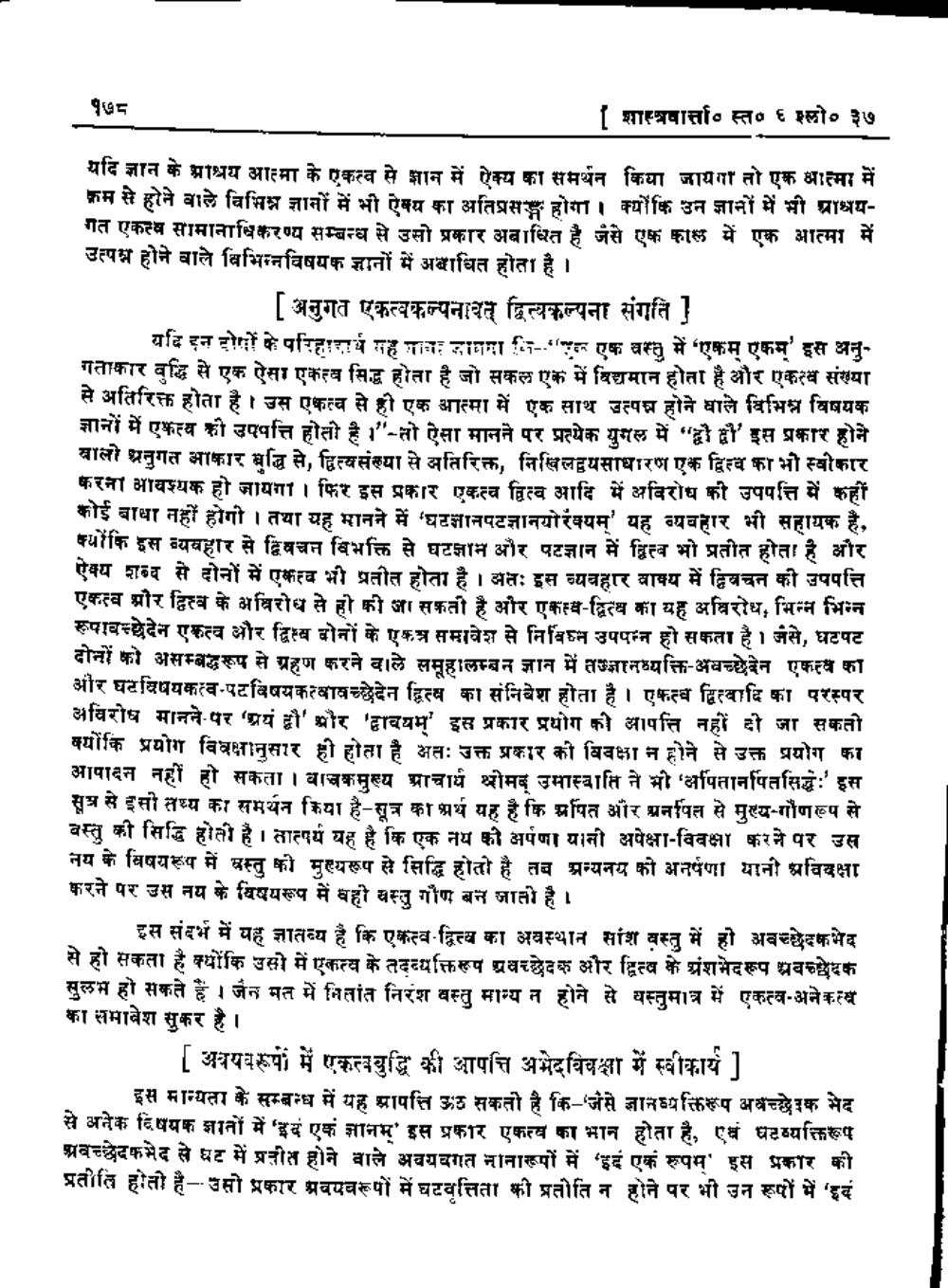________________
१७८
[ शास्त्रवा०ि स्त० ६ श्लो० ३७
यदि ज्ञान के प्राश्रय आत्मा के एकत्व से ज्ञान में ऐक्य का समर्थन किया जायगा तो एक आत्मा में क्रम से होने वाले विभिन्न ज्ञानों में भी ऐक्य का अतिप्रसङ्ग होगा। क्योंकि उन ज्ञानों में भी प्राधयगत एकत्व सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से उसी प्रकार अबाधित है जैसे एक काल में एक आत्मा में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विषयक ज्ञानों में अबाधित होता है ।
[अनुगत एकत्वकल्पनावत् द्वित्यकल्पना संगति ] यदि इन दोनों के परिहार्य सह माना जाममा नि एक वस्तु में 'एकम् एकम्' इस अनुगताकार बुद्धि से एक ऐसा एकत्व सिद्ध होता है जो सकल एक में विद्यमान होता है और एकत्व संख्या से अतिरिक्त होता है । उस एकत्व से ही एक आत्मा में एक साथ उत्पन्न होने वाले विभिन्न विषयक ज्ञानों में एकत्व को उपपत्ति होती है।"-तो ऐसा मानने पर प्रत्येक युगल में "द्वौ द्वौ' इस प्रकार होने बालो अनुगत आकार वि से, द्वित्वसंख्या से अतिरिक्त, निखिलद्यसाधारण एक द्विस्वक करना आवश्यक हो जायगा । फिर इस प्रकार एकत्व नित्व आदि में अविरोध की उपपत्ति में कहीं कोई बाधा नहीं होगी। तथा यह मानने में 'घटज्ञानपटज्ञानयोरक्यम्' यह व्यवहार भी सहायक है, क्योंकि इस व्यवहार से द्विवचन विभक्ति से घटज्ञान और पटज्ञान में द्वित्व भो प्रतीत होता है और ऐक्य शब्ध से दोनों में एकत्व भी प्रतीत होता है । अतः इस व्यवहार वाक्य में द्विवचन की उपपत्ति एकत्व और द्विस्व के अविरोध से हो की जा सकती है और एकस्व-द्वित्व का यह अविरोध, भिन्न भिन्न रूपावच्छेदेन एकत्व और द्वित्व दोनों के एकत्र समावेश से निर्विघ्न उपपन्न हो सकता है । जैसे, घटपट दोनों को असम्बद्धरूप से ग्रहण करने वाले समूहालम्बन ज्ञान में तज्ज्ञानव्यक्ति-अवच्छेवेन एकत्व का और घटविषयकस्व-पटविषयकत्वावच्छेदेन द्वित्व का संनिवेश होता है। एकत्व द्वित्वादि का परस्पर अविरोध मानने पर 'प्रयं द्वौ' और 'हावयम्' इस प्रकार प्रयोग को आपत्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रयोग विवक्षानसार ही होता है अतः उक्त प्रकार की विवक्षा न होने से उक्त प्रयोग का आपादन नहीं हो सकता। वाचकमुख्य प्राचार्य श्रीमद् उमास्वाति ने सूत्र से इसी तथ्य का समर्थन किया है-सूत्र का अर्थ यह है कि प्रपित और अनपिल से मुख्य-गौणरूप से वस्तु की सिद्धि होती है । तात्पर्य यह है कि एक नय को अर्पणा यानी अपेक्षा-विवक्षा करने पर उस नय के विषयरूप में वस्तु को मुख्यरूप से सिद्धि होती है तब अन्यनय को अनर्पणा यानी अविवक्षा करने पर उस नय के विषयरूप में वही यस्तु गौण बन जाती है।
इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि एकत्व-द्वित्व का अवस्थान सांश वस्तु में हो अवच्छेदक भेद से हो सकता है क्योंकि उसो में एकत्व के तदव्यक्तिरूप प्रवच्छेदक और द्वित्व के अंशभेदरूप अवच्छेदक सुलभ हो सकते हैं । जैन मत्त में नितांत निरंश वस्तु मान्य न होने से वस्तुमात्र में एकत्व-अनेकत्व का समावेश सुकर है।
[अवयवरूपों में एकत्वबुद्धि की आपत्ति अभेदविवक्षा में स्वीकार्य ] ___ इस मान्यता के सम्बन्ध में यह प्रापत्ति उसकती है कि-'जैसे जानध्याक्तिरूप अवच्छेदक भेद से अनेक विषयक झानों में 'इदं एक ज्ञानम' इस प्रकार एकत्व का भान होता है, एवं घट व्यक्तिरूप अवच्छेदकभेद से घट में प्रतीत होने वाले अवयवगत नानारूपों में 'इदं एक रुपम्' इस प्रकार की प्रतालि होती है-उसो प्रकार अवयवरूपों में घटवत्तिता की प्रतीति न होने पर भी उन रूपों में 'इदं