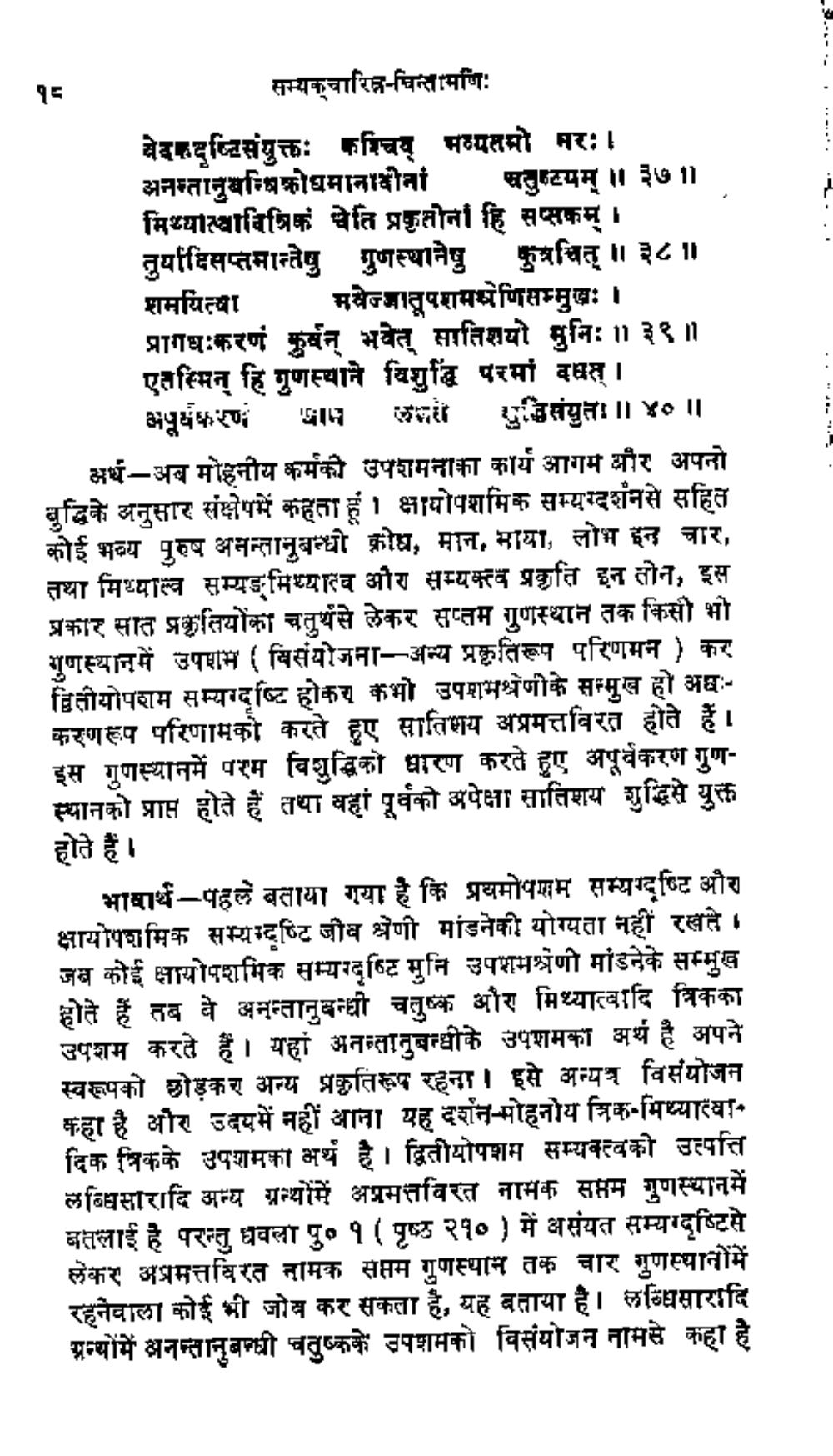________________
१८
सम्यक्चारित्र-चिन्तामणिः
वेदक दृष्टिसंयुक्तः कश्चित् भव्यतम्रो मरः । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानादीनां चतुष्टयम् ॥ ३७ ॥ मिथ्यात्वावित्रिकं चेति प्रकृतीनां हि सप्तकम् । तुर्यादिसप्तमान्तेषु गुणस्थानेषु कुत्रचित् ॥ ३८ ॥ शमयित्वा मवेज्जातू पशमधे णिसम्मुखः । प्रागधःकरणं कुर्वन् भवेत् सातिशयो मुनिः ॥ ३९ ॥ एतस्मिन् हि गुणस्याने विशुद्धि परमां दधत् । अपूर्वकरण प्राम Geit सुद्धिसंयुक्तः ।। ४० ।।
अर्थ - अब मोहनीय कर्मको उपशमनाका कार्य आगम और अपनो बुद्धिके अनुसार संक्षेपमें कहता हूं । क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन से सहित कोई भव्य पुरुष अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार तथा मिथ्यात्व सम्यङ् मिध्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन तीन, इस प्रकार सात प्रकृतियोंका चतुर्थसे लेकर सप्तम गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में उपशम (विसंयोजना- अन्य प्रकृतिरूप परिणमन ) कर द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि होकर कभी उपशमश्रेणी के सम्मुख हो अधःकरणरूप परिणामको करते हुए सातिशय अप्रमत्तविरत होते हैं । इस गुणस्थानमें परम विशुद्धिको धारण करते हुए अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त होते हैं तथा वहां पूर्वको अपेक्षा सातिशय शुद्धिसे युक्त होते हैं।
भावार्थ- पहले बताया गया है कि प्रथमोपणम् सम्यग्दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणी मांडनेकी योग्यता नहीं रखते । जब कोई क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि मुनि उपशमश्रेणी मांडनेके सम्मुख होते हैं तब वे अमन्तानुबन्धी चतुष्क और मिथ्यात्वादि त्रिकका उपशम करते हैं। यहां अनन्तानुबन्धीके उपशमका अर्थ है अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य प्रकृतिरूप रहना । इसे अन्यत्र विसंयोजन कहा है और उदय में नहीं आना यह दर्शन- मोहनीय त्रिक- मिथ्यात्वादिक त्रिकके उपशमका अर्थ है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको उत्पत्ति लब्धिसारादि अन्य ग्रन्थोंमें अप्रमत्तविरत नामक सप्तम गुणस्थान में बतलाई है परन्तु धवला पु० १ ( पृष्ठ २१० ) में असंयत सम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्तविरत नामक सप्तम गुणस्थान तक चार गुणस्थानों में रहनेवाला कोई भी जोव कर सकता है, यह बताया है। लब्धिसारादि ग्रन्थोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उपशमको विसंयोजन नामसे कहा है