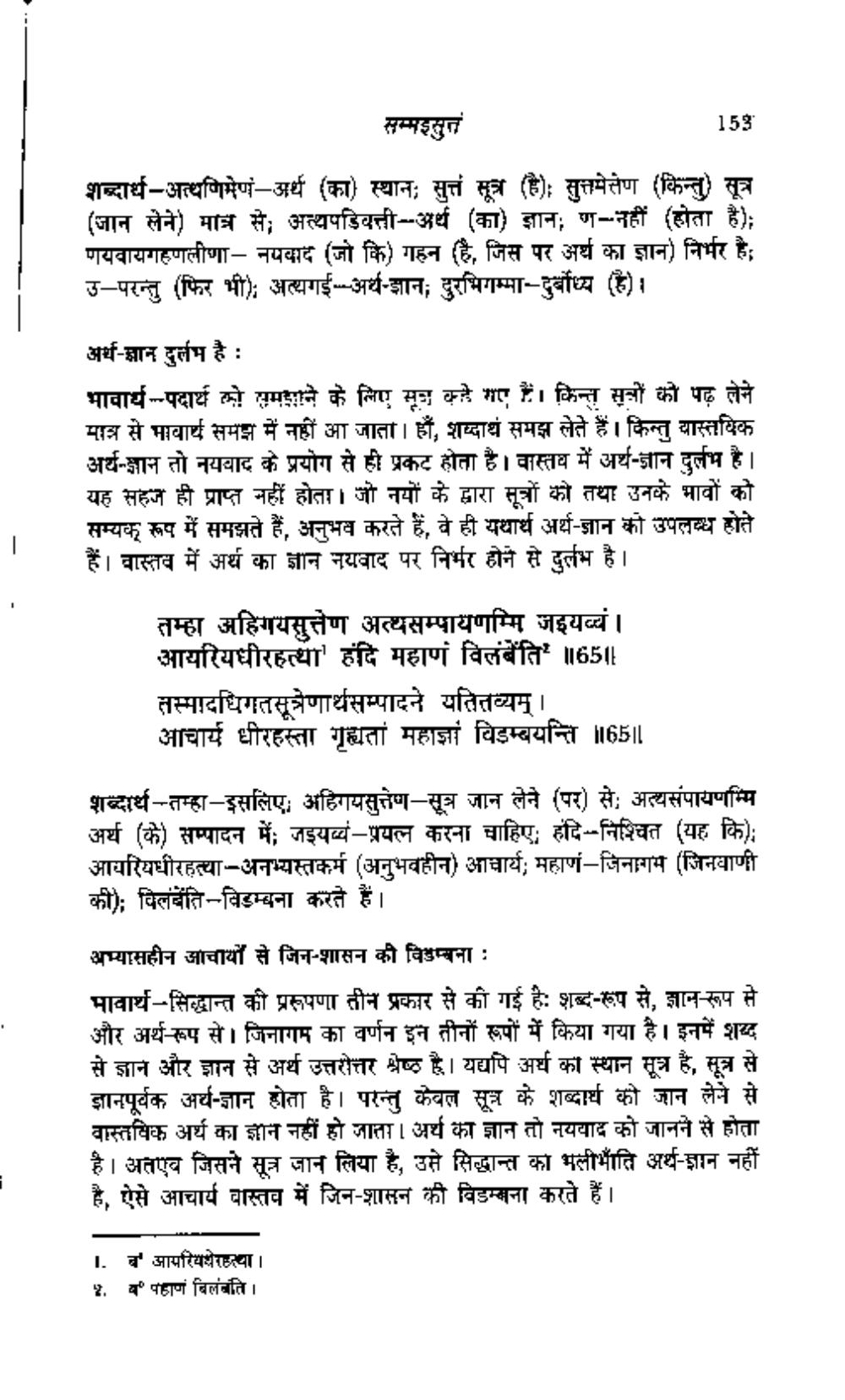________________
सम्मइसुतं
153
शब्दार्थ-अत्यणिमेणं-अर्थ (का) स्थान; सुत्तं सूत्र (है); सुत्तमेतेण (किन्तु) सूत्र (जान लेने) मात्र से; अत्यपडिक्त्ती-अर्थ (का) ज्ञान; ण-नहीं (होता है); णयवायगहणलीणा- नयवाद (जो कि) गहन (है, जिस पर अर्थ का ज्ञान) निर्भर है। उ-परन्तु (फिर भी); अत्यगई-अर्थ-झान; दुरभिगम्मा-दुर्बोध्य (है)।
अर्थ-ज्ञान दुर्लभ है : भावार्थ-पदार्थ को समझाने के लिए सुन कहे गए है। किन्त सलों को पढ़ लेने मात्र से भावार्थ समझ में नहीं आ जाता। हाँ, शब्दाथं समझ लेते हैं। किन्तु यास्तयिक अर्थ-ज्ञान तो नयवाद के प्रयोग से ही प्रकट होता है। वास्तव में अर्थ-ज्ञान दुर्लभ है। यह सहज ही प्राप्त नहीं होता। जो नयों के द्वारा सूत्रों को तथा उनके भावों को सम्यक रूप में समझते हैं, अनुभव करते हैं, वे ही यथार्थ अर्थ-ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। वास्तव में अर्थ का ज्ञान नयवाद पर निर्भर होने से दुर्लभ है।
तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्थसम्पायणम्मि जइयव्यं । आयरियधीरहत्या' हंदि महाणं विलंबेंति' ॥65।। तस्मादधिगतसूत्रेणार्थसम्पादने यतितव्यम् । आचार्य धीरहस्ता गृह्यतां महाज्ञा विडम्बयन्ति ॥65||
शब्दार्थ-तम्हा-इसलिए, अहिंगयसुत्तेण-सूत्र जान लेने (पर) से; अस्थसंपायणम्मि अर्थ (के) सम्पादन में जइयव्यं-प्रयत्न करना चाहिए; हंदि निश्चित (यह कि); आयरियधीरहत्या-अनभ्यस्तकर्म (अनुभवहीन) आचार्य; महाणं-जिनागम (जिनवाणी की); विलति-विडम्बना करते हैं।
अभ्यासहीन आचार्यों से जिन-शासन की विडम्बना : भावार्थ-सिद्धान्त की प्ररूपणा तीन प्रकार से की गई है: शब्द-रूप से, ज्ञान-रूप से और अर्थ-रूप से। जिनागम का वर्णन इन तीनों रूपों में किया गया है। इनमें शब्द से ज्ञान और ज्ञान से अर्थ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। यद्यपि अर्थ का स्थान सूत्र है, सूत्र से ज्ञानपूर्वक अर्थ-ज्ञान होता है। परन्तु केवल सूत्र के शब्दार्थ को जान लेने से वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं हो जाता। अर्थ का ज्ञान तो नयवाद को जानने से होता है। अतएव जिसने सूत्र जान लिया है, उसे सिद्धान्त का भलीभाँति अर्थ-ज्ञान नहीं है, ऐसे आचार्य वास्तव में जिन-शासन की विडम्बना करते हैं।
।. ब' आरियरहत्या। १. व पहाणं बिलंबंति।