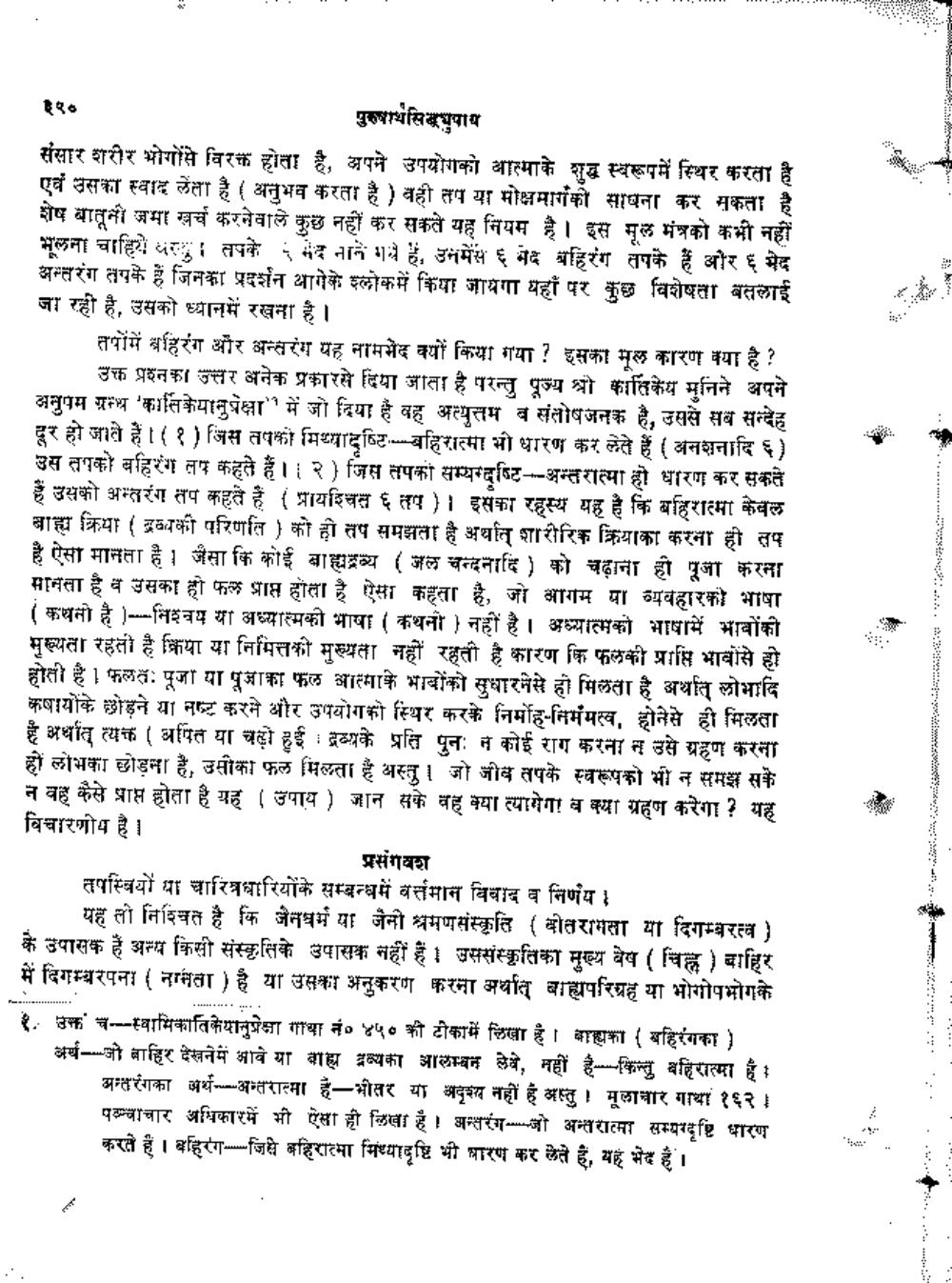________________
३५०
पुरुषार्था
संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, अपने उपयोगको आत्माके शुद्ध स्वरूपमें स्थिर करता है एवं उसका स्वाद लेता है ( अनुभव करता है ) वही तप या मोक्षमार्गको साधना कर सकता है शेष बातूनी जमा खर्च करनेवाले कुछ नहीं कर सकते यह नियम है। इस मूल मंत्र को कभी नहीं भूलना चाहिये वस्तु तपके दाने गये हैं, उनमें ६ मद बहिरंग तपके हैं और ६ भेद अन्तरंग तपके हैं जिनका प्रदर्शन आगेके श्लोक में किया जायेगा यहाँ पर कुछ विशेषता बतलाई जा रही है, उसको ध्यान में रखना है ।
तयोंमें बहिरंग और अन्तरंग यह नामभेद क्यों किया गया ? इसका मूल कारण क्या है ?
उक्त प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता है परन्तु पूज्य श्री कार्तिकेय मुनिने अपने अनुपम ग्रन्थ 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा" में जो दिया है वह अत्युत्तम व संतोषजनक है, उससे सब सन्देह दूर हो जाते हैं । ( १ ) जिस तपकी मिथ्यादृष्टि - बहिरात्मा भी धारण कर लेते हैं ( अनशनादि ६ ) उस तपको बहिरंग लप कहते हैं ।। २) जिस तपकी सम्यग्दृष्टि[-- अन्तरात्मा हो धारण कर सकते हैं उसको अन्तरंग तप कहते हैं ( प्रायश्चित ६ तप । इसका रहस्य यह है कि बहिरात्मा केवल बाह्य क्रिया (sant परिणति ) को ही तप समझता है अर्थात् शारीरिक क्रियाका करना ही तप है ऐसा मानता है । जैसा कि कोई बाह्यद्रव्य ( जल चन्दनादि ) को चढ़ाना ही पूजा करना मानता है व उसका हो फल प्राप्त होता है ऐसा कहता है, जो आगम या व्यवहारको भाषा ( कथनो है ) - निश्वय या अध्यात्मको भाषा ( कथनी ) नहीं है । अध्यात्मको भाषामें भावोंकी मुख्यता रहती है क्रिया या निमित्तको मुख्यता नहीं रहती है कारण कि फलकी प्राप्ति भावोंसे हो होती है । फलतः पूजा या पूजाका फल आत्माके भावोंको सुधारनेसे ही मिलता है अर्थात् लोभादि कषायों छोड़ने या नष्ट करने और उपयोगको स्थिर करके निर्मोह-निर्ममत्व होनेसे ही मिलता है अर्थात् त्यक्त ( अर्पित या चढ़ी हुई द्रव्यके प्रति पुनः न कोई राग करना न उसे ग्रहण करना हो लोभका छोड़ना हैं, उसीका फल मिलता है अस्तु । जो जीव तपके स्वरूपको भी न समझ सके न वह कैसे प्राप्त होता है यह ( उपाय ) जान सके वह क्या त्यागेगा व क्या ग्रहण करेगा ? यह विचारणीय है ।
प्रसंगवश
तपस्वियों या चारित्रधारियोंके सम्बन्ध में वर्तमान विवाद व निर्णय
यह तो निश्चित है कि जैनधर्म या जैनी श्रमण संस्कृति ( वीतरामता या दिगम्बरत्व ) के उपासक हैं अन्य किसी संस्कृतिके उपासक नहीं हैं । उससंस्कृतिका मुख्य वेष (चिह्न) बाहिर में दिगम्बरपना ( नाता ) है या उसका अनुकरण करना अर्थात् बाह्यपरिग्रह या भोगोपभोगके
१. उक्त च स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा नं० ४५० की टीका लिखा है। बाह्यका ( बहिरंगका ) अर्थ---जो बाहिर देखने में आवे या वाह्य अव्यका आलम्बन लेवे, नहीं है-किन्तु वहिरात्मा हूँ +
अन्तरंगका अर्थ----अन्तरात्मा है - भीतर या अदृश्य नहीं है अस्तु । मूलाचार गाथा १६२ । पत्राचार अधिकार में भी ऐसा ही लिखा है । अन्तरंग -जो अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टि धारण करते हैं । बहिरंग — जिसे बहिरात्मा मिध्यादृष्टि भी धारण कर लेते हैं, यह भेद हैं ।