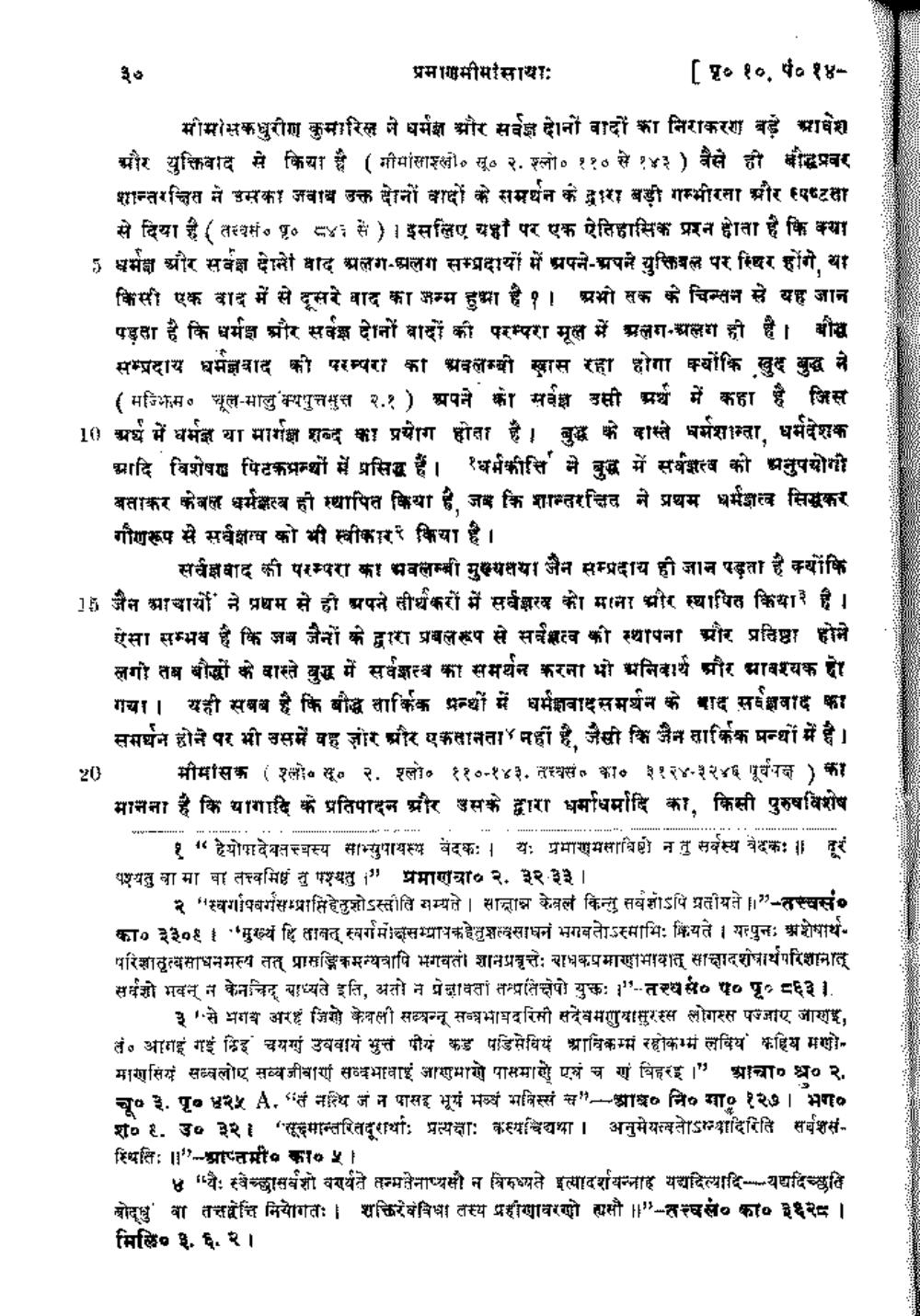________________
प्रमाणमीमांसायाः
[ पृ० १०. पं०१४
5
frienधुरी कुमारिल ने धर्मज्ञ और सर्वज्ञ दोनों वादों का निराकरण बड़े आवेश और युक्तिवाद से किया है ( मीमांसारखी० सू० २. श्लो० ११० से १४३ ) वैसे ही बौद्धप्रवर शान्तरक्षित ने उसका जवाब उक्त दोनों वादों के समर्थन के द्वारा बड़ी गम्भीरता और स्पष्टता से दिया है ( तस्व० पृ० ४ ) । इसलिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रश्न होता है कि क्या और सर्वज्ञ दोनो बाद अलग-अलग सम्प्रदायों में अपने-अपने युक्तिबल पर स्थिर होंगे, या किसी एक बाद में से दूसरे वाद का जन्म हुआ है १ । अभी तक के चिन्तन से यह जान yer है कि धर्म और सर्वश दोनों वादों की परम्परा मूल में अलग-अलग ही है। बौद्ध सम्प्रदाय धर्मवाद की परम्परा का अवलम्बी खास रहा होगा क्योंकि खुद बुद्ध ने ( मज्यिम० चूल-मालुक्यपुत्तसुत २.१ ) अपने को सर्वक्ष उसी अर्थ में कहा है जिस 10 अर्थ में धर्मज्ञ या मार्गश शब्द का प्रयोग होता है । बुद्ध के वास्ते धर्मशाता, धर्मदेशक आदि विशेषण पटकप्रन्थों में प्रसिद्ध हैं । १धर्मकीर्ति ने बुद्ध में सर्वशत्व को अनुपयोगी aaree hair after हो स्थापित किया है, जब कि शान्तरक्षित ने प्रथम धर्मज्ञत्व सिकर tray से सर्वज्ञ को भी स्वीकार किया है ।
३०
सर्वज्ञबाद की परम्परा का अवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पड़ता है क्योंकि 15 जैन आचार्यों ने प्रथम से ही अपने तीर्थकरों में सर्वज्ञस्य को माना और स्थापित किया है । ऐसा सम्भव है कि जब जैनों के द्वारा प्रबलरूप से सर्वशत्व की स्थापना और प्रतिष्ठा होने लगी तब बौद्धों के वास्ते बुद्ध में सर्वज्ञत्व का समर्थन करना भी अनिवार्य और आवश्यक हो गया । यही सबब है कि बौद्ध तार्किक प्रन्थों में धर्मज्ञवादसमर्थन के बाद सर्वेक्षवाद कर समर्थन होने पर भी उसमें वह जोर और एकतानता नहीं है, जैसी कि जैन तार्किक पन्थों में है ।
20
मीमांसक (श्लो० सू० २ श्लो० ११०-१४३. ० का० ३१२४-३२४६ पूर्व ) का मानना है कि यागादि के प्रतिपादन और उसके द्वारा धर्माधर्मादि का, किसी पुरुषविशेष
१८ हैयोपदेवत स्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः || तुरं पश्यतु वा मा वा त्वमिष्टं तु पश्यतु " प्रमाणवा० २. ३२.३३ ।
२ स्वर्गापवर्गासहेतुज्ञोऽस्तीति यम्यते । सान्नान्न केवलं किन्तु सर्वशोऽपि प्रतीयते ।। " तस्वसं० का० ३३०६ | "मुख्य हि तावत् स्वर्गमोक्षसभ्यापक हेतृशत्वसाधनं भगवतोऽस्माभिः क्रियते । यत्पुनः अशेषार्थपरिशातृत्वसाधनमस्य तत् प्रासङ्गिकमन्यत्रापि भगवती ज्ञानप्रवृत्तेः बाधकप्रमाणाभावात् साक्षादशेषार्थ परिज्ञानात् सर्वज्ञो भवन् न केनचिद् बाध्यते इति, अतो न प्रेावतां तत्प्रतिक्षेपो युक्तः ।" तर० प० पृ० ८६३ | ३ से भग अहं जिसे केवली सम्पन्नू सन्यभावदरिसी सदेवमगुवासुरस्त लोगस्स पज्जाए जागर, ० आगई गई कि चयj उववायं सुतं पीयं क पडिसेवियं श्राविकम्मं रोकम्मं लविय कहिय मोमासय सम्बलोए सव्वजीवाणं सव्वभावाई जारामागे पासमा एवं च यं विहर।" श्राचा० श्र० २. चू० ३. पृ० ४२५ A. “तं नत्थ जंन पास भूयं भव्यं भविस्सं च" आव० नि० मा० १२७ । भगव ०१. उ० ३२ ॥ सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति सर्वशसस्थितिः ॥" आप्तमी० का ५ ।
"यैः स्वेच्छासो वयते तन्मतेनाप्यसौ न विरुध्यते इत्यादर्शयन्नाह यद्यदित्यादि --- यद्यदिच्युति श्रोतु ं वा तत्तद्वेत्ति नियोगतः । शक्तिरेवंविधा तस्य प्रहीयावरयो त्यसौ ।" - तरवले० का० २६२८ । मिलि० ३. ६.२ ।