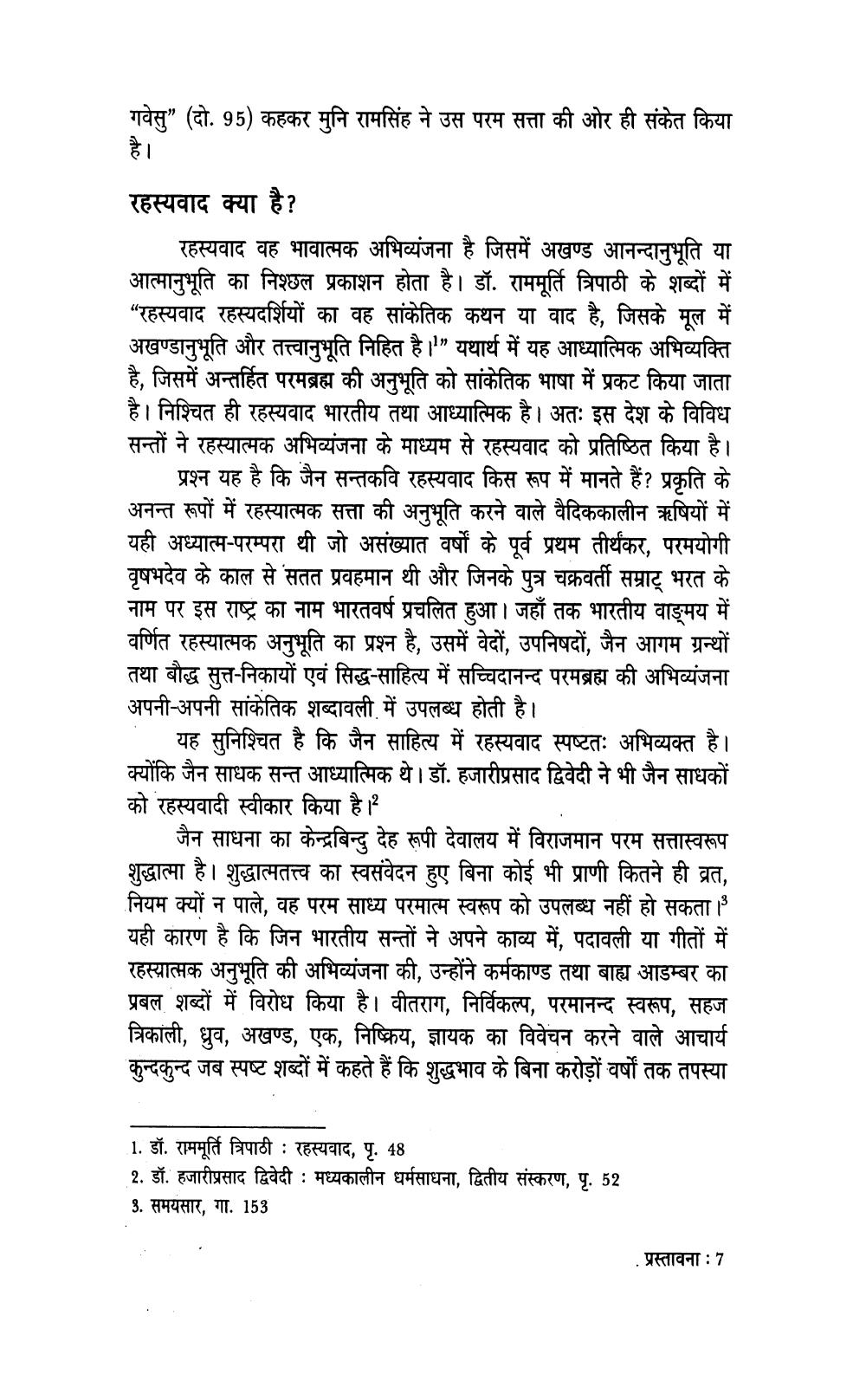________________
गवेसु” (दो. 95) कहकर मुनि रामसिंह ने उस परम सत्ता की ओर ही संकेत किया है।
रहस्यवाद क्या है ?
रहस्यवाद वह भावात्मक अभिव्यंजना है जिसमें अखण्ड आनन्दानुभूति या आत्मानुभूति का निश्छल प्रकाशन होता है। डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी के शब्दों में “ रहस्यवाद रहस्यदर्शियों का वह सांकेतिक कथन या वाद है, जिसके मूल में अखण्डानुभूति और तत्त्वानुभूति निहित है ।" यथार्थ में यह आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अन्तर्हित परमब्रह्म की अनुभूति को सांकेतिक भाषा में प्रकट किया जाता है । निश्चित ही रहस्यवाद भारतीय तथा आध्यात्मिक है । अतः इस देश के विविध सन्तों ने रहस्यात्मक अभिव्यंजना के माध्यम से रहस्यवाद को प्रतिष्ठित किया है।
प्रश्न यह है कि जैन सन्तकवि रहस्यवाद किस रूप में मानते हैं? प्रकृति के अनन्त रूपों में रहस्यात्मक सत्ता की अनुभूति करने वाले वैदिककालीन ऋषियों में यही अध्यात्म-परम्परा थी जो असंख्यात वर्षों के पूर्व प्रथम तीर्थंकर, परमयोगी वृषभदेव के काल से सतत प्रवहमान थी और जिनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट् भरत के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष प्रचलित हुआ । जहाँ तक भारतीय वाङ्मय में वर्णित रहस्यात्मक अनुभूति का प्रश्न है, उसमें वेदों, उपनिषदों, जैन आगम ग्रन्थों तथा बौद्ध सुत्त-निकायों एवं सिद्ध- साहित्य में सच्चिदानन्द परमब्रह्म की अभिव्यंजना अपनी-अपनी सांकेतिक शब्दावली में उपलब्ध होती है।
यह सुनिश्चित है कि जैन साहित्य में रहस्यवाद स्पष्टतः अभिव्यक्त है। क्योंकि जैन साधक सन्त आध्यात्मिक थे। डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी जैन साधकों को रहस्यवादी स्वीकार किया है । 2
जैन साधना का केन्द्रबिन्दु देह रूपी देवालय में विराजमान परम सत्तास्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मतत्त्व का स्वसंवेदन हुए बिना कोई भी प्राणी कितने ही व्रत, नियम क्यों न पाले, वह परम साध्य परमात्म स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो सकता । यही कारण है कि जिन भारतीय सन्तों ने अपने काव्य में, पदावली या गीतों में रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यंजना की, उन्होंने कर्मकाण्ड तथा बाह्य आडम्बर का प्रबल शब्दों में विरोध किया है। वीतराग, निर्विकल्प, परमानन्द स्वरूप, सहज त्रिकाली, ध्रुव, अखण्ड, एक, निष्क्रिय, ज्ञायक का विवेचन करने वाले आचार्य कुन्दकुन्द जब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि शुद्धभाव के बिना करोड़ों वर्षों तक तपस्या
1. डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी : रहस्यवाद, पृ. 48
2. डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी : मध्यकालीन धर्मसाधना, द्वितीय संस्करण, पृ. 52
3. समयसार, गा. 153
प्रस्तावना : 7