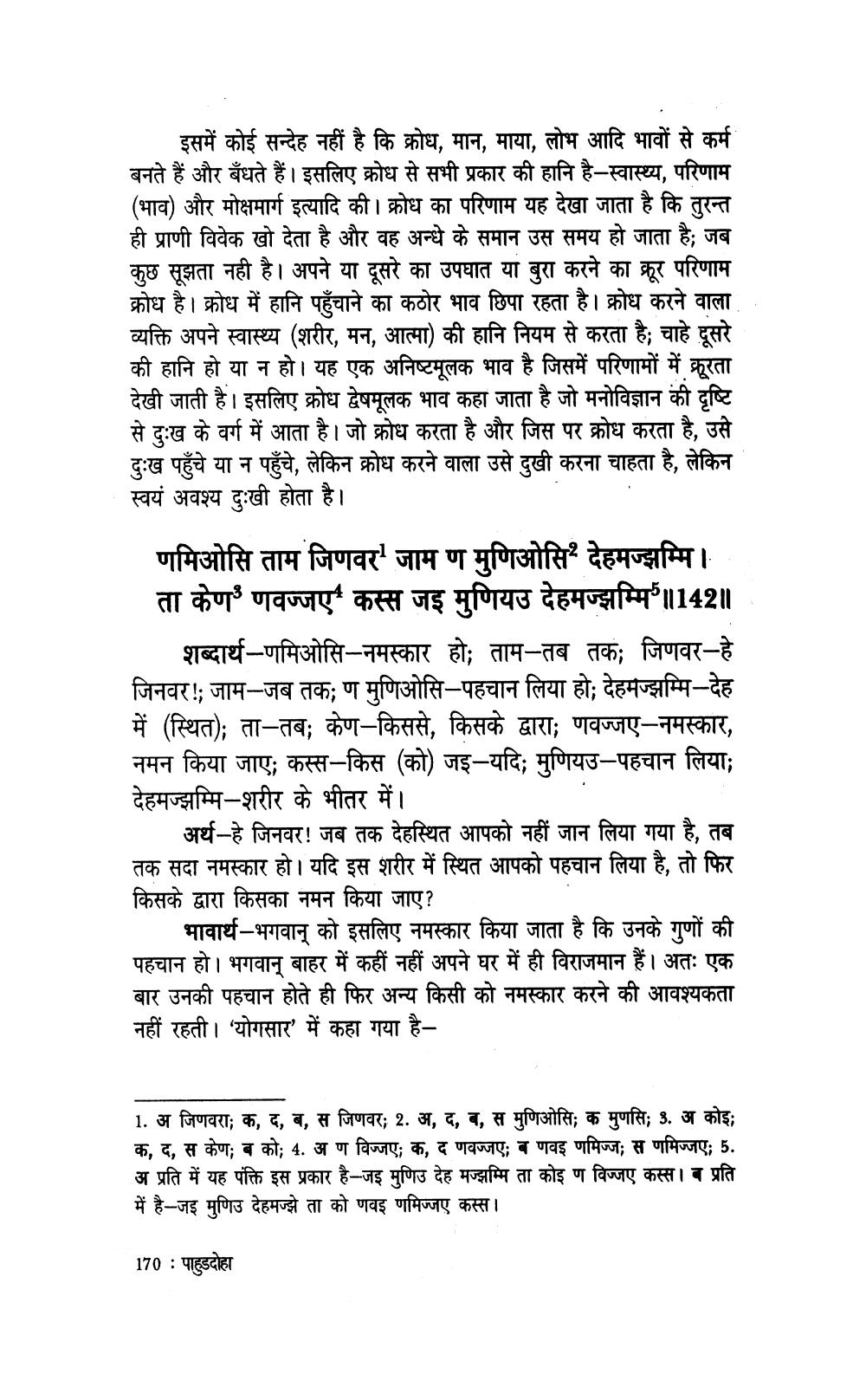________________
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावों से कर्म बनते हैं और बँधते हैं। इसलिए क्रोध से सभी प्रकार की हानि है-स्वास्थ्य, परिणाम (भाव) और मोक्षमार्ग इत्यादि की। क्रोध का परिणाम यह देखा जाता है कि तुरन्त ही प्राणी विवेक खो देता है और वह अन्धे के समान उस समय हो जाता है; जब कुछ सूझता नही है। अपने या दूसरे का उपघात या बुरा करने का क्रूर परिणाम क्रोध है। क्रोध में हानि पहुँचाने का कठोर भाव छिपा रहता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य (शरीर, मन, आत्मा) की हानि नियम से करता है; चाहे दूसरे की हानि हो या न हो। यह एक अनिष्टमूलक भाव है जिसमें परिणामों में क्रूरता देखी जाती है। इसलिए क्रोध द्वेषमूलक भाव कहा जाता है जो मनोविज्ञान की दृष्टि से दुःख के वर्ग में आता है। जो क्रोध करता है और जिस पर क्रोध करता है, उसे दुःख पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन क्रोध करने वाला उसे दुखी करना चाहता है, लेकिन स्वयं अवश्य दुःखी होता है।
णमिओसि ताम जिणवर जाम ण मुणिओसि देहमज्झम्मि। ता केण णवज्जए' कस्स जइ मुणियउ देहमज्झम्मि॥142॥
शब्दार्थ-णमिओसि-नमस्कार हो; ताम-तब तक; जिणवर-हे जिनवर!; जाम-जब तक; ण मुणिओसि-पहचान लिया हो; देहमज्झम्मि-देह में (स्थित); ता-तब; केण-किससे, किसके द्वारा; णवज्जए-नमस्कार, नमन किया जाए; कस्स-किस (को) जइ-यदि; मुणियउ-पहचान लिया; देहमज्झम्मि–शरीर के भीतर में।
अर्थ-हे जिनवर! जब तक देहस्थित आपको नहीं जान लिया गया है, तब तक सदा नमस्कार हो। यदि इस शरीर में स्थित आपको पहचान लिया है, तो फिर किसके द्वारा किसका नमन किया जाए?
भावार्थ-भगवान् को इसलिए नमस्कार किया जाता है कि उनके गुणों की पहचान हो। भगवान् बाहर में कहीं नहीं अपने घर में ही विराजमान हैं। अतः एक बार उनकी पहचान होते ही फिर अन्य किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती। 'योगसार' में कहा गया है
1. अ जिणवरा; क, द, ब, स जिणवर; 2. अ, द, ब, स मुणिओसि; क मुणसि; 3. अ कोइ क, द, स केण; ब को; 4. अ ण विज्जए; क, द णवज्जए; ब णवइ णमिज्ज; स णमिज्जए; 5. अ प्रति में यह पंक्ति इस प्रकार है-जइ मुणिउ देह मज्झम्मि ता कोइ ण विज्जए कस्स। व प्रति में है-जइ मुणिउ देहमज्झे ता को णवइ णमिज्जए कस्स।
170 : पाहुडदोहा