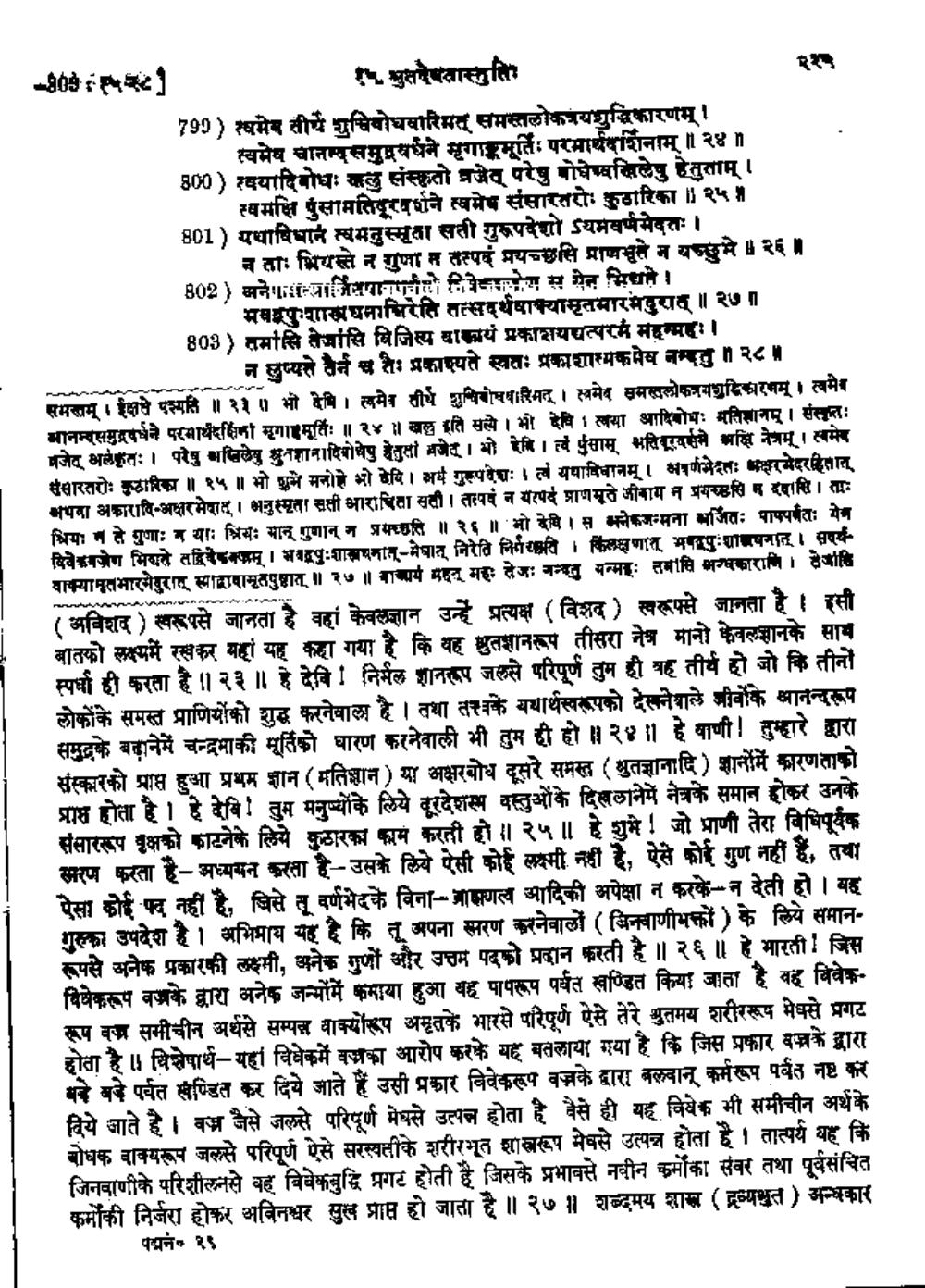________________
R
-80Bire
१५. भुतदेवतास्तुति 799 ) स्वमेव तीर्य शुधिबोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् ।
त्वमेव चानम्दसमुद्रवर्धने मुगाङ्कमूर्तिः परमार्थदर्शिनाम् ॥ २४ ॥ 800 ) स्वयादिबोधः बलु संस्कृतो प्रजेत् परेषु मोघेण्यखिलेषु हेतुताम् ।
स्वमक्षि पुंसामतिदूरवर्शने स्वमेष संसारतरोः कुठारिका ॥ २५॥ 801) यथाविधान स्वमनुस्मृता सती गुरूपदेशो ऽयमवर्णमेदतः।
न ताः भियस्ते न गुणाम तस्पद मयच्छसि प्राणभृते न यच्छुमे ॥ २६ ॥ 802 ) मार्जिापोटोहियोग स न मियते।।
भवापु-शासघनाभिरेति तत्सदर्थवाक्यामृतमारमदुरात् ॥ २७ ॥ 803) तमांसि तेजासि विजिस्य वाकार्य प्रकाशययत्परम महन्महः।
न लुप्यते ते बरी:प्रकाश्यते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नम्बतु ॥२८॥ समस्तम् । ईशवे पश्यति ॥ २३ ॥ भो देधि । त्वमेव तीर्थ शुधियोषधारिमत् । स्त्रमेव समस्खलोकत्रगशुद्धिकरणम् । त्वमेव मानन्दसमुद्रवर्धने परमार्थदर्शिनी मृगाइमूर्तिः ॥ २४ ॥ खल्लु इति सले । भी देवि । स्वया आदिवोपः मतिमानम् । संसातः बजेट अलेकृतः। परेषु अखिलेषु शुतज्ञानादियोधेपु हेतुसो बजेट । भो देहि। त्वं पुंसाम् भतिएवसमे अक्षि नेत्रम् । स्वमेव संवारतरोः कुलारिका ॥१५॥ भो शुभ मनोहे भो देवि। भर्य गुरूपवेधः । त्वंयपाविधानम् । अवर्णमेदतः भक्षरमेदरहितात् भषवा अकारादि-अक्षरमेशात् । भनुस्मृता सप्ती आराधिता सती । तत्पदं न यरपर्द प्राणमते जीवाम न प्रयच्छसि म ददासि । ताः श्रियःमते गुणाः वयाः श्रियः मान् गुणान् न प्रयच्छति ॥२६॥ भो देवि।स भनेकजन्मना भर्जितः पापपर्वतः येष विवेकबजेग मिद्यते सद्विवेकानाम् । भवपुःशासाचनात्-मेघात् निरेति निराति । किंलक्षणात् मादपुःशाषनात् । समयवाक्यामतमारमेबुरात स्मादावामृतपुष्टात् ॥ २७ ॥ बार्य महन् महः तेजा नन्दन यन्महः तमाधि मन्धकाराणि । जाति (अविशद ) वरूपसे जानता है वहां केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद ) स्वरूपसे जानता है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहां यह कहा गया है कि यह भुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलझानके साथ स्पर्धा ही करता है ॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल शानलए जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंको शुद्ध करनेवाला है । तथा तस्वके यथार्थस्वरूपको देखनेवाले जीवोंके श्रानन्दरूप समुद्र के बढ़ाने में चन्द्रमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥२४॥ हे वाणी! तुम्हारे द्वारा संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त (श्रुतज्ञानादि) शानों में कारणताको प्रास होता है। हे देवि! तुम मनुष्यों के लिये दूरदेशल वस्तुओंके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके संसाररूप वृक्षको काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥२५॥ हे शुभे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक सरण करता है- अध्ययन करता है- उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसे कोई गुण नहीं हैं, तथा ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णभेदके विना-प्रामणत्व आदिकी अपेक्षा न करके न देती हो । यह गुरुका उपदेश है। अभिप्राय यह है कि तू अपना सरण करनेवालों (जिनवाणीभक्तों) के लिये समानरूपसे अनेक प्रकारकी लक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥२६॥ हे भारती! जिस विवेकरूप वनके द्वारा अनेक जन्मों में कमाया हुआ यह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेकरूप वन समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योरप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीररूप मेषसे प्रगट होता है । विशेषार्थ-यहां विवेकमें वनका आरोप करके यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार बनके द्वारा बड़े बड़े पर्वत खण्डित कर दिये आते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वजके द्वारा बलवान् कर्मरूप पर्वत नष्ट कर दिये जाते है। वन जैसे जलसे परिपूर्ण मेघसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थ के बोधक वाक्यरूप जलसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरभूत शास्त्ररूप मेवसे उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे यह विवेकबुद्धि प्रगट होती है जिसके प्रभावसे नवीन कोंका संवर तथा पूर्वसंचित कोंकी निर्जरा होकर अविनश्चर सुख प्राप्त हो जाता है ॥ २७॥ शब्दमय शाम (द्रव्यभूत ) अन्धकार
पद्मनं २७