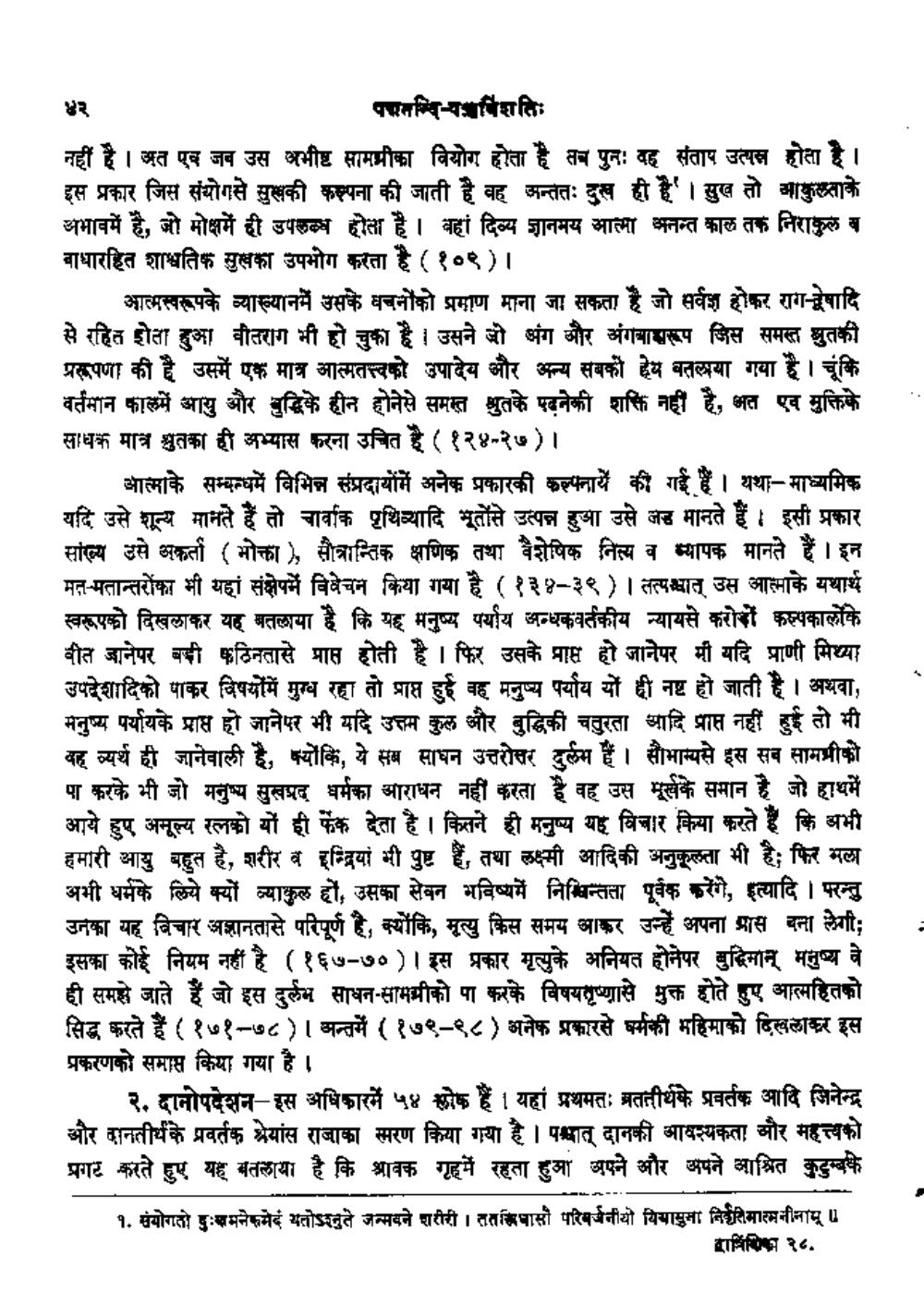________________
पचनन्धि-पत्रपिंशतिः नहीं है । अत एव जब उस अभीष्ट सामग्रीका वियोग होता है सब पुनः वह संताप उत्पन होता है। इस प्रकार जिस संयोगसे सुखकी कल्पना की जाती है वह अन्ततः दुख ही है। सुख तो माकुलताके अभावमें है, जो मोक्षमें ही उपलब्ध होता है। वहां दिव्य ज्ञानमय आमा अनन्त काल तक निराकुल व बाधारहित शाश्चतिक सुखका उपभोग करता है (१०९)।
___ आत्मस्वरूपके व्याख्यानमें उसके वचनोंको प्रमाण माना जा सकता है जो सर्वज्ञ होकर राग-द्वेषादि से रहित होता हुआ वीतराग भी हो चुका है। उसने जो अंग और अंगवामरूप जिस समस्त श्रुतकी प्ररूपणा की है उसमें एक मात्र आत्मतत्वको उपादेय और अन्य सबको हेय बतलाया गया है। चूंकि वर्तमान कालमें आयु और बुद्धिके हीन होनेसे समस्त श्रुतके पढ़नेकी शक्ति नहीं है, अत एव मुक्तिके साधक मात्र श्रुतका ही अभ्यास करना उचित है ( १२४-२७)।
___ आत्माके सम्बन्धमें विभिन्न संप्रदायोंमें अनेक प्रकारकी कल्पनायें की गई है। यथा-माध्यमिक यदि उसे शून्य मानते हैं तो चार्वाक पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हुआ उसे जड मानते हैं। इसी प्रकार सांख्य उसे अकर्ता (भोक्ता ), सौत्रान्तिक क्षणिक तथा वैशेषिक नित्य व व्यापक मानते हैं। इन मत-मतान्तरोंका भी यहां संक्षेपमें विवेचन किया गया है ( १३४-३९) । तत्पश्चात् उस आत्माके यथार्थ स्वरूपको दिखलाकर यह बतलाया है कि यह मनुष्य पर्याय अन्धकवर्तकीय न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंके वीत जानेपर बड़ी फठिनतासे प्राप्त होती है। फिर उसके प्राप्त हो जानेपर मी यदि प्राणी मिथ्या उपदेशादिको पाकर विषयों में मुग्ध रहा तो प्राप्त हुई वह मनुष्य पर्याय यों ही नष्ट हो जाती है । अथवा, मनुष्य पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी यदि उत्तम कुल और बुद्धिकी चतुरता आदि प्राप्त नहीं हुई तो भी वह व्यर्थ ही जानेवाली है, क्योंकि, ये सब साधन उत्तरोतर दुर्लभ हैं। सौभाग्यसे इस सब सामग्रीको पा करके भी जो मनुष्य सुखप्रद धर्मका आराधन नहीं करता है वह उस मूखके समान है जो हाथमें आये हुए अमूल्य रलको यों ही फेंक देता है । कितने ही मनुष्य यह विचार किया करते हैं कि अभी हमारी आयु बहुत है, शरीर व इन्द्रियों भी पुष्ट हैं, तथा लक्ष्मी आदिकी अनुकूलता भी है; फिर मला अभी धर्मके लिये क्यों व्याकुल हों, उसका सेवन भविष्यमें निम्विन्तता पूर्वक करेंगे, इत्यादि । परन्तु उनका यह विचार अज्ञानतासे परिपूर्ण है, क्योंकि, मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना पास बना लेगी; इसका कोई नियम नहीं है (१६७-७०)। इस प्रकार मृत्युके अनियत होनेपर बुद्धिमान् मनुष्य वे ही समझे जाते हैं जो इस दुर्लभ साधन-सामग्रीको पा करके विषयतृष्णासे मुक्त होते हुए आत्महितको सिद्ध करते हैं ( १७१-७८) । अन्तमें ( १७९-९८) अनेक प्रकारसे धर्मकी महिमाको दिखलाकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।
२.दानोपदेशन-इस अधिकारमें ५४ लोक हैं। यहां प्रथमतः प्रततीर्थके प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और वानतीर्थ के प्रवर्तक श्रेयांस राजाका स्मरण किया गया है । पश्चात् दानकी आवश्यकता और महत्त्वको प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि श्रावक गृहमें रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुटुम्बके १. संयोगतो दुःखमनेकमेदं यतोऽश्नुते जन्मदने शरीरी । ततलिचासौ परिवर्जनीयो यियामुना नितिमात्मनीनाम् ॥
वानिधिस २८.