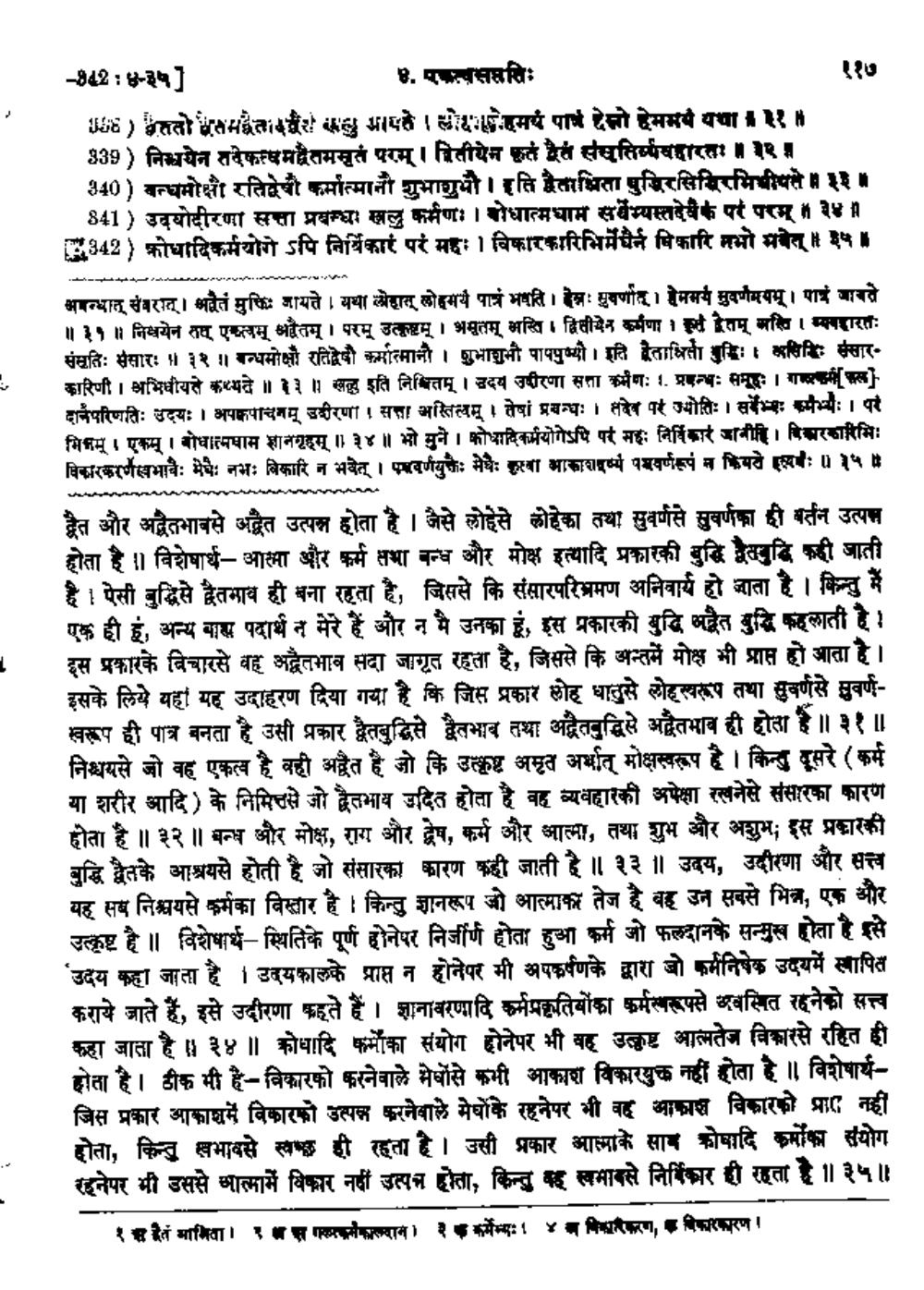________________
-342 : ४-३५]
१. एकत्वसप्ततिः IFE ) ततो समता मापते । लोहमयं पार्थ देखो हेममय यथा ॥५॥ 139) निश्चयेन तदेकत्यमद्वैतममृतं परम् । वितीयेम मत देत संपतिर्व्यवहारतः ॥२९ 340 ) बन्धमोक्षी रतिवेषी कर्मात्मानौ शुभाशुभौ । इति बैताधिता पुखिरसिधिरमिधीयते ॥५॥ 841 ) उदयोदीरणा सत्ता प्रबन्धः खलु कर्मणः । बोधात्मधाम सर्वेभ्यस्तदेवेक पर परम् ॥ ३४॥ 5342) क्रोधादिकर्मयोगे ऽपि निर्यिकारं परं महः । विकारकारिभिर्मे धैर्न पिकारि ममो मवेत् ॥ ३५ ॥
अमन्यात् संवरात्। भवेतं मुफिः जायते । यथा लोहार लोहमये पात्रं भवति । दन्नः सुवर्णात् । हेममय मुवर्णमयम् । पात्र जारते ॥३१॥ निश्चयेन तत् एकलम् अवैतम् । परम् उत्कृष्टम् । अमृतम् भस्ति । द्वितीयेन कर्मणा । इन तम् मस्ति । म्यवहारतः संमृतिः संसारः ॥ ३१ ॥बन्धमोक्षौ रतिद्वेषौ कर्मात्मानौ । शुभाशुभौ पापपुण्यो। इति ताधिता अभिः । सिटि संसारकारिणी। अभिधीयते कथ्यते ॥१३॥ खलु इति निधितम् । उदय उदीरणा सत्ता कर्मणः . प्रबन्धः समूहः । गलकमसल) दानपरिणतिः उदयः । अपनपाचनम् उदीरणा । सत्ता अस्तित्वम् । तेषां प्रबन्धः । तदेव पर ज्योतिः । सर्वेभ्यः कर्मभ्यः । पर मिनम् । एकम् । बोधात्मघाम झानगृहम् ॥ ३४ ॥ भो मुने । कोधादिकर्मयोगेऽपि पर महः निर्विकार जानीहि । विचारकारिमिः विकारकरणेखभावैः मेघः नमः बिकारि न भवेत् । फावर्णयुक्तः मेथैः हत्या भाकाशमध्ये पश्वर्णरूपं म कियते इत्यः ॥ ३५॥
द्वैत और अद्वैतभावसे अद्वैत उत्पन्न होता है । जैसे लोहेसे लोहेका तथा सुवर्णसे सुवर्णका ही वर्तन उत्पन्न होता है। विशेषार्थ- आमा और कर्म सभा बन्ध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि बैतबुद्धि कही जाती है । पेसी बुद्धिसे द्वैतभाव ही बना रहता है, जिससे कि संसारपरिश्रमण अनिवार्य हो जाता है। किन्तु में एक ही ई, अन्य बास पदार्थ न मेरे हैं और न मै उनका हूं, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है। इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतभाव सदा जागृत रहता है, जिससे कि अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो आता है। इसके लिये यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह धातुसे लोहस्वरूप तथा सुवर्णसे सुवर्णखरूप ही पात्र बनता है उसी प्रकार द्वैतबुद्धिसे द्वैतभाव तथा अद्वैतबुद्धिसे अद्वैतभाव ही होता है॥३१॥ निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अद्वैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात् मोक्षस्वरूप है । किन्तु दूसरे (कर्म या शरीर आदि) के निमित्तसे जो द्वैतभाव उदित होता है वह व्यवहारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है ॥३२॥ धन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ; इस प्रकारकी बुद्धि द्वैतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कही जाती है ॥ ३३ ॥ उदय, उदीरणा और सत्त्व यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है। किन्तु ज्ञानरूप जो आत्माकर तेज है वह उन सबसे भिन्न, एक और उत्कृष्ट है ॥ विशेषार्थ-स्थितिके पूर्ण होनेपर निर्जीर्ण होता हुआ कर्म जो फलदानके सन्मुख होता है इसे उदय कहा जाता है । उदयकालके प्राप्त न होनेपर मी अपकर्षणके द्वारा जो कर्मनिषेक उदयमें सापित कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतियोंका कर्मस्वरूपसे अवसित रहनेको सत्त्व कहा जाता है ।। ३४ ॥ क्रोधादि कर्मोंका संयोग होनेपर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकारसे रहित ही होता है। ठीक भी है-विकारको करनेवाले मेघोंसे कभी आकाश विकारयुक्त नहीं होता है ॥ विशेषार्थजिस प्रकार आकाशमें विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके रहनेपर भी वह आकाश विकारको प्रार नहीं होता, किन्तु खभावसे स्वछ ही रहता है। उसी प्रकार आत्माके साब कोषादि कर्मोका संयोग रहनेपर भी उससे पात्मामें विकार नहीं उत्पन्न होता, किन्तु यह समावसे निर्विकार ही रहता है ॥३५॥
१ तं मामिवा। सगलवकालवाम) २५ कर्मेभ्यः ४ व विकारकरण, विकासकारण ।