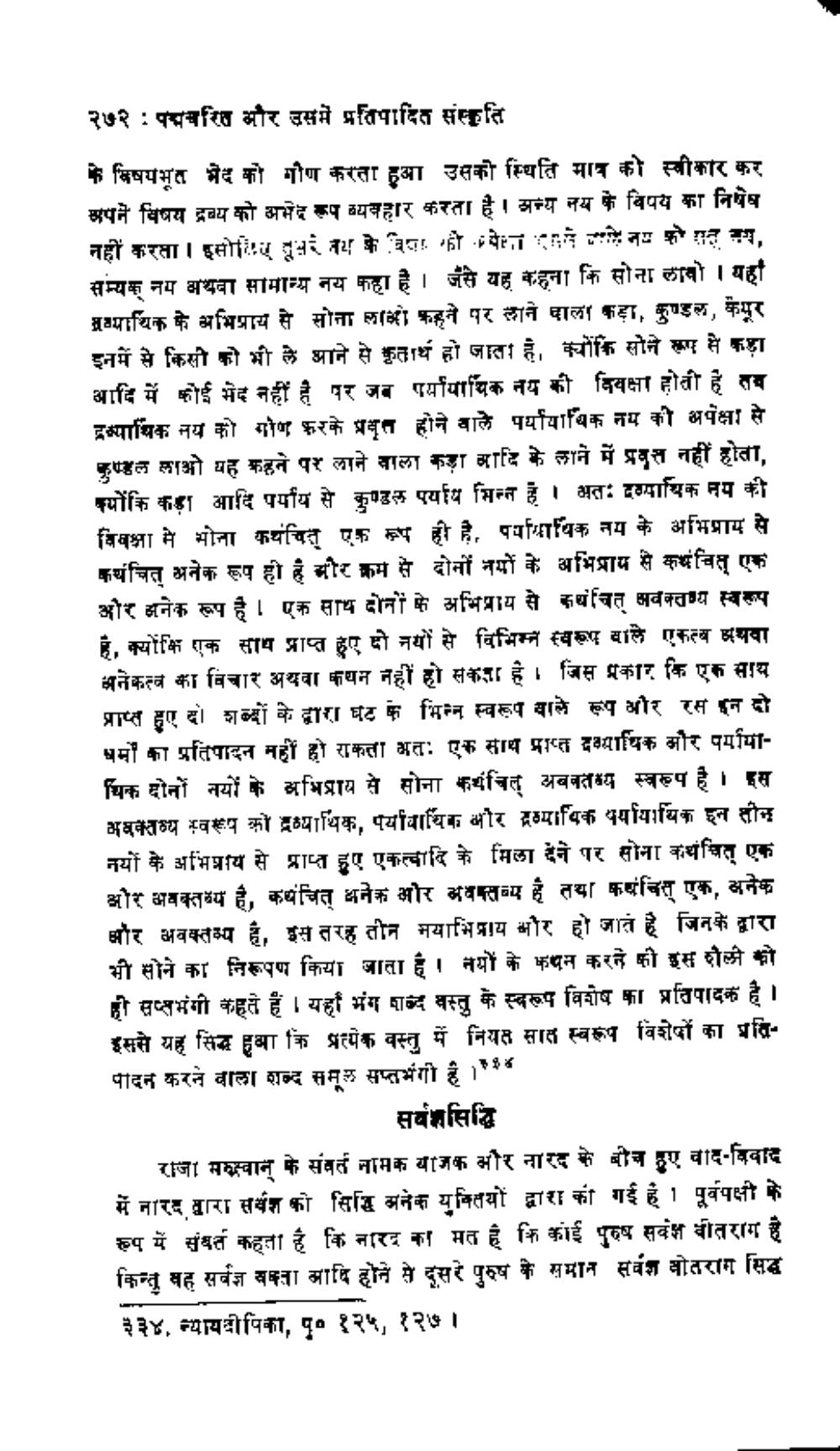________________
२७२ : पनवरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति
के विषयभूत भेद को गौण करता हुआ उसको स्थिति मात्र को स्वीकार कर अपने विषय द्रव्य को अभेद रूप व्यवहार करता है। अन्य नय के विषय का निषेष नहीं करता । इसोनिरसन के बिना को शासन को सात नाय. सम्यक् नय अथवा सामान्य नय कहा है | जैसे यह कहना कि सोना लावो । यहाँ प्रध्याथिक के अभिप्राय से सोना लामो कहने पर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, कैमूर इनमें से किसी को भी ले आने से कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि सोने लए से कड़ा आदि में कोई भेद नहीं है पर जब पर्यायार्थिक नय की विवक्षा होती है तब दम्यार्थिक नय को गोण करके प्रवृत्त होने वाले पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से कुण्डल लाओ यह कहने पर लाने वाला कड़ा मादि के लाने में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्याय से कुण्डल पर्याय मिन्न है । अतः दग्यायिक नय की विवक्षा मे भोना कथंचित् एक रूप ही है, पर्यायाधिक नय के अभिप्राय से कथंचित अनेक रूप ही है और क्रम से दोनों नयों के अभिप्राय से कथंचित एक
और अनेक रूप है । एक साथ दोनों के अभिप्राय से कचित् अवक्तव्य स्वरूप है, क्योंकि एक साथ प्राप्त हए दो नयों से विभिन्न स्वरूप वाले एकत्व अथवा अनेकत्व का विचार अथवा कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो शब्दों के द्वारा घट के भिन्न स्वरूप वाले रूप और रस इन दो धर्मों का प्रतिपादन महीं हो राकता अतः एक साथ प्राप्त दवयार्षिक और पर्यायाथिक दोनों नयों के अभिप्राय से सोना कथंचिल अबवतव्य स्वरूप है। इस अवक्तव्य स्वरूप को द्रव्याथिक, पर्यावार्थिक और म्यार्षिक पर्यायाथिक इन तीन नयों के अभिप्राय से प्राप्त हुए एकत्वादि के मिला देने पर सोना कथंचित् एक और अवक्तव्य है, कथंचित अनेक और अवतब्य है तथा कपंचित् एक, अनेक और अवक्तव्य है, इस तरह तीन मयाभिप्राय और हो जाते है जिनके द्वारा भी सोने का निरूपण किया जाता है। नयों के कथन करने की इस शैली को ही सप्तभंगी कहते हैं । यहाँ भंग शब्द वस्तु के स्वरूप विशेष का प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हया कि प्रत्येक वस्तु में नियत सात स्वरूप विशेषों का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूल सप्तभंगी है । १३४
सर्वशसिद्धि राजा मझवान के संवर्त नामक याजक और नारद के बीच हुए वाद-विवाद में नारद द्वारा सर्वशको सिसि अनेक युक्तियों द्वारा की गई है । पूर्वपक्षी के रूप में संवर्त कहता है कि नारद का मत है कि कोई पुरुष सर्वश वीतराम है किन्तु वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्वज्ञ बोतराम सिद्ध ३३४, न्यायदीपिका, पृ० १२५, १२७ ।