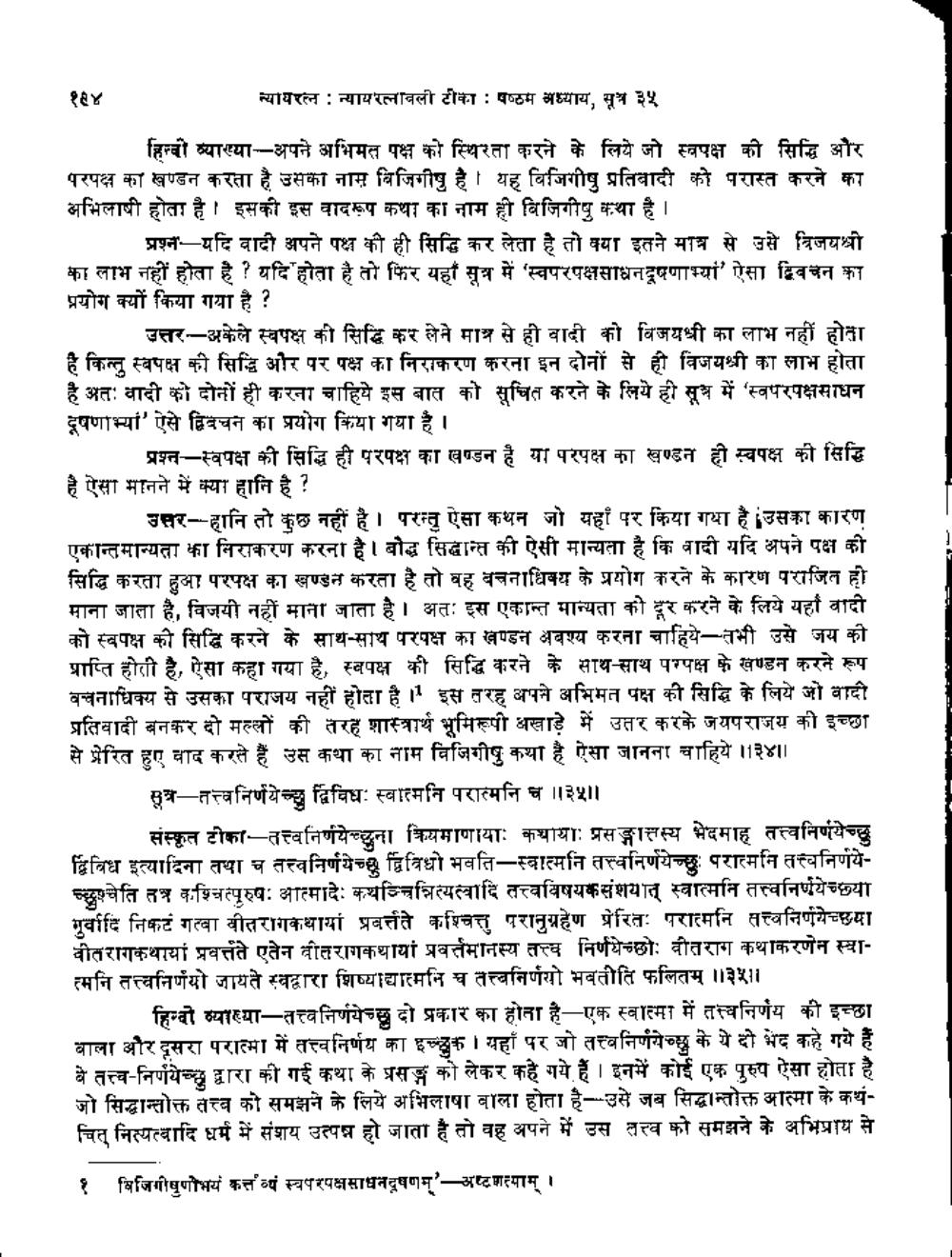________________
१९४
न्यायरल : न्यायरलावली टीका : षष्ठम अध्याय, सूत्र ३५
हिन्दी व्याख्या-अपने अभिमत पक्ष को स्थिरता करने के लिये जो स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष का खण्डन करता है उसका नाम विजिगीषु है। यह विजिगीषु प्रतिबादी को परास्त करने का अभिलाषी होता है। इसकी इस वादरूप कथा का नाम ही विजिगीषु कथा है।
प्रश्न-यदि वादी अपने पक्ष की ही सिद्धि कर लेता है तो क्या इतने मात्र से उसे विजयश्री का लाभ नहीं होता है ? यदि होता है तो फिर यहाँ सूत्र में 'स्वपरपक्षसाधनदूषणाभ्यां' ऐसा द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया है ?
उत्तर-अकेले स्वपक्ष की सिद्धि कर लेने मात्र से ही वादी को विजयश्री का लाभ नहीं होता है किन्तु स्वपक्ष की सिद्धि और पर पक्ष का निराकरण करना इन दोनों से ही विजयश्री का लाभ होता है अतः वादी को दोनों ही करना चाहिये इस बात को सूचित करने के लिये ही सूत्र में 'स्वपरपक्षसाधन दूषणाभ्यां' ऐसे द्विवचन का प्रयोग किया गया है ।
प्रश्न-स्वपक्ष की सिद्धि ही परपक्ष का खण्डन है या परपक्ष का खण्डन ही स्वपक्ष की सिद्धि है ऐसा मानने में क्या हानि है ?
उत्सर-हानि तो कुछ नहीं है। परन्तु ऐसा कथन जो यहाँ पर किया गया है। उसका कारण एकान्तमान्यता का निराकरण करना है। बौद्ध सिद्धान्त की ऐसी मान्यता है कि वादी यदि अपने पक्ष की सिद्धि करता हुआ परपक्ष का खण्डन करता है तो वह बचनाधिक्य के प्रयोग करने के कारण पराजित ही माना जाता है, विजयी नहीं माना जाता है। अतः इस एकान्त मान्यता को दूर करने के लिये यहाँ वादी को स्वपक्ष की सिद्धि करने के साथ-साथ परपक्ष का खण्डन अवश्य करना चाहिये-तभी उसे जय की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है, स्वपक्ष की सिद्धि करने के साथ-साथ परपक्ष के खण्डन करने रूप वचनाधिक्य से उसका पराजय नहीं होता है। इस तरह अपने अभिमत पक्ष की सिद्धि के लिये जो वादी प्रतिवादी बनकर दो मल्लों की तरह शास्त्रार्थ भूमिरूपी अखाड़े में उत्तर करके जयपराजय की इच्छा से प्रेरित हुए बाद करते हैं उस कथा का नाम विजिगीषु कथा है ऐसा जानना चाहिये ।।३४।।
सूत्र-तत्त्वनिर्णयेच्छु द्विविधः स्वात्मनि परात्मनि च ।।३५॥
संस्कृत टीका-तत्त्वनिर्णयेच्छना क्रियमाणायाः कथायाः प्रसङ्गात्तस्य भेदमाह तत्त्वनिर्णयेच्छु विविध इत्यादिना तथा च तत्त्वनिर्णयेच्छु द्विविधो भवति-स्वात्मनि तत्त्वनिर्णयेच्छुः परात्मनि तत्त्वनिर्णये
सुश्चेति तत्र कश्चित्पुरुषः आत्मादेः कथञ्चिन्नित्यत्वादि तत्त्वविषयकसंशयात् स्वात्मनि तत्त्वनिर्णयेच्च्या मुर्वादि निकटं गत्वा वीतरागकथायां प्रवर्तते कश्चित्तु परानुग्रहेण प्रेरितः परात्मनि सत्त्वनिर्णयेच्छया वीतरागकथायां प्रवर्तते एतेन वीतरागकथायां प्रवर्तमानस्य तत्त्व निर्णयेच्छोः वीतराग कथाकरणेन स्वात्मनि तत्त्वनिर्णयो जायते स्वद्वारा शिष्याद्यात्मनि च तत्त्वनिर्णयो भवतीति फलितम् ॥३५।।
हिन्दी व्याख्या-तत्त्वनिर्णयेच्छु दो प्रकार का होता है—एक स्वात्मा में तत्त्वनिर्णय की इच्छा बाला और दूसरा परात्मा में तत्त्वनिर्णय का इच्छुक । यहाँ पर जो तत्त्वनिर्णयेच्छु के ये दो भेद कहे गये हैं बे तत्त्व-निर्णयेच्छु द्वारा की गई कथा के प्रसङ्ग को लेकर कहे गये हैं । इनमें कोई एक पुरुप ऐसा होता है जो सिद्धान्तोक्त तत्त्व को समझने के लिये अभिलाषा वाला होता है-उसे जब सिद्धान्तोक्त आत्मा के कथंचित् नित्यत्वादि धर्म में संशय उत्पन्न हो जाता है तो वह अपने में उस लत्त्व को समझने के अभिप्राय से
१ विजिगीषुणोभयं कर्तव्यं स्वपरपक्षसाधनदूषणम्'–अष्टशत्याम् ।