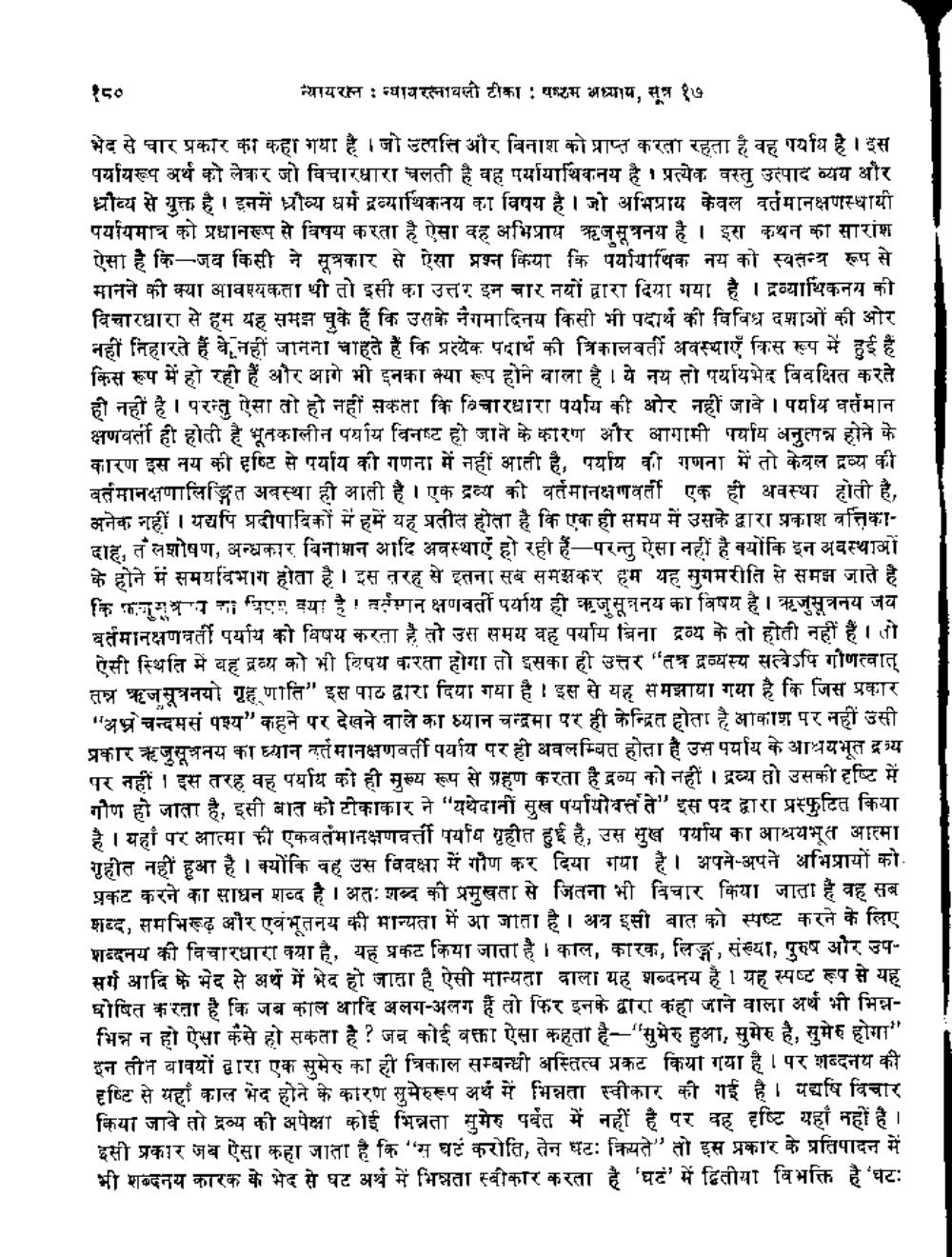________________
१८०
न्यायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : परम अध्याय, सत्र १७
भेद से चार प्रकार का कहा गया है । जो उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त करता रहता है वह पर्याय है । इस पर्यायरूप अर्थ को लेकर जो विचारधारा चलती है वह पर्यायार्थिवनय है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त है । इनमें ध्रौव्य धर्म द्रव्याथिकनय का विषय है । जो अभिप्राय केवल वर्तमानक्षणस्थायी पर्यायमात्र को प्रधानरूप से विषय करता है ऐसा वह अभिप्राय ऋजसूत्रनय है । इस कथन का सारांश ऐसा है कि जब किसी ने सूत्रकार से ऐसा प्रश्न किया कि पर्यायाथिक नय को स्वतन्त्र रूप से मानने की क्या आवश्यकता थी तो इसी का उत्तर इन चार नयों द्वारा दिया गया है । द्रव्याथिकनय की विचारधारा से हम यह समझ चुके हैं कि उसके नैगमादिनय किसी भी पदार्थ की विविध दशाओं की ओर नहीं निहारते हैं वे नहीं जानना चाहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की त्रिकालवर्ती अवस्थाएँ किस रूप में हुई हैं किस रूप में हो रही हैं और आगे भी इनका क्या रूप होने वाला है । ये नय तो पर्यायभेद विवक्षित करते ही नहीं है । परन्तु ऐसा तो हो नहीं सकता कि विचारधारा पर्याय की ओर नहीं जावे । पर्याय वर्तमान क्षणवर्ती ही होती है भूतकालीन पर्याय बिनष्ट हो जाने के कारण और आगामी पर्याय अनुत कारण इस नय की दृष्टि से पर्याय की गणना में नहीं आती है, पर्याय की गणना में तो केवल द्रव्य की वर्तमानक्षणालिङ्गित अवस्था ही आती है । एक द्रव्य की वर्तमानक्षणवर्ती एक ही अवस्था होती है, अनेक नहीं । यद्यपि प्रदीपादिकों में हमें यह प्रतीत होता है कि एक ही समय में उसके द्वारा प्रकाश बत्तिकादाह, तं लशोषण, अन्धकार विनाशन आदि अवस्थाएं हो रही हैं परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि इन अवस्थाओं के होने में समयविभाग होता है। इस तरह से इतना सब समझकर हम यह सुगमरीति से समझ जाते है कि कम अपना प्रषा क्या है। वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय ही ऋजुसूत्रनय का विषय है । ऋजुसुत्रनय जय वर्तमानक्षणवर्ती पर्याय को विषय करता है तो उस समय वह पर्याय बिना द्रव्य के तो होती नहीं है । तो ऐसी स्थिति में बह द्रव्य को भी विषय करता होगा तो इसका ही उत्तर "तत्र द्रव्यस्य सत्वेऽपि गौणत्व तन्न ऋजसूत्रनयो गृह णाति" इस पाठ द्वारा दिया गया है । इस से यह समझाया गया है कि जिस प्रकार "अभ्र चन्दमसं पश्य" काहने पर देखने वाले का ध्यान चन्द्रमा पर ही केन्द्रित होता है आकाश पर नहीं उसी प्रकार ऋजुसूत्रनय का ध्यान दर्तमानक्षणवर्ती पर्याय पर ही अवलम्बित होता है उस पर्याय के आथयभूत द्रव्य पर नहीं । इस तरह वह पर्याय को ही मुख्य रूप से ग्रहण करता है द्रव्य को नहीं । द्रव्य तो उसकी दृष्टि में गौण हो जाता है, इसी बात को टीकाकार ने "यथेदानीं सुख पर्यायोवर्तते" इस पद द्वारा प्रस्फुटित किया है । यहाँ पर आत्मा की एकवर्तमानक्षणवर्ती पर्याय गृहीत हुई है, उस सुख पर्याय का आश्रयभूत आत्मा गृहीत नहीं हुआ है । क्योंकि वह उस विवक्षा में गौण कर दिया गया है। अपने-अपने अभिप्रायों को प्रकट करने का साधन शब्द है । अतः शब्द की प्रमुखता से जितना भी विचार किया जाता है वह सब शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूतनय की मान्यता में आ जाता है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शब्दनय की विचारधारा क्या है, यह प्रकट किया जाता है । काल, कारक, लिङ्ग, संख्या, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है ऐसी मान्यता वाला यह शब्दनय है । यह स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि जब काल आदि अलग-अलग हैं तो फिर इनके द्वारा कहा जाने वाला अर्थ भी भिन्नभिन्न न हो ऐसा कैसे हो सकता है ? जब कोई बक्ता ऐसा कहता है-"सुमेर हुआ, सुमेरु है, सुमेरु होगा" इन तीन बावयों द्वारा एक सुमेरु का ही त्रिकाल सम्बन्धी अस्तित्व प्रकट किया गया है । पर शब्दनय की दृष्टि से यहाँ काल भेद होने के कारण सुमेरुरूप अर्थ में भिन्नता स्वीकार की गई है। यद्यषि विचार किया जावे तो द्रव्य की अपेक्षा कोई भिन्नता सुमेरु पर्वत में नहीं है पर वह दृष्टि यहाँ नहीं है । इसी प्रकार जब ऐसा कहा जाता है कि "म घटं करोति, तेन घटः क्रियते' तो इस प्रकार के प्रतिपादन में भी शब्दनय कारक के भेद से घट अर्थ में भिन्नता स्वीकार करता है 'घटे' में द्वितीया विभक्ति है 'घटः