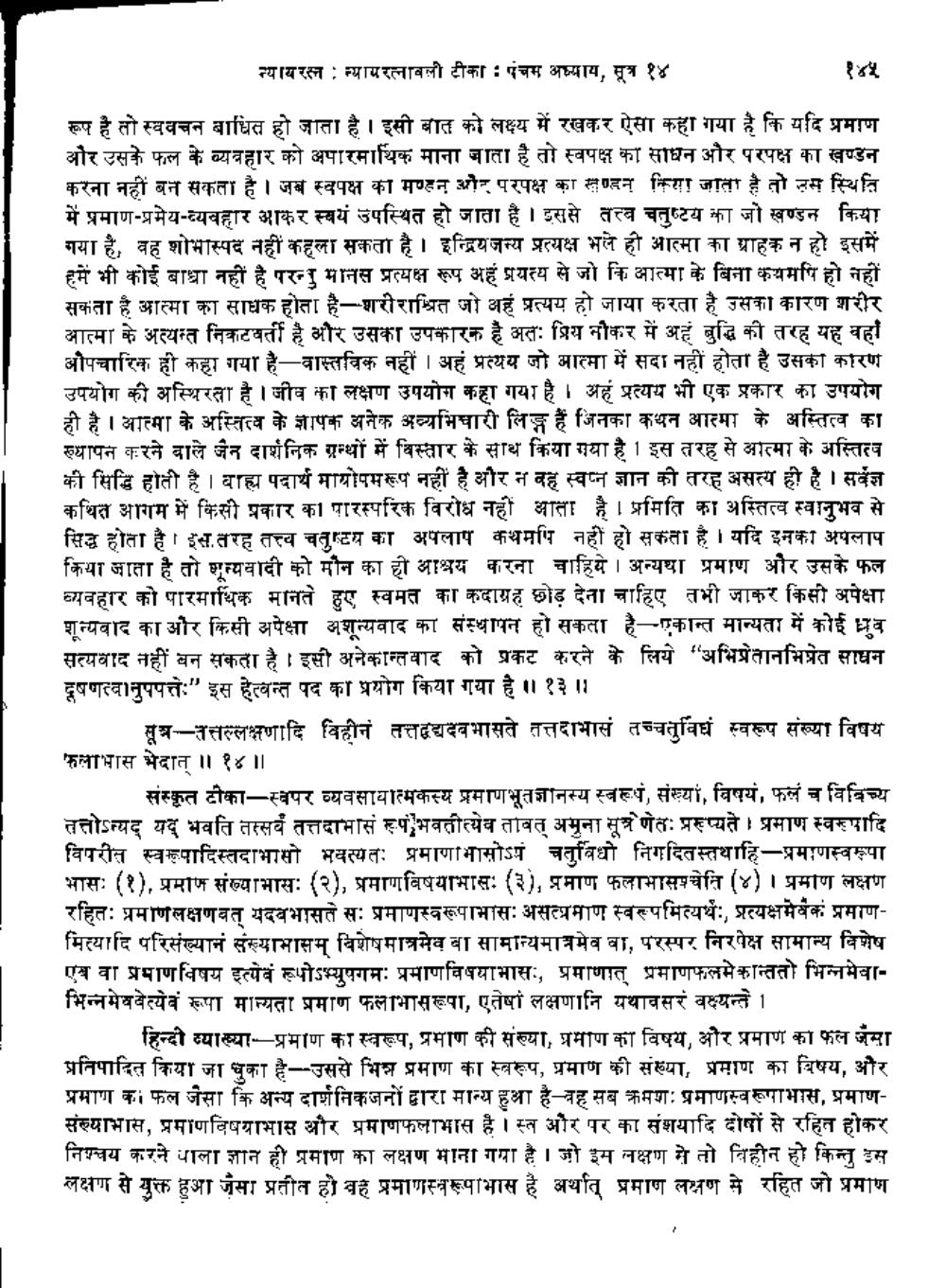________________
न्यायरल : न्यायरत्नावली टीका: पंचम अध्याय, सूत्र १४
रूप है तो स्ववचन बाधित हो जाता है । इसी बात को लक्ष्य में रखकर ऐसा कहा गया है कि यदि प्रमाण और उसके फल के व्यवहार को अपारमार्थिक माना जाता है तो स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का खण्डन करना नहीं बन सकता है । जब स्वपक्ष का महान ओट परपक्ष का स्तुण्डन किया जाता है तो उस स्थिति में प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार आकर स्वयं उपस्थित हो जाता है । इससे तत्त्व चतुष्टय का जो खण्डन किया गया है, वह शोभास्पद नहीं कहला सकता है। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष भले ही आत्मा का ग्राहक न हो इसमें हमें भी कोई बाधा नहीं है परन्तु मानस प्रत्यक्ष रूप अहं प्रयत्य से जो कि आत्मा के बिना कममपि हो नहीं सकता है आत्मा का साधक होता है-शरीराश्रित जो अहं प्रत्यय हो जाया करता है उसका कारण शरीर आत्मा के अत्यन्त निकटवर्ती है और उसका उपकारक है अतः प्रिय नौकर में अहं बुद्धि की तरह यह वहाँ औपचारिक ही कहा गया है वास्तविक नहीं । अहं प्रत्यय जो आत्मा में सदा नहीं होता है उसका कारण उपयोग की अस्थिरता है । जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है । अहं प्रत्यय भी एक प्रकार का उपयोग ही है । आत्मा के अस्तित्व के ज्ञापक अनेक अव्यभिचारी लिङ्ग हैं जिनका कथन आत्मा के अस्तित्व का ख्यापन करने वाले जैन दार्शनिक ग्रन्थों में विस्तार के साथ किया गया है । इस तरह से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है । बाह्य पदार्थ मायोपमरूप नहीं है और न वह स्वप्न ज्ञान की तरह असत्य ही है । सर्वज्ञ कथित आगम में किसी प्रकार का पारस्परिक विरोध नहीं आता है । प्रमिति का अस्तित्व स्वानुभव से सिद्ध होता है। इस.तरह तत्त्व चतुष्टय का अपलाप कथमपि नहीं हो सकता है । यदि इनका अपलाप किया जाता है तो सत्यवादी को मौन का ही आश्रय करना चाहिये । अन्यथा प्रमाण और उसके फल व्यवहार को पारमार्थिक मानते हुए स्वमत का कदाग्रह छोड़ देना चाहिए तभी जाकर किसी अपेक्षा शून्यवाद का और किसी अपेक्षा अशून्यवाद का संस्थापन हो सकता है-एकान्त मान्यता में कोई ध्रुव सत्यवाद नहीं बन सकता है । इसी अनेकान्त वाद को प्रकट करने के लिये "अभिप्रेतानभिप्रेत साधन दूषणत्वानुपपत्तेः" इस हेत्वन्त पद का प्रयोग किया गया है ॥ १३ ॥
सूत्र-तत्तल्लक्षणादि विहीनं तत्तद्वद्यदवभासते तत्तदाभासं तच्चतुर्विधं स्वरूप संख्या विषय 'फलाभास भेदात् ॥ १४ ॥
संस्कृत टीका-स्वपर व्यवसायात्मकस्य प्रमाणभूतज्ञानस्य स्वरूपं, संख्या, विषयं, फलं च विविच्य तत्तोऽन्यद यद भवति तत्सर्व तत्तदाभासं रूपं भवतीत्येव तावत अमना सत्रणेतः प्ररूप्यते। प्रमाण स्वरुपादि विपरीत स्वरूपादिस्तदाभासो भवत्यतः प्रमाणाभासोऽयं चतुर्विधो निगदितस्तथाहि-प्रमाणस्वरूपा भासः (१), प्रमाण संख्याभासः (२), प्रमाणविषयाभासः (३), प्रमाण फलाभासपचेति (४) । प्रमाण लक्षण रहितः प्रमाणलक्षणवत् यदवभासते सः प्रमाणस्वरूपाभासः असत्प्रमाण स्वरूपमित्यर्थः, प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमित्यादि परिसंख्यानं संख्याभासम् विशेषमात्रमेव वा सामान्यमात्रमेव वा, परस्पर निरपेक्ष सामान्य विशेष एक वा प्रमाणविषय इत्येवं रूपोऽभ्युपगमः प्रमाणविषयाभासः, प्रमाणात प्रमाणफलमेकान्ततो भिन्नमेवाभिन्नमेववेत्येवं रूपा मान्यता प्रमाण फलाभासरूपा, एतेषां लक्षणानि यथावसरं वक्ष्यन्ते ।
हिन्दी व्याख्या प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का विषय, और प्रमाण का फल जमा प्रतिपादित किया जा चुका है--उससे भिन्न प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का विषय, और प्रमाण का फल जैसा कि अन्य दार्शनिकजनों द्वारा मान्य हआ है-वह सब क्रमशःप्रमाणस्वरूपाभास, प्रमाणसंख्याभास, प्रमाणविषयाभास और प्रमाणफलाभास है। स्त और पर का संशयादि दोषों से रहित होकर निश्चय करने पाला ज्ञान ही प्रमाण का लक्षण माना गया है । जो इस लक्षण मे तो बिहीन हो किन्तु इस लक्षण से युक्त हुआ जसा प्रतीत हो वह प्रमाणस्वरूपाभास है अर्थात् प्रमाण लक्षण से रहित जो प्रमाण